आप गा रहे हैं। गाए जा रहे हैं। वैसे सुनने वालों को आपका यह गाना आलाप, प्रलाप या विलाप कुछ भी लग सकता है। पर उससे आपको क्या। आपको को तो गाने से मतलब है। आज तय करके आए हैं कि गाना ही है सो गा रहे हैं। वैसे आप मध्यकालीन साहित्य पढ़ाते हैं, कोई साहित्य नहीं पढ़ते, लेकिन संयोग से आपकी यह कविता रीतिकालीन बन पड़ी है, इसलिए आप खुश हैं। गीत का मुखड़ा जो आप हर चौथी लाइन के बाद तीन बार दोहरा रहे हैं, कुछ इस तरह से है, ‘हे गोरी, पनघट की डगर (काफी) कठिन है, (इसलिए) जरा सँभल के चलो।’ आपने सँभल की तुक पर लचक, मचक, फिसल और दहल शब्द रखकर अपनी साहित्यिक उदारता का परिचय दिया है। अलबत्ता, गीत में आप गोरी को सँभलकर चलने की बात तो बता रहे हैं, पता नहीं चल पा रहा कि यह उसे नेक सलाह है, धमकी है, आदेश, मार्गदर्शन है, गिड़गिड़ाहट है या फिर उससे अनुरोध किया जा रहा है। वजह यह है कि आपकी मुखमुद्रा तो हास्य-रस की कविता सुनाने जैसी हो रही है, और आवाज़ में इतनी करुणा है कि ‘जरा सँभल के चलो’ तक आते-आते पूरी तरह पंचर हो जाती है। आपके खड़े होने का अंदाज धोबी पछाड़ लगा चुके उस पहलवान की तरह है जो सामने धराशाई पड़े पहलवान के उठ खड़े होने का इंतज़ार कर रहा होता है। माइक आपने वीररस की मुद्रा में दोनों हाथों से मजबूती से थामा हुआ है। आँखें आपकी बार-बार बन्द हो जाती हैं। इसलिए श्रोता परेशान हैं कि आपकी कविता और गायन कला को किस कैटेगरी में डालें। वैसे आज का यह कवि-सम्मेलन पर्यावरण को समर्पित है।
एक बात बताएँ। आपको इस तरह भंड़ैती करते देख हमें आप पर तरस ही आ रहा है। थ्री पीस सूट पहने, बढ़िया टाई लगाए आप ये सब राग अलापते बिल्कुल नहीं जॅच रहे। एक बात और भी है, आपकी कविता ही आपकी पोल खोल रही है कि आपने फिल्मों में जितने भी पनघट और पनिहारिनें देखी हों, असल ज़िन्दगी में तो एक भी नहीं देखी है। पता नहीं आप किस इमारत के पिछवाड़े कदम ताल करते रह गये। इस बीच कविता आगे निकल गयी और पनिहारिनें पीछे रह गयीं। आप जिस गोरी या सांवली को पनघट की राह पर संभल कर चलने की सलाह दे रहे हैं, उस करमजली की तो कई पीढ़ियां गुज़र गयीं पनघट से दिन में चार बार पानी लाने और उसे आप चलना सिखा रहे हैं। रहने दीजिए, आपको शायद पता नहीं, आजकल पनघट किस हालत में हैं, और पनिहारिनें किस हाल में अपने दिन गुज़ार रही हैं।
नदी, नाले, पनघट, कूएं सब कब से सूखे पड़े हैं। वहाँ तो अब डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी भी नहीं है। और पनिहारिनें? वे तो.. अब क्या बताएं आपको कैसे गुज़ार रही हैं वे अपने दिन। पैरों में चप्पल नहीं, तन पर पूरे कपड़े नहीं, पेट में खाना नहीं, और भी पचासों तकलीफें है। पैरों का बिवाइयों के मारे बुरा हाल है। एड़ियाँ घिस गई हैं। इन सारी परेशानियों के साथ आप उसके जले पर नमक और छिड़क रहे हैं कि गोरी जरा संभल के चलो कि कहीं पाँव लचक न जाए। बेहतर हो, आप यह नेक सलाह अपने पास ही रखें और उसे उसकी राह जाने दें। वह बेचारी कहीं अपने पैरों की लचक की तरफ ध्यान देने लग गई और आपकी सलाह मानकर कदम-कदम सँभल के चलने लग गई तो हो चुके उसके काम। उसे सिर्फ पानी लाने का ही काम नहीं है। दसियों और धंधे हैं करने को। और क्या कोई फिल्म की शूटिंग हो रही है यहाँ कि जरा संभल के चले कि शॉट सही आ जाए। जहाँ असली जिन्दगी होती है, वहाँ ये सब चोंचले नहीं चलते श्रीमान।
विश्वविद्यालय में हिन्दी साहित्य पढ़ाना और पनघट से पानी लाना बिल्कुल अलग-अलग चीजें हैं। दोनों को एक ही कुंजी से मत पढ़ाइए।
वैसे आप बुरा न मानें तो हम ही कह दें कि संभलकर चलने और बोलने, कविता करने की असली जरूरत तो आपको है, जिसे न आज की कविता का पता न पनघट का। कविता कहाँ से कहाँ पहुँच गई जनाब, जरा स्टार टीवी और जीटीवी छोड़कर घर से बाहर तो निकलिए। अब तेरहवीं सदी का बासी माल कविता के नाम पर इस वातानूलित ऑडिटोरियम में जबरदस्ती काहे परोसे जा रहे हैं। वैसे अगर यहाँ आने की कोई बहुत बड़ी मजबूरी थी, यहाँ से मिलने वाला लिफाफा काफी वजनदार था और आना जरूरी था, तो अच्छा होता आप कभी खुद की लिखी या किसी से लिखवाई गई पीएचडी की थीसिस में से एकाध पैराग्राफ पढ़कर सुना देते, सबका मनोरंजन हो जाता। शायद उसमें कुछ मौलिकता भी नज़र आ जाती। कविता को पनघट के कीचड़ में लथेड़ कर आप उसकी मिट्टी पलीद ही कर रहे हैं। अब बहुत हुआ। दुनिया में और पचासों काम हैं, जिन्हें आप ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं और घर बैठे कमा भी सकते हैं। कविता आपका फील्ड नहीं है। इसे आप आउट ऑफ कोर्स ही रखें तो बेहतर।
क्षमा करें पाठकगण, हम आपको आज के आयोजन के बारे में तो बताना भूल ही गये। यह मौका है आकाशवाणी केन्द्र द्वारा आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का। वैसे तो मुहावरा तीन बुलाए तेरह आये का है, लेकिन सच में इसका उलट हुआ है। आकाशवाणी ने बाहर से तेरह बुलाए थे, तीन ही आए हैं, इसलिए मंच भरने के लिए आप जैसी स्थानीय प्रतिभाओं की भरपूर सेवाएँ ली गई हैं। चूँकि विषय पर्यावरण यानी प्रकृति है और तीनों पधारे कवि पहुँचे हुए गीतकार-गायक हैं, इसलिए देखा-देखी स्थानीय कवि-समुदाय ने भी गाकर सुनाने की कसम खा ली है । श्रोताओं की संख्या में भी ऊपर वाले मुहावरे का व्यावहारिक पक्ष ही देखा जा सकता है। दो सौ बुलाए, तीस आए। यह जो भरा-भरा-सा हॉल है, इनमें से आधे से ज्यादा तो आकाशवाणी के ही कर्मचारी हैं।
संचालन बाहर से पधारे एक कवि कर रहे हैं अत: बेचारे इन प्रतिभाओं का पूरा परिचय भी नहीं दे पा रहे हैं। अभी आपसे पहले न केवल संचालक, बल्कि सारे श्रोता भी गच्चा खा गए थे। हुआ यह कि संचालक ने उन्हें कविता-पाठ के लिए आमंत्रित किया। उनके माइक सँभालते ही पूरा हॉल नीरजमय हो गया। वही नीरज की आवाज़, उन्हीं के शब्द, लटके, झटके और ठसके और नीरज का खास लहजा फिज़ा में तैरने लगा। सब हैरान । संचालक परेशान । उनसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। यहाँ नीरज जी आए हुए हैं, मंच पर कविता-पाठ कर रहे हैं और वे पहचानते तक नहीं उन्हें । कहीं भाँग तो नहीं खिला दी किसी ने। उन्होंने बार-बार देखा, नाम दोबारा पढ़ा-लगती कहाँ हो गई है। हार कर साथ बैठे स्थानीय कवि से पूछा तो पता चला इन कविजी में अक्सर जीवित और दिवंगत कवियों का सूक्ष्म शरीर प्रवेश कर जाता है। आज सौभाग्य से नीरज जी का नंबर लग गया, सो इतने सस्ते में आप उन्हें सुन पा रहे हैं।
कार्यक्रम की अध्यक्षता शहर में होने वाले सभी साहित्यिक आयोजनों के स्थायी अध्यक्ष उज्ज्वल धोतीधारी जी कर रहे हैं। वे जाते ही उस सम्मेलन में हैं, जिसमें उन्हें अध्यक्षता करनी होती है। वे स्थानीय विश्वविद्यालय के भूतपूर्व आचार्य और ऐसे सम्मेलनों के अभूतपूर्व अध्यक्ष हैं। वे क्या बोलेंगे और कौन-सी कविता सुनाएँगे,श्रोताओं को पहले से मालूम रहता है। यहाँ तक कि वे लतीफा कौन-सा सुनाएँगे, लोग-बाग इस पर भी शर्त लगा सकते हैं। उन्होंने भी आजीवन मध्यकाल पढ़ाया है, मध्यकालीन साहित्य ही पढ़ा है और लिखा भी उसी काल का है। वे एक मायने में मध्यकालीन कवियों से बेहतर हैं कि मध्यकालीन कवियों की पोथियाँ उनके जीते जी प्रकाशित नहीं हुई थी, जबकि इनकी हो गई हैं। ये प्रतिदिन अध्यक्षता करते हैं जबकि सूर, तुलसी को शायद ही किसी आयोजन की अध्यक्षता का मौका मिला हो। कवि लोग केवल कवि थे, जबकि ये आचार्य और कवि दोनों हैं।
बात लंबी खिच रही है। सौभाग्य से बाहर बरसात थमने का सुखद समाचार मिला है। ‘आप’ अभी भी ज़रा सँभल के चलो’ पर स्थायी भाव से अटके’ हुए हैं। हम तो चले। अलबत्ता, ‘संभल के चलेंगे’, बाहर कीचड़ हो गया है और कहीं हमारे ही पैर लचक गए तो?
1994
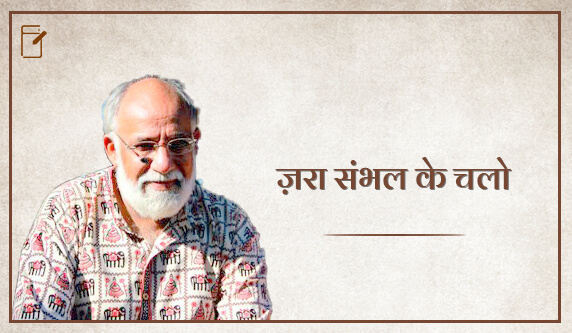
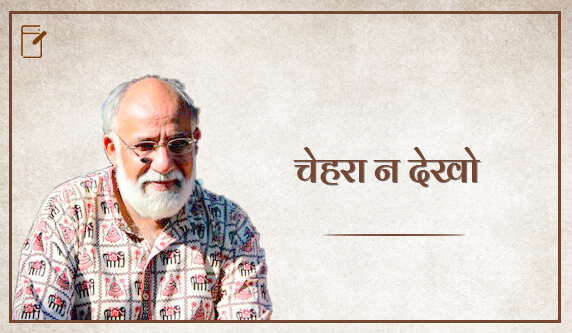
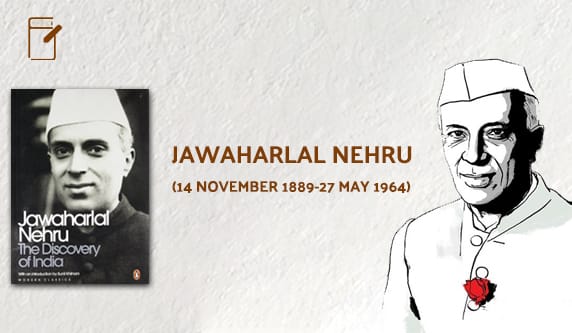
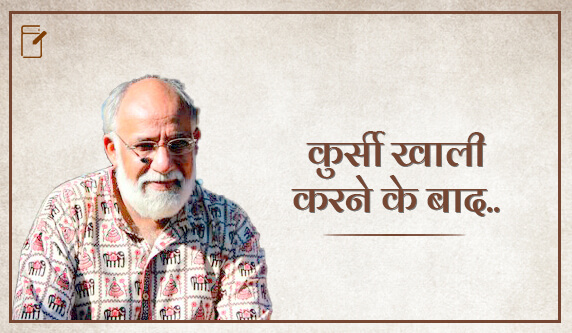

No Comments