बात शायद 1999 के मुंबई फि़ल्म फेस्टिवल की है। तब तक उसका मुंबई से स्थायी रूप से मोहभंग नहीं हुआ था और वह अपनी रोज़ी-रोटी मुंबई में ही कमा खा रहा था। उन दिनों मेरा ऑफिस मुंबई में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुआ करता था और फि़ल्म फेस्टिवल के सीज़न टिकट मेरे ऑफिस के रास्ते में ही यशवंत राव चौहान हॉल में मिलने वाले थे। हमने तय किया कि किसी शनिवार को वहां जाकर लेते आएंगे।
काउंटर पर जो अंग्रेजीदां लड़की बैठी थी, उसने फार्म उसकी तरफ बढ़ाया और अंग्रेजी में ही कहा कि इसे भर दीजिए और साथ में दो फोटोग्राफ दे दीजिए। उसने अपनी सदाबहार स्टाइल में कहा कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती। ये सुनते ही वह लड़की झटके से अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे कुछ सूझा ही नहीं कि क्या कहे। उसके सामने फैशनेबल कपड़े पहने एक खूबसूरत नौजवान खड़ा है जो फि़ल्म फेस्टिवल देखने की चाह रखता है और जब उसे इसके लिए फार्म भरने के लिए कहा जाता है तो बताता है कि उसे अंग्रेजी नहीं आती। उसने बट, हाउ जैसे कुछ शब्दों के सहारे जानना चाहा कि फिर आप ये फि़ल्में! तब हमारे नौजवान दोस्त ने उस लड़की से कहा था कि अंग्रेजी क्या, किसी भी भाषा की फि़ल्म देखने के लिए अंग्रेजी जानने की ज़रूरत नहीं होती।
यह खूबसूरत नौजवान था मनोज रूपड़ा। उसे सचमुच अंग्रेजी बोलना, पढ़ना या लिखना आज भी नहीं आता, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसने जितनी संख्या में अंग्रेजी की और दुनिया भर की दूसरी भाषाओं की फि़ल्में देखी होंगी, शायद ही किसी हिंदी कहानीकार ने देखी होंगी। और मैं यह शर्त भी बद सकता हूं कि जिस अधिकार और आत्मविश्वास के साथ वह दुनिया की किसी भी भाषा की फि़ल्म के क्राफ्ट, शिल्प, कैमरावर्क, स्क्रिप्ट और दूसरे तकनीकी पक्षों पर बात कर सकता है, शायद ही कोई और समकालीन कहानीकार कर सकता है। उसने पहली संगमन गोष्ठी में आज से पंद्रह बरस पहले समांतर फि़ल्मों पर कोई तीस पेज का गंभीर लेख पढ़कर सुनाया था।
अब जब फि़ल्मों की बात चल रही है तो पहले यही बात पूरी कर ली जाए। अभी पिछले दिनों पुणे में इंटरनेशनल फि़ल्म फेस्टिवल सम्पन्न हुआ। मैंने मनोज को इसके बारे में बताया तो उसने तुरंत अपने फोटो भेज दिए कि उसके लिए भी सीज़न टिकट बुक करवा रखूं। वह पूरे हफ्ते के लिए आएगा। इसी फेस्टिवल के लिए दिल्ली से मेरे बहुत पुराने दोस्त और कथाकार सुरेश उनियाल भी आ रहे थे। पुणे में ही स्थायी रूप से बस चुके विश्व सिनेमा पर अथोरिटी समझे जाने वाले हमारे दोस्त मनमोहन चड्ढा तो थे ही। हमने एक साथ खूब फि़ल्में देखीं, खूब धमाल किया और देखी गई और न देखी गई फि़ल्मों पर खूब बहस भी की। इसी फेस्टिवल में हमने एक ऐसी फि़ल्म देखी, जिसके बारे में मैंने मनोज से ही सुना था और इसके बारे में इंटरनेट से और जानकारी खंगाली थी। (मनोज यह फि़ल्म पहले देख चुका था और उसका आगामी उपन्यास भी इसी फि़ल्म से गहरा ताल्लुक रखता है।) यह फि़ल्म थी 1927 में प्रदर्शित हुई फिट्ज़ लैंग की मेट्रोपॉलिस।। ढाई घंटे की यह मूक फि़ल्म कई मायनों में अद्भुत थी और अपने वक्त से बहुत आगे की बात कहती थी। पूंजी और श्रम के बीच के टकराव, आदमी को पूरी तरह से निचोड़कर रख देने वाली दैत्याकार मशीनें, आदमी और मशीन की लड़ाई, डबल रोल, रोबो की कल्पना और उसके ज़रिए हमशक्ल नेगेटिव पात्र का सृजन, कल्पनातीत स्पेशल इफेक्ट्स वग़ैरह फि़ल्म निर्देशक आज से अस्सी साल पहले परदे पर साकार कर चुका था। इस फेस्टिवल में हमने जितनी फि़ल्में देखीं, उनमें मादाम बावेरी और मैट्रोपोलिस सबसे अच्छी रहीं। फि़ल्मों का चस्का मनोज को दुर्ग के दिनों से है। उन दिनों वह दुर्ग में प्रगतिशील लेखक संघ का अध्यक्ष हुआ करता था। मध्य प्रदेश में उन दिनों तक एक सिलसिला चला करता था महत्त्व फलां फलां। इसके अंतर्गत रचनाकारों पर केन्द्रित कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। भीष्म साहनी आदि पर हो चुके थे और दुर्ग में ‘महत्त्व नामवर सिंह’ के आयोजन की रूपरेखा बनायी गई थी। इस काम के लिए एक लाख का बजट था। बताया गया कि कोई व्यापारी धन देगा। स्थानीय इकाई के अध्यक्ष होने के नाते मनोज ने इसका विरोध किया और कहा कि मजदूर विरोधी पूंजीपति के पैसे से इस कार्यक्रम को वे नहीं होने देंगे। इसके बजाए कम खर्चे पर कोई फि़ल्म आधारित कार्यक्रम रखा जाए। संस्था में दो गुट बन गए। ज्यादातर सदस्य ‘महत्व नामवर सिंह’ के पक्ष में। मनोज ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और अकेले अपने बलबूते पर फि़ल्म आधारित कार्यक्रम की तैयारियां की। फि़ल्मों पर बात करने और कुछ चुनींदा फि़ल्में दिखाने के लिए प्रख्यात फि़ल्म हस्ती सतीश बहादुर को आमंत्रित किया गया। संयोग ऐसा बना कि आयोजन में भाग लेने के लिए कोई भी नहीं आया। बेशक सतीशजी अपने तामझाम के साथ वहां पहुंच गए थे।
निराश कर देने वाले ऐसे मुश्किल पलों में भी कुछ सुंदर, कुछ शिव छुपा हुआ था। मनोज अकेले ही पूरे अरसे तक सतीश बहादुर से फि़ल्मों की बारीकियों का गंभीर अध्ययन करता रहा। उनके द्वारा लाई गईं दुर्लभ फि़ल्मों का इकलौता दर्शक बना रहा और उन पर बात करता रहा। बेशक बीच-बीच में दो चार लोग आते जाते रहे होंगे, लेकिन कुल मिलाकर ये पूरा सिलसिला वन टू वन ही रहा। शायद सतीशजी को भी न पहले न बाद में इस जैसा समर्पित विद्यार्थी कभी मिला होगा। उन्हीं की सिफारिश पर बाद में मनोज ने पटना में प्रकाश झा की पंद्रह दिवसीय कार्यशाला में सक्रिय भागीदारी की और फि़ल्म की भाषा को और गहराई से पढ़ा। बाद में ‘महत्व नामवर सिंह’ भी हुआ जिसमें मनोज नहीं गया, बेशक नामवरजी उसके बारे में पूछताछ करते रहे।
मनोज पर यह बात सिर्फ़ फि़ल्मों के बारे में ही लागू नहीं होती। वह मध्य प्रदेश की लोक कलाओं और लोक कलाकारों से भी नज़दीकी से जुड़ा रहा है और उन पर भी पूरे अधिकार के साथ बात कर सकता है। वह नाचा के महान कलाकार मदन निषाद का मुरीद है और उन्हें दुनिया के किसी भी कलाकार की तुलना में श्रेष्ठ मानता है। उसे इस बात का भी बेहद अफसोस है कि मदन निषाद की कला उनके साथ ही ख़त्म हो गई है। न केवल लोक कलाओं से बल्कि नाटक से भी उसका नाता रहा है और उसने देवेन्द्र राज अंकुर के निर्देशन में नाटकों में काम भी किया है।
मनोज के यही स्कूल रहे हैं जहां बेशक अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती थी, लेकिन जीवन के सारे असली पाठ मनोज ने इन्हीं पाठशालाओं से सीखे हैं। वाचिक परंपरा कह लें या चीज़ों को देखने परखने की गहरी दृष्टि और लगन, मनोज ने स्कूली पढ़ाई की कमी इसी तरह पूरी की है। मनोज ने पढ़ा भी ख़ूब है। जो कुछ हिन्दी के ज़रिए उस तक पहुंचा, उसने उसे आत्मसात किया है। अब ये बात अलग है कि एक्स्ट्रा ट्यूटोरियल के नाम पर मनोज ने कुछ बदमाशियां, कुछ हरमज़दगियां और कुछ आउट ऑफ़ कोर्स की चीज़ें भी सीखीं और इफरात में सीखीं। ये बातें भी मनोज के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा हैं। बेशक सामने वाले को हवा भी नहीं लगती कि ये सामने गैलिस वाली पैंट और अजीब सी कमीज़ पहने या परदे के कपड़े की पैंट और उस पर सुर्ख लाल कमीज पहने भोला सा लड़का खड़ा है, जो किसी भी परिचित या अपरिचित व्यक्ति से बात तक करने में संकोच करता है, और मुश्किल से ही सामने वाले से संवाद स्थापित कर पाता है, दरअसल खेला खाया है और जीवन के हर तरह के अनुभव ले चुका असली इंसान है। लेकिन एक बात है। जब अनुभव लेने की बात आती है या जीवन के किन्हीं दुर्लभ पलों का आनंद लेने की बात आती है तो मनोज के सामने बस वही पल होते हैं। उसमें लेखक के रूप में उस अनुभव से गुज़रने की ललक कहीं नहीं मिलती कि घर जाकर इस अनुभव को एक धांसू कहानी में ढालना है। मनोज की इसी बात पर मैं जी जान से फि़दा हूं। उसका कहना है कि जो लोग हर वक्त लेखक बने रहते हैं, न तो जीवन का आनंद ले पाते हैं और न ही स्थायी किस्म का लेखन ही कर पाते हैं। भोगा हुआ सबकुछ कहानी का कच्चा माल नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसा भी हो जिसमें आपने भरपूर आनंद लिया हो। उसे लिखने का कोई मतलब नहीं होता। लेखक को बहुत कुछ पाठक पर भी छोड़ देना चाहिए और सबकुछ जस तस उसके सामने नहीं परोस देना चाहिए कि अख़बार की ख़बर और कहानी में फ़र्क किया ही न जा सके। यही वजह है कि उसकी कोई भी कहानी-पता है कल क्या हुआ मार्का नहीं है। मनोज यह भी मानता है कि कभी भी पाठक को कम करके मत आंको। वह भी लेखक के समाज का ही बाशिंदा है और हो सकता है लेखक से ज्यादा संवेदनशील हो और च़ीजों को बेहतर तरीके से जानता हो।
एक बार मनोज देर रात मुंबई में वीटी स्टेशन के पास मटरगश्ती कर रहा था। उसका सामना वहीं चौराहे पर बैठे कुछ आवारा छोकरों के साथ हो गया। वे लड़के दीन दुनिया से ठुकराये गए थे और उन्होंने अपने आप को नशे की दुनिया के हवाले कर रखा था। मनोज भी रोमांच के चक्कर में उनमें जा बैठा और जल्द ही उनके साथ घुल मिल गया। अब मनोज एक दूसरी ही दुनिया में था। वह कई घंटे उनके साथ रहा और उनके बीच में से ही एक बनकर रहा। वहीं पर उन बच्चों के बारे में रोंगटे खड़े कर देने वाले कई सच उसके सामने आए लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसने मेरे या अपने अभिन्न मित्र आनंद हर्षुल के अलावा किसी और से ये अनुभव बांटे हों या इस पर कुछ लिखा हो।
लेखन और आनंद या जि़न्दगी को भरपूर जीना उसके लिए अलग अलग चीज़ें हैं और उनमें कोई घालमेल नहीं। मैं कितने ही ऐसे रचनाकारों को जानता हूं जिन्होंने रात को घटी घटना पर सुबह सुबह ही कहानी लिखकर पहली ही डाक से किसी प्रिय संपादक के पास रवाना भी कर दी। यह बात दीगर है कि इस तरह की रचना कितनी देर के लिए और किस तरह प्रभाव छोड़ती है।
मनोज ने कार्ल मार्क्स और दूसरा विश्व साहित्य भट्ठी के आगे बैठे हुए कढ़ाई में दूध औंटाते हुए पढ़ा है। मुझे नहीं पता कि किन वजहों से उसकी स्कूली पढ़ाई छूटी होगी, लेकिन एक बात तय है कि मनोज ने गोर्की की तरह जो कुछ जीवन की पाठशालाओं में सीखा है, हमारे देश के किसी स्कूल की न हैसियत थी और न है कि उसे वह सबकुछ सिखा सकता जो उसने स्कूल से बाहर रहकर सीखा है। यही उसके जीवन की असली पाठशालाएं है।
मनोज जब छठी कक्षा में ही था तो उसे जुए की लत लग गयी। दोस्तों के साथ चितपट नाम का जुआ खेलना मनोज को बहुत भाता था। एक दिन इसी चक्कर में शहर के गांधी चौराहे पर मनोज चार दोस्तों के साथ जुआ खेल रहे एक लड़के के पिता वहां आ पहुंचे। तब मनोज की जो पिटाई हुई, उसकी टीस वह आज भी याद करता है। जुआ तो हमेशा के लिए छूटा ही, स्कूल भी तभी छूट गया था।
एक और बार मनोज बुरी तरह से पिटते-पिटते बचा। दुर्ग में एक व्यापारी हैं जिनका शराब बनाने का कारखाना है। उनका सचिव था रमा शंकर तिवारी जो जनवादी लेखक संघ का पदाधिकारी था और मनोज का दोस्त था। एक बार व्यापारी के यहां कोई परिवारिक आयोजन था जिसमें सभी २५०० मज़दूरों को खाना खिलाना था। दारू का इंतज़ाम तो उनकी तरफ से था ही। तिवारीजी ने यारी-दोस्ती में खाना खिलाने का ठेका मनोज को दिलवा दिया। मनोज ने मज़दूरों की खान-पान की आदतों और उससे पहले पिलाई जाने वाली मुफ्त की शराब को देखते हुए २५०० की बजाये ३५०० लोगों के खाने का इंतज़ाम किया। ५०० मज़दूरों की पहली पंगत खाना खाने बैठी और जितना भी खाना तैयार था, सारा का सारा खा गयी। अब अगली पंगत बैठने के लिए तैयार लेकिन खाना भी नहीं और खाना तैयार करने के लिए सामान भी नहीं। हंगामा मच गया। मज़दूर शराब तो वैसे ही पिये हुए थे, तोड़-फोड़ पर उतर आये। मज़दूरों ने रसोई वाले हिस्से में हल्ला बोल दिया। सारे कारीगर प्राण बचाते भागे। पहले तो मनोज भी भागा लेकिन उसे लगा कि उसके भागने से कहीं हालत और न बिगड़ जायें, उसने सबको शांत करते हुए उन पांच छ: सौ मज़दूरों के जमावड़े के सामने माइक के जरिये भाषण देना शुरू कर दिया। मनोज साफ झूठ बोल गया और कहा कि ग़लती खाना बनाने वाले ठेकेदार की नहीं है। ठेकेदार को तो सामान दिया गया था और सिर्फ़ खाना तैयार करके खिलाने का काम सौंपा गया था। अब मज़दूरों का गुस्सा उस व्यापारी पर। उनके खिलाफ नारेबाज़ी होने लगी, नेता लोग आये और कारखाने में हड़ताल की घोषणा हो गयी। जब उस व्यापारी को पता चला कि एक तो मनोज ने सबको खाना नहीं खिलाया और ऊपर से झूठ बोलकर मज़दूरों को उनके खिलाफ भड़का कर हड़ताल भी करवा दी है तो रात को मनोज की पेशी हुई। मनोज ने साफ-साफ कह दिया कि जितने के लिए कहा गया था उससे ज्यादा खाना अगर सदियों से भूखे आपके ५०० मज़दूर खा गये तो मैं क्या करूं। अब मज़दूरों के हाथों पिटने से बचने के लिए कुछ तो करना ही था। जो भी सूझा मैंने बोल दिया।
मनोज से मेरी पहली मुलाक़ात १९९२ में कानपुर में पहले संगमन के मौके पर हुई थी। बेशक वह मौका मेरे लिए एक हादसे की तरह था। कुछ ही दिनों पहले मैं ‘वर्तमान साहित्य’ में अपनी विवादास्पद कहानी ‘उर्फ़ चंदरकला’ की वजह से सारे ज़माने की दुश्मनी मोल चुका था। कहानी सबसे ज़ेहन में ताजा थी। अब हुआ यह कि पहले संगमन के पहले सत्र का संचालन राजेन्द्र राव कर रहे थे। अध्यक्षता राजेन्द्र यादव कर रहे थे और मेरी यही वाली कहानी वे लौटा चुके थे। राजेन्द्र राव ने आव देखा न ताव, सत्र की शुरुआत में ही इस कहानी पर पिल पड़े। मुझे ही सबसे पहले बोलने के लिए आमंत्रित भी कर लिया। वे मुझे सबसे पहले बोलने के लिए आमंत्रित करने वाले हैं, यह मुझे पता नहीं था। किसी भी आयोजन में जाने का ये मेरा पहला ही मौका था। इस हिसाब से मैं सबसे पहली बार ही मिल रहा था। कुल जमा चार-पांच कहानियों की ही पूंजी थी मेरी। नर्वस मैं पहले से था, बाक़ी रही सही कसर राव जी ने पूरी कर दी। इस तरह की धज्जियां उखाड़ने वाली ओपनिंग से मैं गड़बड़ा गया और पता नहीं क्या-क्या बोलने लगा। दो चार मिनट तक बक-बक करने के बाद मैं बैठ गया। ये संगमन की शुरुआत थी जो मैंने बहुत ही बोदे ढंग से की थी। वहीं पर मैं अपनी कथाकार मित्र सुमति अय्यर से पहली और आखि़री बार मिला था। उनसे बरसों से पत्राचार था। कथाकार मित्र अमरीक सिंह दीप से भी लम्बी दोस्ती की शुरुआत वहीं से हुई थी। और वहीं पर मेरी पहली मुलाक़ात मनोज रूपड़ा से हुई।
शाम बहुत ही नाटकीय थी। रात किसी होटल में दैनिक जागरण की तरफ से डिनर का इंतज़ाम था और उससे पहले कहीं तरल गरल का आयोजन था, जिसके लिए चार बजते न बजते गुपचुप रूप से ख़ास दरबारियों को न्योते दिए जाने लगे थे।
जहां हमें ठहराया गया था, वहीं पर शाम के वक्त जयनंदन और मनोज से मेरा विधिवत परिचय हुआ और हम उसी पल दोस्त बन गए। मनोज ने मेरी कहानी पढ़ रखी थी और उसने कहा था कि राजेन्द्र राव तुम्हारी इस कहानी की इस तरह से बखिया उधेड़ने से पहले अपनी ‘कीर्तन’ कहानी का जिक्र करना क्यों भूल गए। उसमें वे कौन से मूल्यों की स्थापना की बात कर रहे थे। उसकी बातों से मेरा दिन भर का बिगड़ा मूड संभला था। तो हुआ यह कि कमरे में कई साहित्यकार मित्र थे जो शाम वाले जमावड़े में न्योते नहीं गए थे और अलग अलग समूहों में बैठे शाम गुज़ारने का जुगाड़ बिठा रहे थे। तभी मनोज ने बताया कि उसके पास हाफ के करीब रम है, अगर कोई उसके साथ शेयर करना चाहे तो स्वागत है। अब मुझे ठीक से याद नहीं कि उस हाफ में से जयनंदन, मनोज और मेरे अलावा किस किस के गिलास भरे गए थे, लेकिन इतना याद है कि यह बैठक मनोज और जयनंदन के साथ एक लम्बी दोस्ती की शुरुआत थी। बाद में जब मनोज अपने काम धंधे के सिलसिले में मुंबई आया तो हम अक्सर मिलते रहे। फोन पर बातें होती रहतीं। कभी कभार बैठकी भी जम जाती। अब मनोज के नागपुर चले जाने के बाद मैं जब भी वहां जाता हूं, वह मेरे लिए भरपूर समय निकालता है। फोन पर अक्सर बात होती ही रहती हैं।
जब पांचवां इन्दु शर्मा कथा सम्मान देने की बात चल रही थी, तब तक इस सम्मान के कर्ता धर्ता और मेरे मित्र तेजेन्द्र शर्मा पारिवारिक कारणों से लंदन जा चुके थे और उनकी हार्दिक इच्छा थी कि कैसे भी हो यह सम्मान चलते रहना चाहिए। वे इसकी सारी जि़म्मेवारी मुझे सौंप गए थे। संस्था की पहली पुस्तक बंबई-एक का सम्पादन भी मैं ही कर रहा था। तेजेन्द्र के लंदन होने के कारण इतना बड़ा आयोजन करने में मेरे सामने दिक्कतें तो आ ही रही थीं।
उन्हीं दिनों मनोज ने बताया कि उसे लंदन में ही अपनी मन पसंद का बहुत बढि़या काम मिल रहा है और वह कैसे भी करके लंदन जाना चाहता है। पासपोर्ट बनवाने के लिए उसने मेरी मदद मांगी थी। शायद घर के पते के प्रमाण को लेकर कुछ तकलीफ आ रही थी।
एक दूसरा संयोग यह हुआ कि तेजेन्द्र ने मुझसे पूछा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस बार यह सम्मान लंदन में ही दिया जाए। टिकट का इंतजाम वह कर देगा। मेहमान को अपने घर पर ठहरा भी देगा और थोड़ा बहुत लंदन घुमा भी देगा। लेकिन इसमें भी दिक्कतें थीं। बेशक तेजन्द्र ने अपने पल्ले से बैंक में इतनी राशि जमा कर रखी थी कि कम से कम दो आयोजन आराम से किए जा सकें, लेकिन एहतियात के तौर पर आयोजन का सारा खर्च स्मारिका छाप कर पूरा किया जाता था। आयोजन लंदन में करने के अपने संकट थे, पूरी व्यवस्था यहीं से करनी होती। सिर्फ़ आयोजन वहां होता। स्मारिका छपवाने से भिजवाने तक। दूसरी बात, उन दिनों कथा सम्मान की शील्ड एक्रेलिक के एक बहुत बड़े बॉक्स में हुआ करती थी। उसे बनवा कर लंदन भिजवाना। और भी कई दिक्कतें थी़।
तेजेन्द्र ने इसका भी समाधान खोजा कि क्यों न ये सारी चीज़ें सम्मान पाने वाला लेखक अपने साथ लंदन लेता आए। पता नहीं क्यों मुझे यह बात हज़म नहीं हुई कि किसी रचनाकार से पूछें कि भई हम तुम्हें लंदन ले जाकर सम्मानित करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें सारा ताम झाम अपने साथ ख़ुद ही लंदन ले जाना होगा।
जब यह तय हो चुका था कि यह सम्मान मनोज रूपड़ा को उसके कहानी संग्रह ‘दफ़न और अन्य कहानियां’ पर दिया जा रहा है और वह ख़ुद लंदन जाने की जुगाड़ में है तो तेजेन्द्र ने कई बार मुझसे कहा कि मैं मनोज से बात करके देखूं। अगर वो राजी है तो हम उसे लंदन में सम्मानित करने की सोच सकते हैं। लेकिन मैं ही संकोच कर गया। मेरे अपने डर थे। मनोज अपना यार-दोस्त है। ख़ुद का सम्मान करवाने के लिए लंदन तक शील्ड ले जाने का बुरा नहीं मानेगा, लेकिन आने वाले वर्षों में सम्मानित होने वाले रचनाकार मुंबई के नहीं होंगे और हो सकता है, परिचित भी न हों। किसी से भी ये कहना कि अपने सम्मान का सामान लंदन लेकर जाओ, मुझे ठीक नहीं लग रहा था। मुझे यह भी डर था कि हिन्दी साहित्य जगत इस प्रस्ताव का ख़ूब माखौल उड़ाएगा। फिर भी आज लगता है कि अगर मैंने मनोज से पूछ ही लिया होता तो शायद वह लंदन जाकर कथा सम्मान लेने वाला पहला लेखक बनता। क्या पता शील्ड वग़ैरह भिजवाने का कोई और इंतजाम हो गया होता और ये भी तो हो सकता था कि एक बार पासपोर्ट बन जाने और लंदन पहुंच जाने के बाद वहां उसे मनपसंद काम मिल गया होता और इस समय वह नागपुर के बजाय लंदन के किसी बाज़ार में जलेबियां छान रहा होता। लेकिन अब ये सब ख्याली पुलाव पकाने का कोई मतलब नहीं। मनोज रूपड़ा ने मुंबई में ही पांचवां इन्दु शर्मा कथा सम्मान प्राप्त किया था और उसके बाद संयोग ऐसा बना कि अगले ही वर्ष से ये सम्मान कथा यूके के तत्वावधान में लंदन में ही दिया जा रहा है और मज़े की बात कि किसी भी सम्मानित लेखक को कुछ भी नहीं ले जाना होता। सारी व्यवस्था आपने आप हो जाती है।
वरिष्ठ कथाकार गोविन्द मिश्र जी के हाथों से सम्मान लेते समय मनोज ने बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात कही थी लेकिन जो कुछ कहा था, वह मायने रखता है। उसने कहा था कि आमतौर पर सम्मानों के साथ कोई न कोई विवाद जुड़ा रहता है लेकिन यह सम्मान लेने में उसे कोई संकोच नहीं हो रहा है क्योंकि ये सम्मान एक लेखक द्वारा अपनी स्वर्गीय लेखिका पत्नी की याद में तीसरे लेखक को दिया जा रहा है और ये एक ईमानदार कोशिश है। मनोज ने अपने इस जुमले पर ख़ूब तालियां बटोरी थीं।
श्रीगंगानगर में २००४ में आयोजित संगमन में एक मज़ेदार किस्सा हुआ। आयोजन की दूसरी शाम की बात है। तरल गरल का इंतजाम किया गया था और कई रचनाकार जुट आए थे। कुछ बुलाए, कुछ बिन बुलाए। दस बारह लोग तो रहे ही होंगे। से रा यात्री, विभांशु दिव्याल, प्रियंवद, कमलेश भट्ट कमल, अमरीक सिंह दीप, ओमा शर्मा, मनोज रूपड़ा आनंद हर्षुल, मोहनदास नैमिशराय, हरि नारायण, देवेन्द्र और मैं वहां थे। शायद संजीव भी थे। दो एक और रहे होंगे। पीने वाले पी रहे थे और सूफी लोग बातें कर रहे थे। जिस तरह की बातें इस तरह के जमावड़े में पीते पिलाते वक्त होती हैं, वही हो रही थीं। तभी मनोज ने बताना शुरू किया कि किस तरह वह पुणे में एक देवदासी के सम्पर्क में आया था और देवदासियों के जीवन को नज़दीक से जानने के मकसद से वह उसके साथ कर्नाटक में कहीं दूर उसके गांव गया था। उसके परिवार से मिला था और उसके घर के सदस्य की तरह वहां दो तीन महीने रहा था। मनोज अपनी रौ में बात किए जा रहा था। तभी नैमिशरायजी ने टोककर उससे देवदासी के बारे में सवाल पूछे कि वह कैसी थी। उसका घरबार कैसा था। क्या उसके पति को और घरवालों को एतराज़ नहीं हुआ, वहां उसके जाने से। उसके बच्चों मां बाप वग़ैरह के बारे में उन्होंने कुछ सवाल पूछे। शायद एकाध सवाल सेक्स को लेकर भी पूछा। यहां मैं एक बात बता दूं कि देवदासियों पर नैमिशरायजी का एक उपन्यास ‘आज बाज़ार बंद है’ कुछ ही दिनों पहले आया था। उस वक्त तो मनोज ने गोलमाल उत्तर दे दिए थे उनके सवालों के, लेकिन बाद में मुझसे अफसोस के साथ कहा कि देवदासियों के जीवन पर पूरा उपन्यास लिखने के बाद वे पूछ रहे हैं कि देवदासी होती क्या है! आखि़र इस तरह के लेखन के क्या मायने होते हैं।
मनोज बेहतरीन कारीगर हैं। शब्द शिल्पी तो वो है ही। कई तरह की मिठाइयां और नमकीन बनाने के प्रयोग करता रहता है। वह दोनों जगह सफल हैं। लेखन में भी और धंधे में भी। हाल में ही उसने नागपुर में अपनी देखरेख में अपना ख़ूबसूरत घर भी बनवाया है। उसमें उसने लेखकों के लिए अलग से दो कमरे बनावाए हैं, जहां कोई भी लेखक (लेखिका भी) आराम से दो चार दिन गुज़ार सकता है।
लेकिन एक बात है। मनोज थोड़ा सा शेख चिल्ली भी है। जिस काम की उसे कोई समझ नहीं होती, उसमें भी हाथ डालकर दो चार लाख रुपये गंवाना उसे बहुत अच्छा लगता है। उसने कई धंधे शुरू किए और तगड़ा घाटा उठाने के बाद बंद भी किए। एक बार उसने मुंबई से १६० किलोमीटर दूर रसगुल्ले बनाने का कारखाना लगवाया था। पता नहीं कितने बने और कितने बिके, लेकिन हमेशा की तरह उसने ख़ूब घाटा उठाकर धंधा बंद कर दिया। सीधा वह इतना है कि उसे आसानी से बुद्धू बनाकर उससे पैसे झटके जा सकते हैं। मुंबई के पांच सात बरस के प्रवास में कम से कम उसे १५ लाख रुपये का चूना तो लोगों ने लगाया ही होगा। लोगबाग उससे माल सप्लाई करने के बहाने पैसे ले जाते हैं और दोबारा कम से कम इस जनम में वे अपना चेहरा दोबारा नहीं ही दिखाते। एक नहीं कई हैं जिन्होने बाकायदा मनोज रूपड़ा को दुहा है और कई बार दुहा है।
वह नुकसान उठाने के लिए हमेशा तैयार रहता है और नुकसान उठाने के लिए नये नये तरीके ढूंढता रहता है। ये मनोज के साथ ही हो सकता है कि उसे दस लाख की कीमत पर एक ऐसा मकान बेच दिया गया हो, जो पहले ही दो आदमियों को बेचा जा चुका था। मनोज के हाथ में आश्वासन तक नहीं आया कि इसके बदले तुम्हे दूसरा मकान दे देते हैं।
एक और मज़ेदार किस्सा हुआ उसके साथ। घाटकोपर में उसके कारखाने मे पास ही दोपहर के वक्त कोई लड़का घबराया हुआ आया और लोगों से कहने लगा कि मुझे कहीं छुपा लो, गुंडे मेरे पीछे लगे हैं। जब उसे पानी वानी पिलाया गया तो उसने बताया कि उसकी पांच लाख की लाटरी लगी है और गुंडे टिकट छीनने की फिराक में हैं और वह जान बचाता फिर रहा है। बहुत डरते डरते उसने लाटरी की टिकट और अख़बार में छपा लाटरी का परिणाम दिखाया जिसमें पहला ईनाम उसी नम्बर पर था। उस लड़के ने तब कहा कि वह कैसे भी करके इस टिकट से जान छुड़ाना चाहता है ताकि उसकी जान बची रहे। आखि़र सामूहिक रूप से सौदा पटा और शायद तीन लाख में कुछ लोगों ने मिलकर उससे वह टिकट ख़रीद लिया। अपने मनोज भाई भी उनमें से एक थे, बल्कि सबसे आगे थे।
जब ईनाम का दावा करने के लिए टिकट पेश किया गया तो पता चला कि ये स्कैन करके प्रिंट किया हुआ डुप्लीकेट टिकट था और इसी टिकट पर ईनाम के पांच दावेदार पहले ही आ चुके हैं।
तो ऐसे हैं अपने मनोज भाई। यारों के यार। खाने पीने और खिलाने पिलाने के शौकीन। घुमक्कड़ी का कोई मौका नहीं छोड़ते। उसकी घुम्मकड़ी का ये आलम था कि जब दुर्ग में दुकान पर बैठता था तो जब भी मन करे, गल्ले में से पैसे निकाले, शटर गिराए और घर में बिना बताए कहीं भी अकेले ही घूमने निकल जाया करते। बाद में जब स्वर्गीय कथाकार पूरन हार्डी का साथ मिला तो दूर दूर की यात्राएं कीं। उसके साथ घूमने की वजहें भी थीं। पूरन रेल्वे में था और मनोज के लिए डुप्लिकेट रेल्वे पास का इंतजाम कर दिया करता था। एक बार इसी तरह वह गोवा जा पहुंचा और मस्ती मारता रहा। पास में जितने पैसे थे, खत्म हो गए। उन्हीं दिनों गोवा में हबीब तनवीर साहब के नाटकों का उत्सव चल रहा था। मनोज साहब उसका लालच कैसे छोड़ें। अटैची होटल के रिसेप्शन पर रखी थी। हफ्ते भर वहीं रखी रही। तो ढूंढते ढांढते मनोज जी को समुद्र तट पर एक मज़ार मिल गई। रात के डेरे की समस्या हल हुई। थोड़ा बहुत पेट में डालकर नाटक देखते। वापसी की यात्रा बिना टिकट के हुई। बस, पकड़े नहीं गए।
मनोज की एक बहुत अच्छी आदत है कि बस में, ट्रेन में चीज़े भूल जाएंगे। मेरे घर रात गुजारी (मेरे घर का मतलब मेरा ही घर है, कहीं और नहीं) तो पर्स वहीं भूल जाएंगे। पता नहीं बस टिकट का इंतज़ाम कैसे करते होंगे। बसों में सामान भूलने में तो जनाब को महारत हासिल है। अपनी बनाई मिठाइयां और नमकीन तो हर बार बस में ही छोड़ आते हैं। एक बार राजकोट में ट्रेन में मनोज की अटैची चोरी चली गई। अब क्या हो! शायद पैसे भी उसी में थे। राजकोट से अहमदाबाद आए और वहां से भोपाल। देखते क्या हैं कि एक आदमी सामने ही उनकी अटैची लिए जा रहा है। मनोज को लगा कि यार ये अटैची तो जानी पहचानी लग रही है। फिर याद आया कि ये तो अपनी ही है जो परसों राजकोट में चोरी चली गई थी। उस भले आदमी को रोका, उससे झगड़ा हुआ, उसे अटैची के भीतर की सारी चीज़ों के बारे में बताया, तभी उसे वापिस ले सके।
लेकिन हर बार मनोज किस्मत के इतने धनी नहीं होते। जो खो गया उसे भुलाता चला गया। कभी मनोज से पूछूंगा कि जब गुमशुदा चीज़ों की गिनती सौ तक पहुंच जाए तो बताना। गुमशुदा शतक मनाएंगे।
मनोज ख़ूब पढ़ते हैं और किताबें ख़रीदकर पढ़ते हैं। जब से नागपुर गए हैं, संगीत के कार्यक्रमों में ज्यादा जाने लगे हैं। और अब तो अपनी प्यारी और बहुत हंसमुख पत्नी मीता और उससे भी ज्यादा प्यारी और नटखट बच्चियों चार्मी और प्रीतू को भी साथ ले जाने लगे हैं। वे नागपुर में पढ़ रहे मेरे बेटे के लोकल गार्जियन हैं और यदा कदा अपना फ़र्ज़ निभाते रहते हैं। हिन्दी के सभी छोटे बड़े लेखक मनोज के दोस्त हैं, लेकिन सगे दोस्त आनंद हर्षुल और जयशंकर ही हैं।
उसकी एक बहुत अच्छी बात है कि वह जिस दोस्त के घर भी जाता है, वहां घर परिवार के सदस्य की तरह रह लेता है। कम से कम चीज़ों में गुज़ारा कर लेता है। खाने-पीने के कोई नखरे नहीं करता। ऐसे में मेज़बान दोस्त की पत्नी की तारीफ उसका काम और आसान कर देती है।
मनोज की प्रेमिकाओं के बारे में मुझे पता नहीं है। वैसे वह बीच बीच में न्यूज़ीलैंड का जिक्र करता रहता है कि कभी वहां जाना है। इस बार जब वह फि़ल्में देखने पुणे आया तो नागपुर स्टेशन पर उसने रास्ते में पढ़ने के लिए जानते हैं क्या ख़रीदा ? दुनिया का नक्शा। सत्रह घंटे की यात्रा में वह उसमें न्यूज़ीलैंड ही खोजता रहा। वह सवेरे चार बजे मेरे घर पहुंचा था। उसने पहला काम ये किया कि मुझे नक्शा देते हुए न्यूज़ीलैंड खोजकर दिखाने को कहा। जब उसने देखा कि न्यूज़ीलैंड तो भारत से बहुत दूर है तो थोड़ा निराश हो गया था।
मनोज ने बहुत कम लिखा है। शायद पंद्रह बरस में पंद्रह कहानियां और पिछले दिनों पहला उपन्यास। लेकिन जो भी लिखा है, उसे यूं ही दरकिनार नहीं किया जा सकता। अभी उसे एक बहुत लम्बी पारी खेलनी है। लेखन की, यारबाशी की और अपनी तरह से अपनी शर्तों पर जीवन जीने की भी। उसकी इच्छा है कि अगले जन्म में वह भी मेरी तरह रिज़र्व बैंक की नौकरी करे, जहां खूब यात्राएं होती हैं और बकौल मनोज सारी सुविधाओं के बावजूद काम धेले का नहीं करना पड़ता। कहावत है कि अपने बच्चे और दूसरे की बीवी सबको अच्छी लगती है। मनोज ने इस सूची में मेरी नौकरी को भी शामिल कर लिया है।
ज़हे नसीब !
अप्रैल 2005

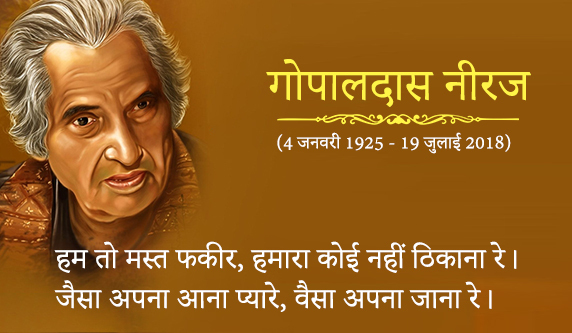



No Comments