आज पता नहीं क्यों, नामी मास्टर याद आ रहे हैं। उनसे आखिरी बार पढ़े और मार खाये 45 बरस तो बीत ही गये होंगे। पता नहीं वे अब हैं भी या नहीं। अगर होंगे भी तो इस समय कम से कम 85 बरस के तो होंगे ही। मैं ही साठ पार कर गया। उनसे आखिरी बार उस वक्त मुलाकात हुई थी जब वे रिटायर होने के बाद अपने ही घर के नीचे दूध की एक डेयरी चला रहे थे। उनकी नज़र कमज़ोर हो चुकी थी और उन्हें सुनायी भी कम देने लगा था। जब मैंने उनके पैर छूए थे और उन्हें याद दिलाया था तो उन्हें मेरा नाम याद आ गया था। इस बात को भी बीसेक बरस तो बीत ही चुके होंगे।
उनका असली नाम तो राम स्वरूप भाटिया था लेकिन वे अपने मोहल्ले में, बिरादरी में और जान पहचान वालों में नामी मास्टर के नाम से ही जाने जाते थे। बेशक स्कूल की चारदीवारी के भीतर वे हमारे भाटिया, आरट टीचर थे। पूरे नाम की ज़रूरत किसे पड़ती थी। पता भी किसे था। बाकी सब जगह नामी मास्टर। वे खुद को आरट टीचर ही कहते थे। कई शब्द ऐसे थे जिनके उच्चारण वे अपने तरीके से करते थे या यूं कहें कि वे कई शब्दों का सही उच्चारण कर ही नहीं पाते थे। आगे चल कर ऐसे कई शब्द इस कहानी में आयेंगे।
वे हरफनमौला थे। अगर कोई शब्द हरधनमौला होता हो तो दरअसल वे यही थे। इसकी वजह ये थी कि धन से जुड़ा कोई भी काम हो वे आधी रात को भी करने के लिए तैयार थे या यूं कहें कि वह हर काम में अपने लायक कुछ कमाने की गुंजाइश आधी रात को भी निकाल सकते थे। निकालते भी थे। वे किसी भी काम में अपना हिस्सा पैदा करने या हथियाने में माहिर थे। एक बहुत पुराना किस्सा जिसमें जिसे लहरें गिनने के काम में भी कमाने की जुगाड़ बिठा लेना कहते हैं, वे कर सकते थे। स्कूल में या जीवन में भी जहां कहीं भी धन की बात हो, वे वहां मौजूद होते थे। खासकर वहां जहां कमाने की गुंजाइश हो, न भी हो तो वे अपनी जगह बना ही लेते थे।
कहा तो यही जाता था कि वे हमारे स्कूल के सबसे कम पढ़े लिखे मास्टर थे। सिर्फ दसवीं पास जो दसवीं तक को पढ़ाते थे। वो भी पता नहीं थे या नहीं, क्योंकि बताते हैं कि वे जब देश के बंटवारे के समय पाकिस्तान से आये थे तो नौकरी की तलाश में दर दर भटकते सब जगह उन्होंने यही रोना रोया था कि वे पाकिस्तान से अपने परिवार के साथ खाली हाथ ही आ पाये थे और उनका सब कुछ पीछे छूट गया था। और इस तरह से ड्राइंग मास्टर की ये नौकरी मिली थी उन्हें।
लोग बाग तो ये भी बताते हैं कि सन 1950 के आसपास जब हमारे स्कूल की नींव रखी जा रही थी तो वे यहां पर मजदूर की हैसियत से ईंट गारा ढोया करते थे और स्कूल की ज्यादातर दीवारों को खड़ा करने में उनके हाथों की मेहनत का भी करिश्मा था। वे खुद भी कई बार ये बात गर्व से बताया करते थे कि इस स्कूल को खड़ा करने के पीछे उनकी मेहनत का भी योगदान है। बाद में वे सारे मजदूरों के मेट और फिर ठेकेदार बन गये थे। स्कूल के बीचों बीच बना पार्क उन्हीं का बनवाया या बनाया हुआ है। स्कूल की इमारतों में सीमित बजट के चलते जितना भी निखार लाया जा सकता था या जहां जहां फूलपत्ती आदि बनाये जा सकते थे, ये सब उन्हीं का काम था और इस तरह वे स्कूल बनने के साथ वे स्थायी रूप से अंदर आ गये थे। यही कहानी ज्यादा विश्वसनीय मानी जाती रही है क्योंकि ये उनके चरित्र के ज्यादा नजदीक बैठती है।
एक बात और भी इस कहानी के पक्ष में जाती है कि स्कूल के विस्तार का काम लगातार बरसों तक चलता रहा था। जब भी कहीं से कुछ धन का जुगाड़ होता, एकाध नया कमरा खड़ा कर ही लिया जाता। गरमियों की या दूसरी छुट्टियों में स्कूल में बारातें ठहराना भी इस तरह की धन उगाही का एक जरिया था और बताते हैं कि इसके पीछे भी अक्सर नामी मास्टर का हाथ रहता।
स्कूल जब शुरू हुआ था तो आठवीं तक का था और हमारे आते आते यहां पहले दसवीं तक की और फिर बारहवीं तक की पढ़ाई होने लगी थी। हर बरस कभी लैब बन रही होती कहीं हॉल या कभी नयी कक्षाओं के लिए कमरे तो कभी बड़ा सभा भवन। बेशक वे अब ईंट गारा न ढोते हों फिर भी सारे निर्माण कार्य की देखभाल, सीमेंट रेती का हिसाब किताब और अपनी पसंद के मिस्त्री के रखना तो वे कर ही सकते थे और करते भी थे। दोनों तरफ से अपना हिस्सा रखते हुए। संभव है स्कूल के भीतर पैठ बनाने और कैरियर बनाने की नामी मास्टर की शुरुआत ऐसे ही हुई होगी। जब मास्टरों की भर्तियां शुरू हुई होंगी तो छोटी क्लासों के लिए ड्राइंग मास्टर के रूप में उन्हें रख लिया गया होगा और धीरे धीरे तरक्की करते हुए उन्होंने दसवीं तक की क्लासों को पढ़ाने की जुगत भिड़ा ली होगी। आखिर ड्राइंग ही एक ऐसा विषय होता है जिसमें अक्षर ज्ञान की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब अगर वे अनपढ़ भी रहे हों तो भी क्या फर्क पड़ने वाला था। उन्हें भी पढ़ाते समय पूरे कैरियर में कभी भी एक से जेड तक के अक्षर भी नहीं लिखने पड़े होंगे।
हमें वे जो ड्राइंग पढा़ते थे उसके दो हिस्से थे। विशुद्ध कला पक्ष जिसमें वे हमें ड्राइंग शीट्स पर सुराही, गिलास, घड़ा या ऐसी ही चीजों की आकृति बनाना और उसमें शेड करना सिखाते थे। शायद वे इन पाँच सात घरेलू चीजों की ड्राइंग बनाना ही जानते थे और बरसों बरस, पीढ़ी दर पीढ़ी यही बनवाते चले आ रहे थे। इसमें भी उन्हें करना कुछ नहीं होता था। क्लास में आते ही अपना झोला डंडा मेज में रखते, और ब्लैक बोर्ड पर इन गिनी चुनी चीजों में से एकाध बना कर हमें हुक्म सुना देते कि बनाओ इसे। एक बात थी कि उनका हाथ बहुत साफ था और नाप का अनुपात ग़ज़ब का। वे ब्लैक बोर्ड पर एक ही बार में जो भी बनाते वह हर कोण से इतना बराबर होता कि नापने पर मिलीमीटर तक सही आता। और यही सफाई और परफैक्शन वे हमसे चाहते।
उनके पास सभी कक्षाओं में पढ़ाने की जो दूसरी आइटम होती थी, वह थी हस्तकला। यानी कागज और गत्ते की मदद से घरेलू उपयोगी चीजें बनाना। मसलन दीवार पर टांगने के तिकोने पैन स्टैंड जिसे हम शायद दीवालगिरी कहते थे। इसी तरह की कई चीजें वे हमें बनाना सिखाते। गत्ते और रंगीन कागज ले कर उनसे डिब्बे, गिफ्ट बाक्स, स्टेशनरी बॉक्स वगैरह बनाना। ये बात अलग होती कि मेहनत और बहुत मुश्किल से जुटाये गये पैसे से बनायी ये चीजें शायद ही हमारे कभी काम ही आती। या तो इन्हें घर में रखने की जगह ही न होती, या इनका कोई उपयोग ही न होता। लेकिन इन्हें बनाना जरूरी होता। क्लास के लिए भी और परीक्षा के लिए भी। ये बहुत मेहनत का और खर्चीला काम होता।
ये बात मैं बता ही चुका कि नामी मास्टर बहुत सफाई पसंद थे और इसी सफाई पसंदगी के चलते उनकी दुकानदारी और सबकी पिटाई के सेशन एक साथ चलते थे। ऊपर मैंने उनके जिस झोले डंडे की जिक्र किया है दरअसल वह उनकी चलती फिरती दुकान होती थी। एक भारी सा बैग, एक फाइल फोल्डर, कोट की सारी जेबें ये सब उनकी चलती फिरती दुकान की अलमारियां थीं जिनमें जरूरत, मांग और मांग के हिसाब से सामान ठूंस ठूंस कर भरा होता। ड्राइंग पेपर, इरेजर जिसे तब हम रबड़ के नाम से जानते थे, पैंसिल, परकार, लकड़ी और प्लास्टिक के स्केल, रंगीन कागज, शार्पनर यानी उनकी कक्षा में इस्तेमाल होने वाला सारा सामान उनसे क्लास में ही नकद और बहुत मजबूरी हो तो एक दिन के उधार पर खरीदा जा सकता था। जिसकी भी ड्राइंग कॉपी में पन्ने कम नज़र आते, परकार खराब हो चुकी होती, सफेद दीवार पर रगड़ने के बाद भी रबड़ का कालापन न जा पाता या स्केल सीधी रेखाएं खींचने के लायक न रहतीं, ऐसे बच्चों को मजबूरन उनका उधारी ग्राहक बनना ही होता।
ऐसा न करने पर उनकी मार खानी पड़ती। मारने का तरीका उनका एकदम मौलिक था। वे डंडे या स्केल का प्रयोग न करते। पढ़ाते समय वे बच्चों को अपने पास न बुला कर हर बच्चे के पास अपनी पूरी दुकानदारी और मार लेकर चलते। वे बेशक हर बच्चे के परिवार से परिचित थे और किसी भी बच्चे के घर की माली हालत उनसे छिपी नहीं थी लेकिन इससे उनकी दुकानदारी और मार की मात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे दोनों मामलों में पक्के समाजवादी थे।
जरा सा का भी काम मनमाफिक न मिलने पर, ड्राइंग बॉक्स पूरा न मिलने पर जो कभी मिलते ही नहीं थे, वे हर बच्चे के लिए एक ही गाली का प्रयोग करते – बेवाकूफ के बच्चे, आरट तेरे बाप के बस की नहीं है, ली क्यूं। अब ले ही ली है तो ढंग से सीख और कुछ बन कर दिखा। और ये कहते कहते अपने दायें हाथ के अंगूठे और पहली उँगली से हमारी बांह घेर कर इतनी बुरी तरह से मसलते कि रोना आ जाता। पूरे स्कूल में उनका कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं था जिसकी बांह पर उनकी बनायी चित्रकारी के पांच सात स्थायी निशान न हों। पिछले निशान गये न होते और वे नये बना चुके होते।
हां, कुछेक बच्चे किस्मत वाले थे जो उनकी मार से बच जाते। या तो उसके लिए उनकी गुड बुक्स में बहुत अच्छा होना होता या उनकी सारी दुकानदारी का स्थायी ग्राहक। दोनों ही बातें मेरे जैसे किसी भी बच्चे के बस में नहीं थी। कई बार तो ऐसा भी होता कि दसवीं में पढ़ने वाले मेरे दोनों भाई और नौंवीं में पढ़ने वाला मैं, तीनों ही एक जैसे दाग अपनी बाहों पर टैटू की तरह सजाये घर आते और घर पर भी इनकी वजह से मार या डांट खाते। मजे की बात ये भी होती कि कभी दुकानदारी का कुछ सामान कम हो जाने पर मुझे ही स्कूल के पास ही नयी खुली दौलत राम की स्टेशनरी की दुकान पर भगाते। वह हमारा रिश्तेदार था और नामी मास्टर अपना सामान वहीं से लेते थे। मुझे पता होता था कि जो ड्राइंग पैंसिल मैं दौलत राम से नकद पैसे होने पर 20 पैसे में खरीद सकता था, वही पैंसिल मुझे खुद ला कर नामी मास्टर से 25 पैसे में खरीदनी होती।
ये बात हमारे इस स्कूल में आने से पहले की है। शायद चीन की लड़ाई से भी बहुत पहले की। मैं इस स्कूल में 1964 में छठी कक्षा में आया था। यानी तब हमें आरट मास्टर ने पढ़ाना शुरू नहीं किया था। जब हम आये थे तो हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य चंद्र भान जी थे। बताते हैं कि उनसे पहले के प्रधानाचार्य परमानंद पांचाल को अचानक हटा दिया गया था और उनकी जगह पर आठवीं के क्लास टीचर चंद्र भान जी को प्रधानाचार्य बना दिया गया था। सीनियर लोग और कई बार मास्टर लोग भी बताते थे कि परमानंद पांचाल बहुत अनुशासनप्रिय प्रधानाचार्य थे और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनकी बात का जवाब भी दे सके। उनकी गूंजती और कड़क आवाज किसी की भी सिट्टी पिट्टी गुम करने के लिए काफी होती थी।
बहुत बाद में नंदू के जरिये हमें सारी बात पता चली थी। मेरा सहपाठी, दोस्त और पड़ोसी नंदू गौड़ मास्टर जी के यहां गणित की ट्यूशन पढ़ता था। वैसे तो वह सभी विषयों की ट्यूशन पढ़ता था लेकिन गणित में खास कमजोर था। गौड़ साहब ने बात चलने पर बताया था कि पांचाल जी के स्कूल से निकाले जाने के पीछे खुद उनका इतना कसूर नहीं था जितना नामी मास्टर का। वे फंस गये थे। दरअसल जब गर्मियों की छुट्टियों में स्कूल का एक पूरा नया ब्लाक बन रहा था तो उसी समय परमानंद पांचाल जी के घर की दूसरी मंजिल भी बन रही थी। गौड़ जी के अनुसार वहां लगने वाला सारा सामान स्कूल के सामान से ही निकल कर वहां पहुंच रहा था और इसके पीछे कहीं न कहीं नामी मास्टर की सलाह और योजना का ही हाथ था। अचानक किसी ने शिकायत कर दी थी कि पांचाल जी का घर स्कूल के सामान से बन रहा है तो वे धर लिये गये थे। जब केस बना तो नामी मास्टर के खिलाफ एक भी सबूत जुटाया नहीं जा सका था और परमानंद पांचाल जी फंस गये थे और बहुत शर्मिंदगी के साथ उन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ा था।
बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे किस्से हैं और बहुत सारे जीते जागते लतीफे भी हैं जो नामी मास्टर के बारे में आज याद आ रहे हैं। इनके पीछे कितना सच है और कितना मनगढंत, ये तो बताने वाले जाने लेकिन मैं खुद उनकी कई मनोरंजक बातों और आदतों का गवाह रहा हूं और आज वही सब याद भी आ रहे हैं और आपसे शेयर करने का मन है।
बात शुरू से शुरू करते हैं। एक बात और, नामी मास्टर जी के बारे में बात करते हुए हो सकता है कि मुझे कुछ और भी मास्टर पढ़ाने के अपने अनोखे ढंग या पढ़ाई से इतर कारणों से याद आयें या स्कूल की उस वक्त की कुछ बातें याद आयें और मैं साथ साथ उन्हें भी शेयर करता चलूं तो आप अन्यथा नहीं लेंगे। ये भी कहा जा सकता है कि आज नामी मास्टर जी के बहाने डाउन मेमोरी लेन उतरने की मासूम सी इच्छा है।
हमारे स्कूल में तीन ही लोग अपने अपने चैम्बर में बैठते थे। प्रधानाचार्य जी का ही चेम्बर ऐसा था जिसमें दसेक लोग बैठ सकते थे। उप प्रधानाचार्य का चेम्बर एक गलियारे को छेक कर बनाया गया गली नुमा कमरा ही था जिसमें उनकी कुर्सी, मेज और अलमारी के बाद मुश्किल से एक ही मेहमान के बैठने की जगह बचती थी। वैसे भी उनके चैम्बर में किसी को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पता नहीं वे वहां खुद भी बैठते थे या नहीं।
नामी मास्टर ऐसे तीसरे व्यक्ति थे जिनके पास एक नहीं दो चेम्बर थे। एक उनका अपना और एक स्पोर्ट्स रूम के नाम पर हथियाया हुआ। उनका चेम्बर भी उनके खुद के व्यक्तित्व की तरह मल्टी फंक्शनल था।
दरअसल वे स्कूल में हर दिन सभी बच्चों को दिये जाने वाले नाश्ते के भी इंचार्ज थे। मिड डे मील की महिमा तो अब सुनायी देने लगी है। ये बात 1964 की है जब हमें नाश्ते के नाम पर हफ्ते में तीन दिन बिस्किट, दो दिन केले और एक दिन भुने हुए चने मिलते थे। बेशक इसके लिए हमारी फीस के साथ पचास पैसे महीने के कटते। हर दिन हाज़िरी के बाद हर क्लास का मानीटर ऑफिस में हाज़िरी रजिस्टर वापिस रखने जाते समय नामी मास्टर के चेम्बर के पास बने एक बोर्ड पर उपस्थित छात्रों की संख्या लिख आता। इस संख्या के आधार पर नामी मास्टर हर क्लास के लिए नाश्ते की ट्रे तैयार करते। इंटरवल की घंटी से पाँच मिनट पहले एक घंटी बजती। तब मानीटर एक साथी को ले कर नाश्ते की ये ट्रे लाता और सब बच्चों में नाश्ता बांटा जाता। तय है सभी मानीटर उपस्थित बच्चों की संख्या दो चार ज्यादा ही लिखते और ट्रे वापिस करने जाते समय बाकी बचा नाश्ता आपस में बांट लेते।
बिस्किट का तो फिर भी ठीक था, केले और चने बेहद खराब क्वालिटी के होते। केले कभी कच्चे तो कभी ज्यादा पके। शिकायत करने की परम्परा नहीं थी। वैसे भी स्कूल में किसी भी बात की शिकायत करने का मतलब अतिरिक्त मार खाना ही होता था।
जहां तक स्पोर्ट्स रूम का सवाल था, उसके पट साल में एक बार तभी खुलते थे जब स्पोर्ट्स का पुराना सामान नीलाम किया जाना होता। पूरे साल लाख गिड़गिड़ाने पर भी किसी को भी फुटबाल या वॉली बाल के अलावा कुछ भी न मिलता। हम बैडमिंटन खेलना चाहते लेकिन सामान के बदले डांट ही मिलती। फुटबाल या वॉली बाल की बॉल भी सदियों पुरानी ही इश्यू की जाती। हम इस बात को कभी समझ नहीं पाये कि बरस भर कभी भी किसी भी बच्चे को गिल्ली डंडा तक न देने वाले नामी मास्टर के पास स्कूल के आखिरी दिनों में नीलामी के लिए सारा का सारा पुराना सामान कहां से आ जाता। उनकी नीलामी एक तरह से जबरदस्ती वाली सेल की ही तरह होती जिसमें हम गली मोहल्लों में रहने वाले गरीब बच्चों के मत्थे बेकार के क्रिकेट बैट, फटे हुए वॉली बाल नेट या फुट बॉल नेट मढ़ दिये जाते। साल भर नया सामान एक बार भी देखने को न मिलता और नीलामी के समय सारा पुराना तामझाम बिक रहा होता।
वैसे हमारा स्कूल शहर के अच्छे स्कूलों में से एक समझा जाता। तब तक अंग्रेजी स्कूलों की बहार नहीं आयी थी। बेशक नामी मास्टर स्पोटर्स के सामान पर कुछ भी न देते लेकिन हमारे स्कूल में हमेशा अच्छे धावक रहे थे जो शहर में और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में अपना और स्कूल का नाम रौशन करते ही थे। इसी तरह से स्कूल के पास हमेशा अच्छे वक्ता रहते ही थे जो विभिन्न वाद विवाद प्रतियोगिताओं की चल वैजयंती जीत कर लाते ही थे। तीन वर्ष तक लगातार कोई प्रतियोगिता जीतने पर वह वैजयंती स्कूल की ही हो जाती। ये और कुछ और कारण थे जिनकी वजह से दूर दराज के गांवों के बच्चे भी हमारे स्कूल में आना पसंद करते। उन्हें और दूर रहने वाले दूसरे बच्चों को भी मजबूरन साइकिलों पर आना पड़ता। ऐसे ही में जब लगभग 10 किमी दूर से आने वाले एक गरीब बच्चे की साइकिल चोरी हो गयी तो जैसे हंगामा मच गया। वह कैसे भी करके रोजाना बीस किमी चल कर स्कूल नहीं आ जा सकता था। वह प्रधानाचार्य के सामने बहुत रोया धोया था।
अगले दिन प्रधानाचार्य ने प्रार्थना सभा में दो घोषणाएं की थीं। नयी साइकिल लगभग 200 रुपये की आती थी। सभी विद्यार्थियों से कहा गया कि सभी बच्चे और अध्यापक स्वेच्छा से दो आने, चार आने उस बच्चे की साइकिल के लिए दान में दें। बाकी कमी बेसी स्कूल की तरफ से पूरी की जायेगी ताकि बच्चे को एक नयी साइकिल उपहार में दी जा सके। संयोग से उसी दिन सारी रकम जुटा ली गयी थी और वह लड़का नयी साइकिल पर बैठ कर अपने घर गया था।
दूसरी घोषणा स्कूल में पार्क के सामने वाली खाली जगह में साइकिल स्टैंड बनाने की थी जहां कम से कम 100 साइकिलें आराम से खड़ी की जा सकती थीं। इसके लिए साइकिल लाने वाले बच्चों को एक रुपया महीना देना होता। इस साइकिल स्टैंड का मैनेजमेंट भी नामी मास्टर ने ही हथिया लिया था।
पता नहीं ऐसे कैसे होता जाता कि पैसे से जुड़ा स्कूल का कोई भी मामला होता, सब पहले से जानते थे कि इसके लिए नामी मास्टर की झोली ही ठीक रहेगी। शायद इसके पीछे ये कारण भी रहा हो कि बाकी मास्टरों को अपने अपने विषय की ट्यूशन पढ़ाने से ही फुर्सत न मिलती। हिंदी मास्टर के सिवाय सभी मास्टर सुबह 6 बजे ही अपने घरों में ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देते। कई बच्चे तो जरूरत न होने पर भी सिर्फ इसलिए पढ़ते कि रोज रोज की मार से बचे रहें और उससे बड़ा लालच से रहता था कि लगभग सभी मास्टर वेरी वेरी इम्पार्टेंट क्वेश्चंस के नाम पर पूरा पेपर ही लीक कर दिया करते थे। अब ये उन बच्चों पर होता कि पूरा पेपर हाथ में आ जाने के बाद भी उसके साथ कितना न्याय कर पाते थे।
मार हमारे स्कूल का स्थायी भाव था। सारे मास्टर अपने अपने कारणों से और अपने अपने तरीके से पीटते ही थे। और इस मार से बचने का एक ही तरीका होता कि ट्यूशन पढ़ो। बात बे बात की मार से बचने के जो सफल और आजमाये हुए तरीके थे, वे महंगे थे और उनमें हम फेल थे। घर की माली हालत के चलते और पढ़ाई में ठीक ठीक होने के कारण हम भाइयों में से कोई भी ट्यूशन नहीं लेता था।
शायद आठवीं की छमाही परीक्षाओं की बात रही होगी। अचानक नंदू ट्यूशन से लौटा था। उत्साहित भी और घबराया हुआ भी। एक कागज था उसके हाथ में। सिर्फ 6 प्रश्न लिखे थे। वेरी वेरी इम्पार्टेंट क्वेश्चंस। छमाही परीक्षा में 30 नम्बर के 6 ही सवाल पूछे जाते थे। नंदू तीन घंटे ट्यूशन पढ़ कर आया था फिर भी उनमें से उसे एक भी सवाल हल करना नहीं आता था। मेरी मदद लेने आया था। हमने लालटेन की रौशनी में वे 6 सवाल हल किये थे।
इसे संयोग कहा जायेगा या ट्यूशन के पैसों का लालच कि वे और वही सवाल अगले दिन पेपर में पूछे गये थे। मैंने तीस में से 30 अंक पाये थे और नंदू ने 12 ही। एक और चमत्कार हुआ था उस बरस। छमाही परीक्षा में पास होने वाला मैं पूरी कक्षा का इकलौता विद्यार्थी रहा था।
बात हो रही थी नामी मास्टर की और बीच में आ गये ट्यूशन वाले। नामी मास्टर के किसी रिश्तेदार ने एक पुरानी बस खरीदी थी जो शादियों वगैरह के लिए चलती थी। उन दिनों शादियों का सीजन नहीं था और बस घर पर खड़ी थी। नामी मास्टर और रिश्तेदार ने मिल कर योजना बनायी कि बच्चों को दिल्ली, आगरा और मथुरा की सैर करायी जाये। बस रिश्तेदार की होती, खाने का इंतजाम नामी मास्टर का और ठहराना स्कूलों में। ऐसे कामों के लिए नामी मास्टर प्रधानाचार्य को पटाने में महारत रखते थे। पूरी योजना बन गयी और नामी मास्टर ये खुशखबरी हर क्लास में खुद सुना आये। दिल्ली, आगरा, मथुरा, वृंदावन वगैरह। बहुत खुशखबरियां सुनाने के बावजूद नामी मास्टर इतने बच्चे और मास्टर नहीं जुटा पाये कि खर्चा पानी निकलता।
तभी एक दिन नामी मास्टर किसी और पीरियड के बीच चले आये। उनके लिए ये सामान्य बात थी कि कभी भी किसी भी क्लास में चले जाते। आते ही जोर जोर से चिल्लाने लगे- खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। अब यात्रा गवलियार तक बढ़ा दी गयी है। ये बात अलग है कि उन्हीं पैसों में गवलियार तक की यात्रा कराने की उनकी योजना सफल नहीं हो पायी थी।
आठवीं के बाद जब साइंस या आर्ट्स या कॉमर्स लेने की बात आती तो बच्चे समझ न पाते कि किस स्ट्रीम में जायें। सब बच्चों के घर वालों को इतनी समझ न होती कि बता बाते। नतीजा यही होता कि बच्चे परिचित मास्टरों और सीनियर बच्चों से पूछते फिरते। कई बच्चे नामी मास्टर के पास आते। मास्टर जी उसका आठवीं का रिजल्ट देखते, उसे तौलते, उसमें अगले दो बरस के लिए ग्राहक बने रहने की संभावनाएं तलाशते और फिर बताते – बेवाकूफ के बच्चे, सेंस ले ले, बयालोजी ले ले, जोगरफी या कोमरस ले ले, आरट तेरे बाप के बस की नहीं है। ये बात अलग होती कि देर सबेर सारे बच्चे आर्ट ही लेना पसंद करते थे। बेशक यहां मार थी और फालतू का सामान खरीदना होता लेकिन इस विषय का सबसे बड़ा फायदा ये होता था कि एक विषय कम पढ़ना या रटना होता था। आर्ट्स में याद करने या ट्यूशन पढ़ने जैसा कुछ भी नहीं होता था। थोड़ा बहुत गिड़गिडाने के बाद वे सबको आर्ट्स में आने देते थे। सबको ग्राहक बनाना और सबकी पिटाई करना उनके बायें हाथ का काम था।
वैसे तो पैसे को ले कर किये जाने वाले सारे काम उनके बायें हाथ के ही खेल थे। वे ऐसे सारे काम देर सबेर हथिया ही लेते या ऐसे काम पैदा कर लेते। हमारे स्कूल के सारे बच्चे हर बरस 6 दलों में बांटे जाते। हर दल को हफ्ते का एक दिन दिया जाता और उस दिन स्कूल की सफाई, प्रधानाचार्य के चैम्बर के दोनों तरफ बने बोर्ड पर अख़बार से देख कर मुख्य समाचार लिखना, देर से या बिना वर्दी या बिना स्कूल बैज के आने वाले बच्चों के नाम लिखना वगैरह काम करने होते। ये दल थे नालंदा, उत्तराखंड, वैशाली, सांची, विक्रमशिला और सारनाथ। पहले सब बच्चों के लिए स्कूल का मैटल का बना एक ही बैज हुआ करता था और एक रुपये में खरीदना पड़ता था। था। लेकिन एक अच्छी बात होती थी कि वही बैज बरसों बरस चलता रहता था। बड़े भाई का बैज उसी स्कूल में पढ़ने वाले छोटे भाई के काम आ जाता था। लेकिन नामी मास्टर ने इसमें भी कमाई का रास्ता खोज लिया था। उन्होंने हर दल के लिए दल के नाम वाले अलग अलग रंग के बैज शुरू करा दिये थे जो अगले बरस दल बदलने के साथ ही बेकार हो जाते। यह वह वक्त था जब स्कूल के अधिकतर बच्चों के लिए किसी भी काम के लिए एक रुपया जुटाना या घर से मांग कर लाना भारी पड़ता था।
सिर्फ बैज के मैनेजर ही नहीं, स्कूल में लगने वाली किसी भी प्रदर्शनी के वे नायक होते। स्कूल की वार्षिक पत्रिका के संपादक कोई अध्यापक होते लेकिन उसकी छपाई के लिए प्रेस चुनने के काम में नामी मास्टर भी घुसे होते। स्काउटों की वर्दी बेशक स्काउट विभाग से आती, बच्चों के लिए उसमें कुछ न कुछ जोड़ने की गुंजाइश वे निकाल ही लेते। यानी जहां मलाई की गुंजाइश न भी हो, नामी मास्टर को रखने से निकल ही आती थी।
एक बार सरकार के बचत विभाग की ओर से बच्चों में बचत करने की आदत डालने के लिए स्कूल में एक कैंप लगाया गया। कई तरह के पुरस्कार भी दिये जाने थे। जैसे मैटल का बचत बॉक्स या चाबी का छल्ला वगैरह। सबसे बड़ा ईनाम था कि जो बच्चा महीने में सबसे अधिक बचत करके दिखायेगा, बचत विभाग की ओर से उस बच्चे को उतनी ही रकम ईनाम में दी जायेगी।
इस कैंप की व्यवस्था भी नामी मास्टर ने की थी और तय था कि ये पहला ईनाम भी वे ही हथियाते। उनका लड़का किरण हमारी ही क्लास में पढ़ता था। बाप की दादागिरी में रहता था और न किसी बच्चे की और ही किसी मास्टर की ही परवाह करता था। जब प्रार्थना सभा में सबसे ज्यादा बचत करने वाले बच्चे के रूप में किरण जिसे तोतला होने के कारण सब तिरण के नाम से जानते थे, का नाम पुकारा गया तो किसी को हैरानी नहीं हुई थी। दरअसल नामी मास्टर ने पूरे महीने की अपनी सेलेरी ही तिरण के बचत खाते में जमा करवा दी थी।
किरण की एक बड़ी बहन थी कृष्णा। वह भी तोतली थी। दोनों एक दूसरे को तिरण और तृष्णा कह कर बुलाते थे इसलिए किरण का तिरण नाम स्कूल तक चला आया था।
वैसे तो नामी मास्टर हमारे लिए आतंक, मार और दुकानदारी के डरावने मिश्रण ही थे, लेकिन बरस में हर बरस एक मौका ऐसा जरूर आता था जब हम सब बच्चे चाहते कि क्लास में उनकी निगाह हम पर पड़ जाये और वे हमें भी इशारा कर दें कि तुझे भी आना है। ये एक ऐसा मौका होता जिससे कोई चूकना न चाहता और कई बार ऐसा भी होता कि बच्चे न बुलाये जाने पर भी पहुंच ही जाते और एक बार आ जाने पर किसी न किसी काम में अटका ही लिये जाते।
ये मौका होता दशहरे का रावण बनाने का। पिछले कई बरसों से दशहरे पर परेड ग्राउंड में जलाया जाने वाला रावण वे ही बनाते थे। ये रावण कई हिस्सों में और कई दिनों की कई लोगों की मेहनत से तैयार होता। इस काम से जुड़ना बहुत रोमांचकारी काम होता। बेशक कई कई दिन तक बेगार सी खटनी पड़ती लेकिन ये ऐसी बेगार होती जिसे हर कोई करना चाहता।
रावण और मेघनाथ के पुतले कई हिस्सों में बनाये जाते और हर हिस्से को बनाने से कई काम जुड़े होते। सबसे पहले तो नाप के हिसाब से खपचियां बाँध कर ढांचे खड़े किये जाते। पैर, कमर का घेर, पेट, धड़, गर्दन और फिर मुकुट के साथ चेहरे का हिस्सा। उसके बाद ढेर सारी लेई की मदद से इस ढांचे पर पुराने अखबारों की कई परतें लगायी जातीं। एक परत, दूसरी परत, तीसरी परत और इस तरह कई मन रद्दी की मदद से बांसों और खपचियों के इन ढांचों को रूप आकार मिलना शुरू होता। कई परतें लगतीं। इस काम में बहुत सारे बच्चों की जरूरत पड़ती। पुराने अखबारों और इधर उधर से जुटाई गयी रद्दी पर लेई लगाने वाली एक टीम, लेई लगे कागज रास्ते में बिना खराब हुए ढांचों तक ले जाने वाली दूसरी टीम। वहां इन कागजों को चिपकाने के लिए तीसरी टीम इंतजार कर रही होती। सारी टीमें बहुत तालमेल के साथ काम करतीं। खूब उत्सव का माहौल रहता। शोर शराबा, जल्दी कर जल्दी कर की आवाजें हर तरफ गूंजती। चूंकि स्कूल में दशहरे की दस दिन की छुट्टी रहती, देर रात तक ये काम चलता ही रहता। अखबारों की परतें सूख जाने के बाद ढांचों के विभिन्न हिस्से पेंट किये जाते। पैरों वाले हिस्से आम तौर पर काले रंग में रंगे जाते। घुटनों से नीचे जूतों वाला हिस्सा मानते हुए लाल रंग और पूरी योजना के अनुसार अलग अलग रंग पोते जाते या फिर वहां उसी रंग के कागज चिपकाये जाते। हर स्टेज पर ढांचों का निखार बढ़ता रहता और हम अपने काम का नतीजा देख देख कर खुश होते रहते। रावण और मेघनाथ को जो चोला पहनाया जाता, उसमें हरा, पीला लाल रंग होता। इसी तरह से मुकुट भी रंगीन बनाया जाता। हां, चेहरे पर आंखें, मूंछें और इतर अंग रंगने का काम मास्टर जी खुद करते। वे दायें बायें अंगों के अनुपात और बराबर आकार के बारे में बहुत ही सतर्क रहते थे और इस काम के लिए किसी पर भरोसा नहीं करते थे। ढांचे के सहारे ही लकड़ी की एक सीढ़ी पर चढ़ कर रस्सी की मदद से दायीं बायीं मूंछ, आँख, भौंह वगैरह नापते और उसके बाद ही वहां रंगीन कागज लगाने या रंग करने का काम होता।
कभी कभी मास्टर जी की बेटी तृष्णा यानी कृष्णा सबके लिए घर से चाय और बिस्किट भी भेज देती। वैसे तो हर हिस्से के काम से जुड़ने के अलग रोमांच होते लेकिन सबसे रोमांचक पल वे होते जब रावण और मेघनाथ के पुतलों के अलग अलग हिस्सों में भीतर घुस कर बम पटाके बांधे जाते। लेकिन ये काम दोनों पुतले परेड ग्राउंड में ले जाये जाने के लिए ट्रकों पर लादे जाने से पहले ही किये जाते। ये काम उसी दिनअल सुबह बहुत गोपनीय तरीके से किये जाते। बेशक लदाई के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती और अमूमन काम करने वाले सारे बच्चों को बुलवाया ही जाता लेकिन बम पटाखे लगाने का काम तिरण और उसकी पसंद के लड़के या नामी मास्टर की पसंद के बड़े बच्चे पहले ही कर चुके होते।
कुल मिला कर मैंने भी कम से कम चार बार रावण बनाने में अपना हाथ लगाया होगा लेकिन ये मौका कभी नहीं मिला कि पटाखे देख भी सकें कि कहां और कैसे लगाये जाते हैं। बेशक बरसों बरस रावण और मेघनाथ के जलाये जाने के समय मेले में मौजूद रह कर ये सुख जरूर पाते रहे कि इनके बनाने में कहीं हमारे हाथ भी लगे हैं।
सूरज प्रकाश
एच1/101 रिद्धि गार्डन, फिल्म सिटी रोड, मालाड पूर्व मुंबई 97
mail@surajprakash
09930991424

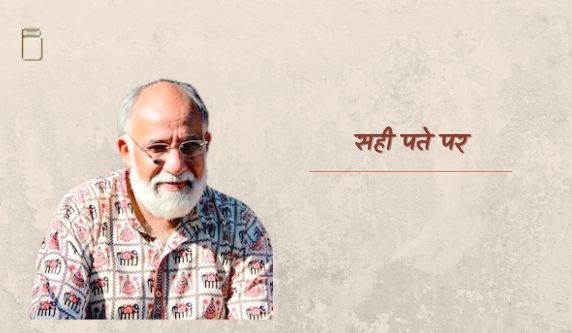



No Comments