जब पहली बार मैंने उन्हें देखा तो वो रहमान भाई के पहले मंज़िले की खिड़की में बैठी लंबी-लंबी गालियाँ और कोसने दे रही थीं। ये खिड़की हमारे सहन में खुलती थी और कानूनन उसे बंद रखा जाता था क्योंकि पर्दे वाली बीबियों का सामना होने का डर था। रहमान भाई रंडियों के जमादार थे, कोई शादी ब्याह, ख़तना, बिस्मिल्लाह की रस्म होती, रहमान भाई औने-पौने उन रंडियों को बुला देते और ग़रीब के घर में भी वहीद जान, मुशतरी बाई और अनवरी कहरवा नाच जातीं।
मगर महल्ले-टोले की लड़कियाँ-बालियाँ उनकी नज़र में अपनी सगी माँ-बहनें थीं। उनके छोटे भाई बुन्दू और गेंदा आए दिन ताक-झाँक के सिलसिले में सर फुटव्वल किया करते थे, वैसे रहमान भाई महल्ले की नज़रों में कोई अच्छी हैसियत नहीं रखते थे। उन्होंने अपनी बीवी की ज़िंदगी ही में अपनी साली से जोड़-तोड़ कर लिया था। उस यतीम साली का सिवाए उस बहन के और कोई मरा-जीता न था। बहन के हाँ पड़ी थी। उसके बच्चे पालती थी। बस दूध पिलाने की कसर थी। बाक़ी सारा गू-मूत वही करती थी।
और फिर किसी नक चढ़ी ने उसे बहन के बच्चे के मुँह में एक दिन छाती देते देख लिया। भांडा फूट गया और पता चला कि बच्चों में आधे बिल्कुल ‘ख़ाला’ की सूरत पे हैं। घर में रहमान की दुल्हन चाहे बहन की दुर्गत बनाती हों पर कभी पंचों में इक़रार न किया। यही कहा करती थीं, “जो कुँवारी को कहेगा, उसके दीदे घुटनों के आगे आएगा।” हाँ बर की तलाश में हर दम सूखा करती थीं, पर उस कीड़े भरे कबाब को बर कहाँ जुड़ता? एक आँख में ये बड़ी कौड़ी सी फली थी। पैर भी एक ज़रा छोटा था। कूल्हा दबा कर चलती थी।
सारे महल्ले से एक अजीब तरह का बायकॉट हो चुका था। लोग रहमान भाई से काम पड़ता तो धौंस जमा कर कह देते, महल्ले में रहने की इजाज़त दे रखी थी। यही क्या कम इनायत थी। रहमान भाई उसी को अपनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई समझते थे।
यही वजह थी कि वो हमेशा रहमान भाई की खिड़की में बैठ कर तूल-तवील गालियाँ दिया करती थी क्योंकि बाक़ी महल्ले के लोग अब्बा से दबते थे। मजिस्ट्रेट से कौन बैर मोल ले।
उस दिन पहली दफ़ा मुझे मालूम हुआ कि हमारी इकलौती सगी फूपी बादशाही ख़ानम हैं और ये लंबी-लंबी गालियाँ हमारे ख़ानदान को दी जा रही थीं।
अम्माँ का चेहरा फ़क़ था और वो अंदर कमरे में सहमी बैठी थीं, जैसे बिच्छू फूपी की आवाज़ उन पर बिजली बन कर टूट पड़ेगी। छट्टे छः माहे इसी तरह बादशाही ख़ानम रहमान भाई की खिड़की में बैठ कर हुंकारतीं, अब्बा मियाँ उनसे ज़रा सी आड़ लेकर मज़े से आराम कुर्सी पर दराज़ अख़बार पढ़ते रहते और मौक़ा महल पर किसी लड़के बाले के ज़रिये कोई ऐसी बात जवाब में कह देते कि फूपी बादशाही फिर शताबियाँ छोड़ने लगतीं। हम लोग सब खेल कूद, पढ़ना-लिखना छोड़कर सहन में गुच्छा बना कर खड़े हो जाते और मुड़-मुड़ अपनी प्यारी फूपी के कोसने सुना करते जिस खिड़की में वो बैठती थीं वो उनके तूल तवील जिस्म से लबालब भरी हुई थी। अब्बा मियाँ से इतनी हम-शक्ल थीं जैसे वही मूँछें उतार कर दुपट्टा ओढ़ कर बैठ गए हों और बावजूद कोसने और गालियाँ सुनने के हम लोग बड़े इत्मिनान से उन्हें तका करते थे।
साढे़ पाँच फुट का क़द, चार उंगल चौड़ी कलाई, शेर सा कल्ला, सफ़ेद बगुला बाल, बड़ा सा दहाना, बड़े बड़े दाँत, भारी सी थोड़ी और आवाज़ तो माशा अल्लाह अब्बा मियाँ से एक सुर नीची ही होगी।
फूपी बादशाही हमेशा सफ़ेद कपड़े पहना करतीं थीं। जिस दिन फूपा मसऊद अली ने मेहतरानी के संग कुलेलें करनी शुरू कीं फूपी ने बट्टे से सारी चूड़ियाँ छना छन तोड़ डालीं। रंगा दुपट्टा उतार दिया और उस दिन से वो उन्हें मरहूम या मरने वाला कहा करती थीं। मेहतरानी को छूने के बाद उन्होंने वो हाथ पैर अपने जिस्म को न लगने दिए।
ये सानेहा जवानी में हुआ था और अब जब से ‘रँडापा’ झेल रही थीं। हमारे फूपा हमारी अम्माँ के चचा भी थे। वैसे तो न जाने क्या घपला था। मेरे अब्बा मेरी अम्माँ के चचा लगते थे और शादी से पहले जब वो छोटी सी थीं तो मेरे अब्बा को देखकर उनका पेशाब निकल जाता था और जब उन्हें ये मालूम हुआ कि उनकी मंगनी इसी भयानक देव से होने वाली है तो उन्होंने अपनी दादी यानी अब्बा की फूपी की पिटारी से अफ़्यून चुरा कर खाली थी। अफ़्यून ज़्यादा नहीं थी और कुछ दिन लोट-पोट कर अच्छी हो गईं। उन दिनों अब्बा अलीगढ़ कॉलेज में पढ़ते थे, उनकी बीमारी की ख़बर सुनकर इम्तिहान छोड़कर भागे। बड़ी मुश्किल से हमारे नाना जो अब्बा के फूपी ज़ाद भाई भी थे और बुज़ुर्ग दोस्त भी, उन्होंने समझा बुझा कर वापस इम्तिहान देने भेजा था। जितनी देर वो रहे, भूके प्यासे टहलते रहे। अध खुली आँखों से मेरी अम्माँ ने उनका चौड़ा चकला साया पर्दे के पीछे बेक़रारी से तड़पते देखा।
“उमराव भाई! अगर उन्हें कुछ हो गया… तो…” देव की आवाज़ लरज़ रही थी। नाना मियाँ ख़ूब हँसे।
“नहीं बिरादर, ख़ातिर जमा रखो। कुछ न होगा।”
उस वक़्त मेरी मुन्नी सी मासूम माँ एक दम औरत बन गई थी। उसके दिल से एक दम देवज़ाद इन्सान का ख़ौफ़ निकल गया था। जभी तो मेरी फूपी बादशाही कहती थी मेरी अम्माँ जादूगरनी है और उसका तो मेरे भाई से शादी से पहले ताल्लुक़ हो कर पेट गिरा था। मेरी अम्माँ अपने जवान बच्चों के सामने जब ये गालियाँ सुनतीं तो ऐसी बिसूर-बिसूर कर रोतीं कि हमें उनकी मार फ़रामोश हो जाती और प्यार आने लगता मगर ये गालियाँ सुनकर अब्बा की गंभीर आँखों में परियाँ नाचने लगतीं। वो बड़े प्यार से नन्हे भाई के ज़रिये कहलवाते, “क्यों फूपी, आज क्या खाया है?”
“तेरी मय्या का कलेजा।” इस बेतुके जवाब से फूपी जल कर मरंदा हो जातीं, अब्बा फिर जवाब दिलवाते, “अरे फूपी, जब ही मुँह में बवासीर हो गई है जुलाब लो जुलाब!”
वो मेरे नौजवान भाई की मिचमिचाती लाश पर कव्वों, चीलों की दावत देने लगतीं। उनकी दुल्हन को जो न जाने बेचारी उस वक़्त कहाँ बैठी अपने ख़्याली दूल्हा के इश्क़ में लरज़ रही होगी, ‘रंडापे’ की दुआएं देतीं और मेरी अम्माँ कानों में उंगलियाँ देकर बुद-बुदातीं, “जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू।”
फिर अब्बा उक्साते और नन्हे भाई पूछते, “फूपी बादशाही, मेहतरानी फूपी का मिज़ाज तो अच्छा है?” और हमें डर लगता कि कहीं फूपी खिड़की में से फाँद न पड़ें।
“अरे जा संपोलिये, मेरे मुँह न लग, नहीं तो जूती से मुँह मसल दूँगी। ये बुड्ढा अंदर बैठा क्या लौंडों को सिखा रहा है। मुग़ल बच्चा है तो सामने आकर बात करे।”
“रहमान भाई, ए रहमान भाई, इस बौरानी कुतिया को संख्या क्यों नहीं खिलाते?”
अब्बा के सिखाने पर नन्हे भाई डरते हुए बोलते। हालाँकि उन्हें डरने की कोई ज़रूरत न थी क्योंकि सब जानते थे कि आवाज़ उनकी है मगर अलफ़ाज़ अब्बां मियाँ के हैं। लिहाज़ा गुनाह नन्हे भाई की जान पर नहीं। मगर फिर भी बिल्कुल अब्बा की शक्ल की फूपी की शान में कुछ कहते हुए उन्हें पसीने आ जाते थे।
कितना ज़मीन-ओ-आसमान का फ़र्क़ था। हमारे दधियाल और नन्हियाल वालों में, नन्हियाल हकीमों वाली गली में थी और दधियाल गाड़ी बानों कटहड़े में। नन्हियाल वाले सलीम चिश्ती के ख़ानदान से थे जिन्हें मुग़ल बादशाह ने मुर्शिद का मर्तबा देकर निजात का रास्ता पहचाना। हिन्दुस्तान में उसे बसे अर्सा गुज़र चुका था। रंगतें सँवला चुकी थीं नुक़ूश नर्म पड़ चुके थे। मिज़ाज ठंडे हो गए थे।
दधियाल वाले बाहर से सबसे आख़िरी खेप में आने वालों में से थे। ज़हनी तौर पर अभी तक घोड़ों पर सवार मंज़िलें मार रहे थे। ख़ून में लावा दहक रहा था। खड़े-खड़े तलवार जैसे नुक़ूश, लाल फ़िरंगियों जैसे मुँह, गोरिल्लों जैसी क़द-ओ-क़ामत, शेरों जैसी गरजदार आवाज़ें। शहतीर जैसे हाथ-पाँव।
और नन्हियाल वाले, नाज़ुक हाथ पैरों वाले शायराना तबीय्यत के, धीमी आवाज़ में बोलने चालने के आदी। ज़्यादातर हकीम, आलिम और मौलवी थे। जभी महल्ले का नाम हकीमों की गली पड़ गया था। कुछ कारोबार में भी हिस्सा लेने लगे थे, शाल बाफ़, ज़रदोज़ और अत्तार वग़ैरा बन चुके थे। हालाँकि मेरी दधियाल वाले ऐसे लोगों को कंजड़े-क़साई ही कहा करते थे क्योंकि वो ख़ुद ज़्यादातर फ़ौज में थे। वैसे मार-धाड़ का शौक़ अभी तक नहीं हुआ था। कुश्ती-पहलवानी, तैराकी में नाम पैदा करना, पंजा लड़ाना, तलवार और पट्टे के हाथों दिखाना और चौसर पचीसी को जो मेरी नन्हियाल के मर्ग़ूब तरीन खेल थे हिजड़ों के खेल समझना।
कहते हैं जब आतिश फ़िशाँ पहाड़ फटता है तो लावा वादी की गोद में उतर आता है। शायद यही वजह थी कि मेरे दधियाल वाले नन्हियाल वालों की तरफ़ ख़ुद ब-ख़ुद खिंच कर आ गए। ये मेल कब और किसने शुरू किया सब शजरे में लिखा है, मगर मुझे ठीक से याद नहीं। मेरे दादा हिन्दुस्तान में पैदा नहीं हुए थे। दादीयाँ भी उसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी मगर एक छोटी सी बहन बिन ब्याही थी। न जाने क्यूँकर वो शेखों में ब्याह दी गई। शायद मेरी अम्माँ के दादा ने मेरे दादा पर कोई जादू कर दिया था कि उन्होंने अपनी बहन बक़ौल फूपी बादशाही कंजड़ों-क़साइयों में दे दी। अपने ‘मरहूम’ शौहर को गालियाँ देते वक़्त वो हमेशा अपने बाप को क़ब्र में चैन न मिलने की बद दुआएँ दिया करतीं। जिन्होंने चुग़्ताई ख़ानदान की मिट्टी पलीद कर दी।
मेरी फूपी के तीन भाई थे। मेरे ताया मेरे अब्बा मियाँ और मेरे चचा। बड़े दो उन से बड़े थे और चचा सबसे छोटे थे। तीन भाईयों की एक लाडली बहन हमेशा की नख़रीली और तुनक मिज़ाज थीं। वो हमेशा तीनों पर रोब जमातीं और लाड करवातीं। बिल्कुल लौंडों की तरह पलीं, शेर सवारी तीर अंदाज़ी और तलवार चलाने की भी ख़ासी मश्क़ थी। वैसे तो फैल फ़ालकर ढेर मालूम होती थीं। मगर पहलवानों की तरह सीना तान कर चलती थीं। सीना था भी चार औरतों जितना।
अब्बा मज़ाक़ में अम्माँ को छेड़ा करते, “बेगम बादशाही से कुश्ती लड़ोगी?”
“उई तौबा मेरी! आलिम-फ़ाज़िल बाप की बेटी” मेरी अम्माँ कान पर कान पर हाथ धर कर कहतीं, मगर वो नन्हे भाई से फ़ौरन फूपी को चैलेंज भिजवाते।
“फूपी हमारी अम्माँ से कुश्ती लड़ोगी?”
“हाँ, हाँ बुला अपनी अम्माँ को। आ जाए ख़म ठोक कर। अरे उल्लू न बना दूँ तो मिर्ज़ा करीम बेग की औलाद नहीं। बाप का नुत्फ़ा है तो बुला। बुला मुल्ला ज़ादी को” और मेरी अम्माँ अपना लखनऊ का बड़े पायंचों का पाजामा समेट कर कोने में दुबक जातीं।
“फूपी बादशाही, दादा मियाँ गँवार थे न? बड़े नाना-जान उन्हें आमद नामा पढ़ाया करते थे। हमारे परनाना के दादा जान ने कभी दादा को कुछ पढ़ा दिया होगा” अब्बा मियाँ छेड़ने को बात तोड़-मोड़ कर कहलवाते।
“अरे वो इस्तंजे का ढीला क्या मेरे बावा को पढ़ाता। मुजाविर कहीं का, हमारे टुकड़ों पर पलता था।” ये सलीम चिशती और अकबर बादशाह के रिश्ते से हिसाब लगाया जाता। हम लोग यानी चुग़्ताई अकबर बादशाह के ख़ानदान से थे। जिन्होंने मेरी नन्हियाल के सलीम चिशती को पीर-ओ-मुर्शिद कहा था। मगर फूपी कहतीं, “ख़ाक, पीर-ओ-मुर्शिद की दुम! मुजाविर थे मुजाविर।”
तीन भाई थे मगर तीनों से लड़ाई हो चुकी थी और वो ग़ुस्सा होतीं तो तीनों की धज्जियाँ बिखेर देतीं। बड़े भाई बड़े अल्लाह वाले थे, उन्हें हिक़ारत से फ़क़ीर और भिकमंगा कहतीं। हमारे अब्बा गर्वनमेंट सर्विस में थे। उन्हें ग़द्दार और अंग्रेज़ों का ग़ुलाम कहतीं, क्योंकि मुग़ल शाही अंग्रेज़ों ने ख़त्म कर डाली, वर्ना आज। ‘मरहूम’ पतली दाल के खाने वाले जोलाहे यानी मेरे फूपा के बजाय वो लाल क़िले में ज़ैब-उन-निसा की तरह अर्क़ गुलाब में ग़ुसल फ़र्मा कर किसी मुल्क के शहनशाह की मल्लिका बनी बैठी होतीं। तीसरे यानी बड़े चचा दस नम्बर के बदमाशों में से थे और सिपाही डरता-डरता मजिस्ट्रेट भाई के घर उनकी हाज़िरी लेने आया करता था। उन्होंने कई क़त्ल किए थे, डाके डाले थे। शराब और रंडी बाज़ी में अपनी मिसाल आप थे। वो उन्हें डाकू कहा करती थीं, जो उनके कैरियर को देखते हुए क़तई फुसफुसा लफ़्ज़ था।
मगर जब वो अपने मरहूम शौहर से ग़ुस्सा होतीं तो कहा करतीं, “मुँह जले। निगोड़ी नाहटी नहीं हूँ। तीन भाईयों की इकलौती बहन हूँ। उनको ख़बर हो गई तो दुनिया का न रहेगा और कुछ नहीं। अगर छोटा सुन ले तो पल भर में अंतड़ियां निकाल के हाथ में थमा दे। डाकू है डाकू… उससे बच गया तो मँझला मजिस्ट्रेट तुझे जेल की सज़ा देगा। सारी उम्र चक्कियाँ पिसवाएगा और उससे बच गया तो बड़ा जो अल्लाह वाला है। तेरी आक़िबत ख़ाक में मिला देगा। देख मुग़ल बच्ची हूँ, तेरी अम्माँ की तरह शेखानी फ़तानी नहीं।” मगर मेरे फूपा अच्छी तरह जानते थे कि तीनों भाई उन पर रहम खाते हैं और वो बैठे मुस्कुराते रहते हैं, वही मीठी-मीठी ज़हरीली मुस्कुराहट जिसके ज़रिये से मेरे नन्हियाल वाले दधियाल वालों को बरसों से जला रहे हैं।
हर ईद-बक़रईद को मेरे अब्बा मियाँ बेटों को लेकर ईदगाह से सीधे फूपी अम्माँ के हाँ कोसने और गालियाँ सुनने जाया करते, वो फ़ौरन पर्दा कर लेतीं और कोठड़ी में से मेरी जादूगरनी माँ और डाकू मामूँ को कोसने लगतीं। नौकर को बुला कर सिवय्याँ भिजवातीं। मगर ये कहतीं, “पड़ोसन ने भेजी हैं।”
“इनमें ज़हर तो नहीं मिला हुआ है?” अब्बा छेड़ने को कहते और फिर सारी नन्हियाल के चीथड़े बिखेरे जाते। सिवय्याँ खा कर ईदी देते जो वो फ़ौरन ज़मीन पर फेंक देतीं कि “अपने सालों को दो वही तुम्हारी रोटियों पर पले हैं” और अब्बा चुपचाप चले आते और वो जानते थे कि फूपी बादशाही वो रुपये घंटों आँखों से लगा कर रोती रहेंगी। भतीजों को वो आड़ में बुला कर ईदी देतीं।
“हरामज़ादो अगर अम्माँ-अब्बा को बतलाया तो बोटियाँ काट कर कुत्तों को खिला दूँगी।” अम्माँ अब्बा को मालूम था कि लड़कों को कितनी ईदी मिली। अगर किसी ईद पर किसी वजह से अब्बा मियाँ न जा पाते तो पैग़ाम पर पैग़ाम आते, “नुसरत ख़ानम बेवा हो गईं, चलो अच्छा हुआ।” मेरा कलेजा ठंडा हुआ बुरे-बुरे पैग़ाम शाम तक आते ही रहते और फिर वो ख़ुद रहमान भाई के कोठे पर से गालियाँ बरसाने आ जातीं।
एक दिन ईद की सिवय्याँ खाते-खाते कुछ गर्मी से जी मालिश करने लगा। अब्बा मियाँ को उल्टी हो गई।
“लो बादशाही ख़ानम, कहा सुना माफ़ करना, हम तो चले।” अब्बा मियाँ ने कराह कर आवाज़ बनाई और फूपी लशतम-पशतम पर्दा फेंक छाती कूटती निकल आईं। अब्बा को शरारत से हँसता देख उल्टे पाँव कोसती लौट गईं।
“तुम आ गईं बादशाही तो मलक-उल-मौत भी घबरा कर भाग गए। वर्ना हम तो आज ख़त्म ही हो जाते।” अब्बा ने कहा। न पूछिए फूपी ने कितने वज़नी कोसने दिए। उन्हें ख़तरे से बाहर देख कर बोलीं, “अल्लाह ने चाहा बिजली गिरेगी। नाली में गिर कर दम तोड़ोगे। कोई मय्यत को कांधा देने वाला न बचेगा”, अब्बा चिढ़ाने को उन्हें दो रुपये भिजवा देते।
“भई हमारी ख़ानदानी डोमनीयाँ गालियाँ दे दें तो उन्हें बेल तो मिलनी ही चाहिए।” और फूपी बौखलाहट में कह जातीं, “बेल दे अपनी अम्माँ बहिनिया को।” और फिर फ़ौरन अपना मुँह पीटने लगतीं, ख़ुद ही कहतीं, “ए बादशाही बंदी, तेरे मुँह को कालिक लगे। अपनी मय्यत आप पीट रही है।” फूपी को अस्ल में भाई से ही बैर था। बस उनके नाम पर आग लग जाती, वैसे कहीं अब्बा के बग़ैर अम्माँ नज़र आ जातीं तो गले लगा कर प्यार करतीं, प्यार से “नछो नछो” कहतीं। “बच्चे तो अच्छे हैं।” वो बिल्कुल भूल जातीं कि ये बच्चे उसी बदज़ात भाई के हैं जिसे वो अज़ल से अबद तक कोसती रहेंगी। अम्माँ उनकी भतीजी भी थीं। भई किस क़दर घपला था मेरी दधियाल नन्हियाल में। एक रिश्ते से मैं अपनी अम्माँ की बहन भी लगती थी। इस तरह मेरे अब्बा मेरे दूल्हा भाई भी होते थे। मेरी दधियाल को नन्हियाल वालों ने क्या-क्या ग़म न दिए। ग़ज़ब तो जब हुआ जब मेरी फूपी की बेटी मसर्रत ख़ानम ज़फ़र मामूँ को दिल दे बैठी।
हुआ ये कि मेरी अम्माँ की दादी यानी अब्बा की फूपी जब लब-ए-दम हुईं तो दोनों तरफ़ के लोग तीमारदारी को पहुँचे। मेरे मामूँ भी अपनी दादी को देखने गए। मसर्रत ख़ानम भी अपनी अम्माँ के साथ उनकी फूपी देखने आईं।
बादशाही फूपी को कुछ डर, ख़ौफ़ तो था नहीं। वो जानती थीं कि मेरे नन्हियाल वालों की तरफ़ से उन्होंने अपनी औलाद के दिल में इत्मिनान बख़्श हद तक नफ़रत भर दी है और पंद्रह बरस की मसर्रत ख़ानम का भी सिन ही क्या था। अम्माँ के कूल्हे से लग कर सोती थीं। दूध पीती ही तो उन्हें लगती थीं।
फिर जब मेरे मामूँ ने अपनी करंजी शर्बत भरी आँखों से मसर्रत जहाँ के लचकदार सरापे को देखा तो वहीं की वहीं जम कर रह गईं।
दिन भर बड़े-बूढ़े तीमारदारी कर के थक कर सो जाते तो ये फ़रमाँबर्दार बच्चे सिरहाने बैठे मरीज़ा पर कम एक दूसरे पर ज़्यादा निगाह रखते, जब मसर्रत जहाँ बर्फ़ में तर कपड़ा बड़ी बी के माथे पर बदलने को हाथ बढ़ातीं तो ज़फ़र मामूँ का हाथ वहाँ पहले से मौजूद होता।
दूसरे दिन बड़ी बी ने पट से आँखें खोल दीं। लरज़ती काँपती गाव तकिए के सहारे उठ बैठीं, उठते ही सारे ख़ानदान के ज़िम्मेदार लोगों को तलब किया। जब सब जमा हो गए तो हुक्म हुआ, “क़ाज़ी को बुलवाओ।”
लोग परेशान कि बुढ़िया क़ाज़ी को क्यों बुला रही है, क्या आख़िरी वक़्त सुहाग रचाएगी, किस को दम मारने की हिम्मत थी।
“दोनों का निकाह पढ़ाओ।” लोग चकराए किन दोनों का, मगर इधर मसर्रत जहाँ पट से बेहोश हो कर गिरीं उधर ज़फ़र मामूँ बौखला कर बाहर चले। चोर पकड़े गए। निकाह हो गया, बादशाही फूपी सन्नाटे में रह गईं।
हालाँकि कोई ख़तरनाक बात न हुई थी, दोनों ने सिर्फ़ हाथ पकड़े थे। मगर बड़ी बी के लिए बस यही हद थी।
और फिर जो बादशाही फूपी को दौरा पड़ा है तो बस घोड़े और तलवार के बग़ैर उन्होंने कुश्तों के पुश्ते लगा दिये। खड़े-खड़े बेटी-दामाद को निकाल दिया। मजबूरन अब्बा मियाँ दूल्हा-दुल्हन को अपने घर ले आए। अम्माँ तो चाँद सी भाबी को देखकर निहाल हो गईं, बड़ी धूम धाम से वलीमा किया।
बादशाही फूपी ने उस दिन से फूपी का मुँह नहीं देखा। भाई से पर्दा कर लिया। मियाँ से पहले ही नाचाक़ी थी। दुनिया से मुँह फेर लिया। और एक ज़हर था कि उनके दिल-ओ-दिमाग़ पर चढ़ता ही गया। ज़िंदगी साँप के फन की तरह डसने लगी।
“बुढ़िया ने पोते के लिए मेरी बच्ची को फँसाने के लिए मकर गाँठा था।”
वो बराबर यही कहे जातीं, क्योंकि वाक़ई वो उसके बाद बीस साल तक और जिईं। कौन जाने ठीक ही कहती हों फूपी।
मरते दम तक बहन भाई में मेल न हुआ। जब अब्बा मियाँ पर फ़ालिज का चौथा हमला हुआ और बिल्कुल ही वक़्त आ गया तो उन्होंने फूपी बादशाही को कहला भेजा, “बादशाही ख़ानम, हमारा आख़िरी वक़्त है। दिल का अरमान पूरा करना हो तो आ जाओ।”
न जाने उस पैग़ाम में क्या तीर छिपे थे। भय्या ने फेंके और बहिनया के दिल में तराज़ू हो गए। हलहलाती, छाती कूटती, सफ़ेद पहाड़ की तरह भूंचाल लाती हुई बादशाही ख़ानम उस ड्योढ़ी पर उतरीं जहाँ अब तक उन्होंने क़दम नहीं रखा था।
“लो बादशाही, तुम्हारी दुआ पूरी हो रही है।” अब्बा मियाँ तकलीफ़ में भी मुस्कुरा रहे थे। उनकी आँखें अब भी जवान थीं।
फूपी बादशाही बावजूद बालों के वही मुन्नी सी बिच्छू लग रही थीं जो बचपन में भाईयों से मचल कर बात मनवा लिया करती थीं। उनकी शेर जैसी खुर्रांट आँखें एक मेमने की मासूम आँखों की तरह सहमी हुई थीं। बड़े-बड़े आँसू उनके संगमरमर की चट्टान जैसे गालों पर बह रहे थे।
“हमें कोसो बिच्छू बी,” अब्बा ने प्यार से कहा। मेरी अम्माँ ने सिसकते हुए बादशाही ख़ानम से कोसने की भीक माँगी।
“या अल्लाह… या अल्लाह…” उन्होंने गरजना चाहा। मगर काँप कर रह गईं। “या… या अल्लाह… मेरी उम्र मेरे भय्या को दे-दे… या मौला… अपने रसूल का सदक़ा।”
वो उस बच्चे की तरह झुँझला कर रो पड़ीं जिसे सबक़ याद न हो।
सबके मुँह फ़क़ हो गए। अम्माँ के पैरों का दम निकल गया। या ख़ुदा आज बिच्छू फूपी के मुँह से भाई के लिए एक कोसना न निकला।
सिर्फ़ अब्बा मियाँ मुस्कुरा रहे थे। जैसे उनके कोसने सुनकर मुस्कुरा दिया करते थे।
सच है, बहन के कोसने भाई को नहीं लगते। वो माँ के दूध में डूबे हुए होते हैं।
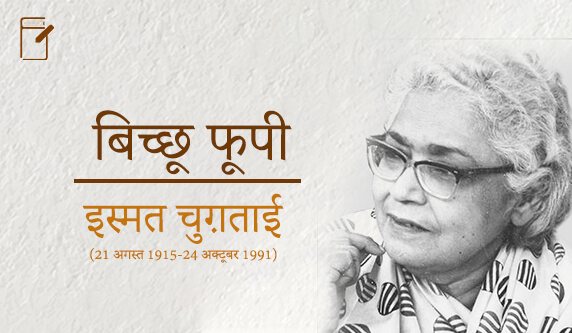

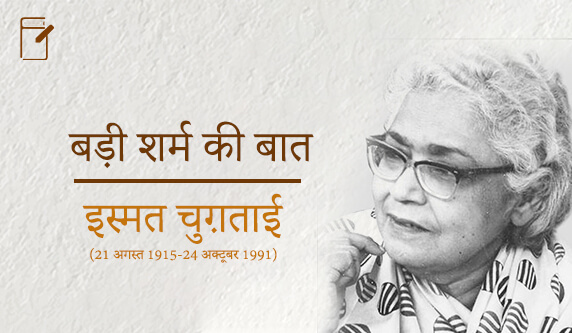
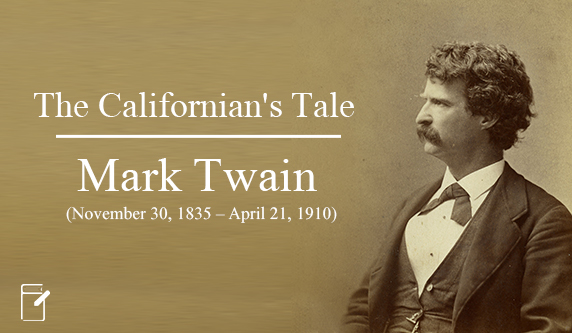

1 Comment
इस्मत चुगताई - Kathanak
August 23, 2021 at 5:54 am[…] बिच्छू फूपी […]