बड़ी मुमानी का कफ़न भी मैला नहीं हुआ था कि सारे ख़ानदान को शुजाअ’त मामूँ की दूसरी शादी की फ़िक्र डसने लगी। उठत बैठते दुल्हन तलाश की जाने लगी। जब कभी खाने पीने से निमट कर बीवियाँ बेटियों की बरी या बेटियों का जहेज़ टाँकने बैठतीं तो मामूँ के लिए दुल्हन तजवीज़ की जाने लगती।
“अरे अपनी कनीज़ फ़ातिमा कैसी रहेंगी।”
“ए है बी, घास तो नहीं खा गई हो, कनीज़ फ़ातिमा की सास ने सुन लिया तो नाक चोटी काट कर हथेली पर रख देंगी। जवान बेटे की मय्यत उठते ही वो बहू के गिर्द कुंडल डाल कर बैठ गई। वो दिन और आज का दिन दहलीज़ से क़दम न उतारने दिया। निगोड़ी का मायके में कोई मरा-जीता होता तो शायद कभी आना जाना हो जाता।”
“और भई, शज्जन भैया को क्या कुँवारी नहीं मिलेगी जो झूटे पत्तल चाटेंगे। लोग बेटियाँ थाल में सजा के देने को तैयार हैं। चालीस के तो लगते भी नहीं,” असग़री ख़ानम बोलीं।
“उई ख़ुदा ख़ैर करे बुआ! पूरे दस साल निगल रही हो! अल्लाह रक्खे ख़ाली के महीने में पूरे पच्चास भर के…. ”
अल्लाह! बेचारी इम्तियाज़ी फुफ्फो बोल के पछताईं। शुजाअ’त मामूँ की पाँच बहनें एक तरफ़ और वो निगोड़ी एक तरफ़। और माशा-अल्लाह पाँचों बहनों की ज़बानें बस कंधों पर पड़ी थीं, ये गज़-गज़ भर की। कोई मुचैटा हो जाता बस पाँचों एक दम मोर्चा बाँध के डट जातीं। फिर मजाल है जो कोई मुग़्लानी, पठानी तक मैदान में टिक जाए। बेचारी शेख़ानियों सैदानियों की तो बात ही न पूछिए। बड़ी-बड़ी दिल गुर्दे वालियों के छक्के छूट जाते।
मगर इम्तियाज़ी फुफ्फो भी इन पाँच पांडवों पर सौ कौरवों से भारी पड़तीं। उनका सबसे ख़तरनाक हर्बा उनकी चिनचिनाती हुई बरमे की नोक जैसी आवाज़ थी। बोलना जो शुरू’ करतीं तो ऐसा लगता जैसे मशीनगन की गोलियाँ एक कान से घुसती हैं और दूसरे कान से ज़न से निकल जाती हैं। जैसे ही उनकी किसी से तकरार शुरू’ होती सारे महल्ले में तुरंत ख़बर दौड़ जाती कि भाई इम्तियाज़ी बुआ की किसी से चल पड़ी, और बीवियाँ कोठे लॉंघतीं, छज्जे फलांगती, दंगल की जानिब हल्ला बोल देतीं।
इम्तियाज़ी फुफ्फो की पाँचों बहनों ने वो टाँग ली कि ग़रीब नक्कू बन गईं, उनकी संझली बेटी गोरी ख़ानम अब तक कुँवारी धरी थीं। छत्तीसवाँ साल छाती पर सवार था मगर कहीं नसीब बनने के आसार नज़र नहीं आ रहे थे। कुँवारे मिलते नहीं, ब्याहे रंडवे नहीं होते। पहले ज़माने में तो हर मर्द तीन चार को ठिकाने लगा देता था। मगर जब से ये हस्पताल और डाक्टर पैदा हुए हैं, बीवियों ने मरने की क़सम खाली है, जिसे देखो आक़िबत के बोरिए समेटने पर तुली हुई है। बड़ी मुमानी की बीमारी के दिनों में ही इम्तियाज़ी फुफ्फो ने हिसाब लगा लिया था। लेकिन उनके फ़रिश्तों को भी पता न था कि दोहाजू के लिए भी कुँए में बाँस डालने पड़ेंगे।
शुजाअ’त मामूँ की उ’म्र का मसअला बड़ी नाज़ुक सूरत इख़्तियार कर गया। क़मर आरा और नूर ख़ाला के लिए तो वो अभी लड़का ही थे। इसलिए वो तो मारे हौल के बरसों की गिनती में बार-बार घपला डाल देतीं। क्योंकि उनकी उ’म्र का हिसाब लग जाने से ख़ुद ख़ालाओं की उ’म्र पर शह पड़ती थी, लिहाज़ा पाँचों बहनें बिल्कुल मुख़्तलिफ़ सिम्त से हमला-आवर हुईं। उन्होंने फ़ौरन इम्तियाज़ी फुफ्फो के नवास दामाद का ज़िक्र छेड़ दिया। जिसका तज़किरा फुफ्फो की दुखती रग था, क्योंकि वो उनकी नवासी पर सौत ले आया था।
मगर हमारी फुफ्फो भी खरी मुग़्लानी थीं, जिनके वालिद शाही फ़ौज में बर्क़-अंदाज़ थे। वो कहाँ मार खाने वालियों में से थे। झट पैंतरा बदल कर वार ख़ाली कर दिया और शहज़ादी बेगम की पोती पर टूट पड़ीं जो खुले बंदों ख़ानदान की नाक कटवा रही थी, क्योंकि वो रोज़ डोली में बैठ कर धनकोट के स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। उस ज़माने में स्कूल जाना उतना ही भयानक समझा जाता था जितना आजकल कोई फिल्मों में नाचने गाने लगे।
शुजाअ’त मामूँ बड़े माक़ूल आदमी थे। निहायत सुथरा नक़्शा, छरेरा बदन, दर्मियाना क़द, इम्तियाज़ी फुफ्फो सारे में कहती फिरतीं थीं कि ख़िज़ाब लगाते हैं, मगर आज तक किसी ने कोई सफ़ेद बाल उनके सर में नहीं देखा, इसलिए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि ख़िज़ाब लगाना कब शुरू’ किया… यूँ देखने में बिल्कुल जवान लगते थे, वाक़ई चालीस के नहीं जचते थे। जब उन पर पैग़ामों की बहुत ज़ोर की बारिश हुई तो बौखलाकर उन्होंने मुआमला बहनों के सपुर्द कर दिया, इतना कह दिया, लौंडिया इतनी छिछोरी न हो कि बेटी लगे, और ऐसी खूसट भी न हो कि उनकी अम्माँ लगे।
“उई, क्या ख़ौफ़ियाता हुआ नाम!” इम्तियाज़ी फुफ्फो को कुछ न सूझा तो नाम ही में कीड़े निकालने लगीं, मगर बहनों ने ऐसा मोर्चा कसा कि उनकी किसी ने न सुनी।
“लौंडिया सोला से एक दिन ज़्यादा की हो तो सौ जूते सुब्ह, सौ जूते शाम, ऊपर से हुक़्क़ा का पानी।” मगर उनकी किसी ने न सुनी। वो अपनी गोरी बेगम की नाव पार लगाने के लिए ख़्वाही न ख़्वाही दुंद मचाती थीं।
रुख़साना बेगम थीं कि बस कोई देखे तो देखता ही रह जाए। जैसे पहली का नाज़ुक शरमाया हुआ चाँद किसी ने उतार लिया हो। शक्ल देखते जाओ पर जी न भरे। तोलो तो पाँचवी के बा’द छटा फूल न चढ़े। रंगत ऐसी जैसे दमकता कुंदन… जिस्म में हड्डी का नाम नहीं जैसे सख़्त मैदे की लोई पर गाय का मक्खन चुपड़ दिया हो। निस्वानियत इस ग़ज़ब की जैसे दर्जन भर औरतों का सत निचोड़ कर भर दिया हो। गर्म-गर्म लपटें सी निकलती थीं, शायद ब-क़ौल फुफ्फो सोला बरस की होंगी, मगर उन्नीस-बीस की उठान थी, बहनों ने मामूँ को पच्चीसवाँ साल बताया था। उन्हें ज़रा सा तकल्लुफ़ तो हुआ मगर फिर टाल गए, कमसिनी तो कोई बड़ा जुर्म नहीं।
सबसे बड़ी बात तो ये थी कि बे-इंतिहा मुफ़लिस घर का बोझ थीं। दोनों तरफ़ का ख़र्चा मामूँ के सर रहा। जब रुख़साना मुमानी ब्याह कर आईं तो उन्हें ग़ौर से देख के मामूँ के पसीने छूट गए।
“बाजी, ये तो बिल्कुल बच्ची है!” उन्होंने बौख़ला कर कहा।
“उई, ख़ुदा ख़ैर करे, ए मियाँ तेल देखो, तेल की धार देखो।”
“मर्द साठा और पाठा, बीवी बीसी और खीसी। दो-चार बच्चे हुए नहीं कि सारी क़लई उतर जाएगी। गो-मूत में न सोला सिंघार रहेंगे, न ये रंग-ओ-रोग़न न ये छल्ला सी कमर रहेगी, न बाज़ुओं का लोच। बराबर की न लगने लगे तो चोर का हाल, सो मेरा। मैं तो कहूँ दस साल में बड़ी भाभी जान की तरह हो जाएगी।”
“फिर हम अपने बैरन के लिए साढे़ बारह बरस की लाएँगे ख़ाला चहकीं।”
“हुश्त!” मामूँ शरमा गए।
“दूसरी बीवी नहीं जीती, इसलिए तीसरी”, शम्सा बेगम बोलीं।
“क्या बक रही हो?”
“हाँ मियाँ बड़े बूढ़ों से सुनते आए हैं। दूसरी तो तीसरी का सदक़ा होती है, उसी लिए पुराने ज़माने में लोग दूसरी शादी गुड़िया से कर दिया करते थे। ताकि फिर जो दुल्हन आए वो तीसरी हो।”
बहनों ने समझाया और मामूँ समझ गए। फिर जल्द ही रुख़साना बेगम ने भी समझा दिया। दो तीन साल में अच्छे खाने, कपड़े और आ’शिक़-ए-ज़ार मियाँ ने वो जादू फेरा कि पहली का चाँद चौधवीं का माहताब हो गया, वो चाँदनी छिटकी कि देखने वालों की आँखें झपक गईं। पोर पोर से शुआएँ फूट निकलीं… शुजाअ’त मामूँ पर ऐसा नशा सवार हुआ कि बिल्कुल धुत हो गए। शुक्र है जल्द ही पेंशन होने वाली थी, वर्ना आए दिन के दफ़्तर से ग़ोते ज़रूर रंग लाते।
बहनों के ले दे के एक भैया थे। बड़ी मुमानी तो दूल्हनापे ही में जी से उतर गई थीं। उनकी कमान कभी चढ़ी ही नहीं। जब तक ज़िंदा रहीं सूरत को तरसती रहीं। आल-ओ-औलाद ख़ुदा ने दी ही नहीं कि उधर जी बहल जाता। मियाँ बहनों के चहेते भाई। सूरत न देखें तो खाना न पचे। दफ़्तर से सीधे किसी बहन के यहाँ पहुँचते, रात का खाना वहीं से खाकर आते। फिर भी डेस्क ख़्वान सजाए रात तक बैठी राह तका करतीं, किसी दिन इत्तिफ़ाक़ से खा लेते तो उनकी ज़िंदगी का मक़सद पूरा हो जाता।
आए दिन बहनों के हाँ हंगामे रहते। झूटों को कभी भावज को भी बुला लेतीं मगर ये बेचारी वहाँ ग़रीब-उल-वतन सी लगती। सबने बुलाना छोड़ दिया। शुजाअ’त मामूँ को कभी यार दोस्तों की दावत करनी होती या क़व्वाली और मुजरे की महफ़िलें जमतीं तो बीवी को पता भी ना चलता, बहनें सब इंतेज़ाम कर देतीं, ये उन ही के हाथ में रुपया दे देते।
किसी ने मुमानी को राय दी कि मियाँ को क़ाबू करने का बस एक गुर है। उसे ऐसे खाने खिलाओ कि किसी के घर का निवाला मुँह को न लगे। बस जी, मुमानी ने खाना पकाने की किताबें मँगाईं, लहसुन की ख़ीर और बादाम के गुलगुले, दम का मुर्ग़ और मछली के कबाब पकाए जिन्हें खाकर मामूँ ने फ़ैसला किया कि वो उन्हें ज़हर देकर मारना चाहती हैं।
मुमानी ख़ून थूक-थूक कर मर गईं।
मगर नई-नवेली का जादू तो आते ही सर चढ़ कर बोलने लगा। न कहीं आने के रहे न जाने के, न किसी का आना भाये। बस मियाँ हैं और बीवी। क्या बाग़-ओ-बहार सा भाई चुटकी बजाते में खुर्रे की तरह बे-रहम और बे-मुरव्वत हो गया। दुनिया उजाड़ हो गई। अपने पाँव आप कुल्हाड़ी मारी। गोरी बेगम से शादी करा दी होती तो यूँ भैया साहब अलक़त न हो जाते।
“ए भाभी, भैया को आँचल में कब तक बाँधे रखोगी?” मर्द ज़ात है कोई झंडूलना नहीं कि हर दम कूल्हे से लगाए बैठी हैं।”
लाख ता’ने दिए जाते, दुल्हन बेगम हैं कि खी-खी हँस रही हैं और मियाँ काठ के उल्लू घिघियाए जाते हैं। अपनी जोरू है कोई पड़ोसी की नहीं कि बस तके जा रहे हैं बजर-बट्टू की तरह।
मामूँ वो मामूँ ही न रहे। अजी कैसी क़व्वालियाँ और कैसे मुजरे बस बीवी तिगुनी का नाच नचा रही है, आप नाच रहे हैं।
“ए बस, और थोड़े दिन के चोंचले हैं, पैर भारी हुआ नहीं कि सारा दुल्हनापा ख़त्म। एक न एक दिन तो भाई का जी भरेगा।” दिलों को तसल्ली दी गई।
अल्लाह-अल्लाह करके रुख़साना मुमानी का पैर भारी हुआ तो अल्लाह तौबा न उल्टियाँ न तबीअ’त माँदी। चेहरे पे और चार चाँद खिल उठे, क्या मजाल जो ज़रा सा अलकस आ जाए। वही शोख़ियाँ, वही अंदाज़-ए-माशूक़ाना जो नई दुल्हनों के हुआ करते हैं। और मामूँ का तो बस नहीं चलता उन्हें उठाकर पलकों में छिपा लें। दिल निकाल के क़दमों में डाले देते हैं। जी से उतरने के बजाए वो तो दिमाग़ पर भी छा गईं।
पूरे दिनों में भी रुख़साना मुमानी के हुस्न को गहन न लगा। जिस्म फैल गया मगर चाँद दमकता रहा। न पैरों पर सूजन, न आँखों के गिर्द हल्क़े, न चलने फिरने में कोई तकलीफ़।
जापे के बा’द चट से खड़ी हो गईं। क्या मजाल जो कमर बराबर भी मोटी हुई हों, वही कुँवारियों जैसा लचकदार जिस्म, भली बीवी के जापे में बाल झड़ जाते हैं, उनके वो अदबदा के बढ़े कि ख़ुद सर धोना दुशवार हो गया।
हाँ बीवी के बदले ज़रा मामूँ झटक गए, जैसे बच्चा उन्होंने ही पैदा किया हो। थोड़ी सी तोंद ढलक आई। गालों में लंबी-लंबी क़ाशें गहरी हो गईं। बाल पहले से ज़्यादा सफ़ेद हो गए। अगर दाढ़ी न बनी होती तो गालों पर च्यूँटी के सफ़ेद-सफ़ेद अंडे फूट आते।
जब दो साल बा’द बेटी हुई तो मामूँ की तोंद और आगे खिसक आई। आँखों के नीचे खाल लटकने लगी। निचली डाढ़ का दर्द क़ाबू से बाहर हो गया तो मजबूरन निकलवाना पड़ी। एक ईंट खिसकी तो सारी इमारत की चूलें ढीली हो गईं। उन दिनों मुमानी की अक़्क़ल दाढ़ निकल रही थी। शुजाअ’त मामूँ की बत्तीसी असली दाँतों से ज़्यादा हसीन थी। उ’म्र का इल्ज़ाम नज़ले के सर गया।
इम्तियाज़ी फुफ्फो के हिसाब से रुख़साना मुमानी छब्बीस बरस की थीं। गो अब वो कभी बच्चों के साथ धमा-चौकड़ी मचाने के मूड में आ जातीं तो सोलह बरस की लगने लगतीं। कई साल से उ’म्र का बढ़ना रुक गया था। ऐसा मा’लूम होता था उनकी उ’म्र अड़ियल टट्टू की तरह एक जगह जम गई है और आगे खिसकने का नाम ही नहीं लेती। ननदों के दिल पर आरे चलते। वैसे भी जब अपने हाथ-पैर थकने लगें तो नौजवानों की शोख़ियाँ मुँह-ज़ोर घोड़े की दुलत्ती की तरह कलेजे में लगती हैं। और मुमानी तो साफ़ अमानत में ख़यानत कर रही थीं। शराफ़त और भल-मलनसाहट का तो ये तक़ाज़ा था कि वो शौहर को अपना ख़ुदा-ए-मजाज़ी समझतीं। अच्छे बुरे में उनका साथ देतीं। ये नहीं कि वो थके-माँदे बैठे हैं और बेगम बे-तहाशा मुर्ग़ियों के पीछे दौड़ रही हैं।
“अरे भाभी, तुम पर ख़ुदा की सुवर, न सर की ख़बर है न पैर की, हुड़दंगी बनी मुर्ग़ियाँ खदेड़ रही हो!”
“ए, तो क्या करूँ ख़ाला, मुई बिल्ली…”
“उई, लो और सुनो। ए बी मैं तुम्हारी ख़ाला कब से हो गई? शज्जन भाई मुझसे चार साल बड़े हैं माशाअल्लाह… बड़ा भाई बाप बराबर… तुम भी मेरी बड़ी हो, ख़बरदार जो तुमने फिर मुझे ख़ाला कहा।”
“जी बहुत अच्छा।” शादी से पहले रुख़साना मुमानी की अम्माँ उनकी दुपट्टा बदल बहन कहलाती थीं।
वही हुस्न और कमसिनी जिसने एक दिन शुजाअ’त मामूँ को ग़ुलाम बना लिया था, अब उनकी आँखों में खटकने लगी। लंगड़ा बच्चा जब दूसरे बच्चों के साथ नहीं दौड़ पाता तो चढ़ कर मचल जाता है कि तुम बे-ईमानी कर रहे हो। मुमानी उनके साथ दग़ा कर रही थीं। कभी कभी तो उन्हें लड़कियों बालियों की तरह हँसता या दौड़ते भागते देखकर उनके दिल में टीसें उठने लगतीं, वो जल कर कोयला हो जातीं।
“लौंडों को लुभाने के लिए क्या तन-तन के चलती हो”, वो ज़हर उगलने लगे। “हाँ अब कोई जवान पट्ठा ढूँढ लो।”
मुमानी पहले तो हँसकर टाल देतीं, फिर झेंप कर गुलनार हो जातीं। इस पर मामूँ और भी चराग़-पा होते और भारी भारी इल्ज़ाम लगाते।
“फ़लाँ से आँखें लड़ा रही थीं, ढिमाके से तुम्हारा तअ’ल्लुक़ है?”
तब मुमानी सन्नाटे में रह जातीं। मोटे-मोटे आँसू छलक उठते, अलगनी से दुपट्टा घसीट कर वो अपना जिस्म ढक कर, सर झुकाए कमरे में चली जातीं। मामूँ का कलेजा कट जाता, उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती। वो उनके तलवे चूमते, उनके क़दमों में सर फोड़ते, उनके आगे नाक रगड़ते, रोने लगते। “मैं कमीना हूँ, हराम-ज़ादा हूँ, जूती लेकर जितने चाहो मरो। मेरी जान, मेरी रुख़ी, मेरी मल्लिका, शहज़ादी।”
और रुख़साना मुमानी अपनी रुपहली बाँहें उनके गले में डाल कर भों-भों रोतीं।
“तुम्हारा आ’शिक़-ए-ज़ार हूँ मेरी जान। रश्क-ओ-हसद से जल-जल कर ख़ाक हुआ जाता हूँ। तुम तो नन्हे को गोद में लेती हो तो मेरा ख़ून खौलने लगता है, जी चाहता है साले का गला घूँट दूँ, मुझे मुआ’फ़ कर दो मेरी जान।” वो झट मुआ’फ़ कर देतीं। इतना मुआ’फ़ करतीं कि शुजाअ’त मामूँ की आँखों के हल्क़े और ऊदे हो जाते, और वो बड़ी देर तक थके हुए ख़च्चर की तरह हाँपा करते।
फिर ऐसे भी दिन आ गए कि वो माफ़ी भी न माँग सकते। कई-कई दिन वो रूठे पड़े रहते। बहनों की उम्मीदें बंध जातीं।
“भैया जान, भाभी को कुढ़ा-कुढ़ा कर मार रहे हैं। अब कोई दिन जाता है कि ये आए दिन की दाँता किल-किल रंग लाएगी।”
मुमानी छुप-छुप कर घंटों रोतीं। आँसू भरी आँखों में लाल-लाल डोरे और भी सितम ढाने लगते। सुता हुआ ज़र्द चेहरा जैसे सोने की गिन्नी में किसी बे-ईमान सुनार ने चाँदी की मिलावट बढ़ा दी हो। फीके फीके होंट, माथे पर उलझी सी एक वारफ़्ता लट। देखने वाले कलेजा थाम कर रह जाते। हुस्न-ए-सोगवार को देखकर मामूँ के कंधे और झुक जाते, आँखों की वीरानी बढ़ जाती।
एक बेल होती है… अमर-बेल। हरे हरे सँपोलिये जैसे डंठल… जड़ नहीं होती… ये हरे डंठल किसी भी सर-सब्ज़ पेड़ पर डाल दिए जाएँ तो बेल उसका रस चूस कर फलती-फूलती है। जितनी ये बेल फैलती है, उतना ही वो पेड़ सूखता जाता है।
जूँ-जूँ रुख़साना बेगम के चमन खिलते जाते थे मामूँ सूखते जाते थे। बहनें सर जोड़ कर खुसर फुसर करतीं। भाई की दिन-ब-दिन गिरती हुई सेहत को देखकर उनका कलेजा मुँह को आता था। बिल्कुल झिरकुट हो गए थे। गठिया की शिकायत तो थी ही, नज़ला अलग अज़ाब-ए-जान हो गया। डाक्टरों ने कहा ख़िज़ाब क़तई मुवाफ़िक़ नहीं। मजबूरन मेहंदी लगाने लगे।
बेचारी रुख़साना एक-एक से बाल सफ़ेद करने के नुस्खे़ पूछती फिरती थीं। किसी ने कहा अगर ख़ुश्बूदार तेल डालो तो बाल जल्दी सफ़ेद हो जाएँगे। दुखिया ने इत्र सर में झोंक लिया। मामूँ की नाक में जो शमामत-उल-अंबर की मदहोश-कुन ख़ुश्बू की लपटें पहुँचीं तो वो ग़लीज़ ऐ’ब उन्होंने मुमानी पर लगाए कि अगर बच्चों का ख़याल न होता तो मुमानी कुँए में कूद जातीं, उनके बाल सफ़ेद होने की बजाए और मुलाइम और चमकदार हो कर डसने लगे।
मुमानी की जवानी के तोड़ के लिए मामूँ ने तिब्ब-ए-यूनानी की तमाम माजूनें, मुक़व्वियात, कुश्ते और तेल इस्ति’माल कर डाले। थोड़े दिन के लिए उनकी भागती हुई जवानी थम गई। बाँकपन लौट आया। मुमानी ने कुछ दुनिया-दारी के दाँव-पेंच तो सीखे न थे, ख़ुद-रौ पौदा थीं… कभी किसी ने बारीकियाँ न समझाईं। अट्ठाईस साल की थीं मगर अठारह बरस जैसी ना-तजुर्बा-कार और अल्हड़पन था।
मोटर बहुत चलाओ तो इंजन जल जाता है, दवाओं का रद्द-ए- अ’मल जो शुरू’ हुआ तो शुजाअ’त मामूँ ढह गए। एक दम बुढ़ापा टूट पड़ा। अगर वो जिस्म और दिमाग़ को इतना न तकतकाते तो बासठ बरस में यूँ लुटिया न डूब जाती। अब वो अपनी उ’म्र से ज़्यादा लगने लगे।
बहनें ज़ार-ओ-क़तार रोईं, हकीम डाक्टर जवाब दे चुके थे। लोगों ने जवान बनने के तो लाखों नुस्खे़ ईजाद किए क़ब्ल-अज़-वक़्त बूढ़ा होने की कोई दवा नहीं, जो मुमानी को खिला दी जाती। ज़रूर उन पर कोई सदाबहार क़िस्म का जिन्न या पीर मर्द आ’शिक़ था कि किसी तौर से उनकी जवानी ढलने का नाम ही न लेती थी। तावीज़ गंडे हार गए, टोने टोटके चित्त हो गए।
अमर-बेल फैलती रही।
बरगद का पेड़ सूखता रहा।
तस्वीर हो तो कोई फाड़ दे, मुजस्समा हो तो पटख़ कर चकना-चूर कर दे। अल्लाह के हाथों का बनाया मिट्टी आग का पुतला, अगर हसीन भी हो और ज़िंदा भी, उसकी हर साँस में जवानी की गर्मी महक रही हो तो फिर कुछ बस नहीं चलता। उसके चढ़े हुए सूरज को उतारने की एक ही तरकीब हो सकती है कि खाने की मार दी जाए। घी, गोश्त, अंडे, दूध क़त’ई बंद।
जब से शुजाअ’त मामूँ का हाज़मा जवाब दे गया था, मुमानी सिर्फ़ बच्चों के लिए गोश्त वग़ैरह मँगाती थीं। कभी-कभार एक निवाला ख़ुद चख लेती थीं, अब उससे भी परहेज़ कर लिया। सबको उम्मीद बंध गई कि अब इंशाअल्लाह ज़रूर बुढ़ापा तशरीफ़ ले आएगा।
“ए भाभी, ये क्या उछाल छक्का लौंडियों की तरह मुई शलवार क़मीज़ पहनती हो, और भी नन्ही बन जाती हो,” ननद कहतीं… “भारी भरकम कपड़े पहनो कि अपनी उ’म्र की लगो।”
मुमानी ने टिका हुआ दुपट्टा और ग़रारा पहन लिया।
“किसी यार की बग़ल में जाने की तैयारी है”, मामूँ ने कचोके दिए, मुमानी कपड़ों से भी ख़ौफ़ खाने लगीं।
“ए भाभी ये क्या एक-आध वक़्त की नमाज़ पढ़ती हो, पंज-वक़्ता की आ’दत डालो।”
मुमानी पंज-वक़्ता नमाज़ पढ़ने लगीं। जब से मामूँ की नींद बूढ़ी और नख़रीली हुई थी, तहज्जुद के वक़्त से जागना पड़ता था।
“मेरे मरने के नफ़्ल पढ़ रही हो”, मामूँ बिसूरते।
दुबली तो थीं, दिन रात की दाँता किल-किल से और भी धान पान हो गईं। घी गोश्त से परहेज़ हुआ तो रंग और भी निखर आया, जिल्द ऐसी शफ़्फ़ाफ़ हो गई कि जैसे कोई दम में बिल्लौर की तरह आर-पार नज़र आने लगेगा। चेहरे पर अजब नूर सा उतर आया।
पहले देखने वालों की राल टपकती थी, अब उनके क़दमों पर सर पटख़ने की तमन्ना जागने लगी। जब सुब्ह-सवेरे नमाज़-ए-फ़ज्र के बा’द क़ुरआन की तिलावत करतीं तो उनके चेहरे पर हज़रत मर्यम का तक़द्दुस और फ़ातिमा ज़ुहरा की पाकीज़गी तारी हो जाती। वो और भी कमसिन और कुँवारी लगने लगतीं।
मामूँ की क़ब्र और पास खिसक आती, और वो उन्हें मुँह भर-भर के कोसते और गालियाँ देते कि भाँजों-भतीजों के बा’द वो जिनों और फ़रिश्तों को वर्ग़ला रही हैं, चिल्ले खींच-खींच कर जिन क़ाबू में कर लिए हैं, उनसे जादू की बूटियाँ मँगाकर खाती हैं।
ख़िज़ाब के बा’द अब मेहंदी भी मामूँ को आँखें दिखाने लगी थी। मेहंदी लगाते तो छींकें आकर नज़ला हो जाता। वैसे भी उन्हें मेहंदी से घिन आने लगी थी। रुख़साना मुमानी उनके बालों में मेहंदी लगातीं तो बा-वजूद एहतियात के उनके हाथों में भी शम’एँ लौ देने लगतीं।
उनके हाथ देखकर शुजाअ’त मामूँ को ऐसा मा’लूम होता जैसे मेहंदी में नहीं मुमानी ने उनके ख़ून-ए-दिल में हाथ डुबो लिए हैं। वही हाथ जिन्हें वो कभी चम्बेली की मुँह-बंद कलियाँ कह कर चूमा करते थे, आँखों से लगाते थे, अब शिकरे के ख़ूँ-ख़्वार पंजों की तरह उनकी आँखों में घुसे जाते थे।
जितना-जितना वो उनकी मुंडिया ज़मीन पर घिसते, मुमानी संदल की तरह महकतीं।
बहनें घर से तर माल तैयार करके भाई को खिलाने लातीं कि कहीं भावज ज़हर न खिला रही हो। अपने हाथ से सामने ख़िलातीं। मगर इन खानों से मामूँ का हाल और पतला हो जाता। बवासीर की पुरानी शिकायत ने वो ज़ोर पकड़ा कि रहा सहा ख़ून भी निचोड़ लिया।
अभी तक उस ना-मुराद कुश्ते का असर बाक़ी था, जो उन्होंने पिछले जाड़ों में मुरादाबाद के एक नामी गिरामी हकीम साहब का नुस्ख़ा लेकर कई सौ की लागत से तैयार कराया था। नुस्ख़ा बेहद शाही क़िस्म का था जिसे मुर्दा खा लेता तो तनतना कर खड़ा हो जाता। मगर मामूँ गोंदनी की तरह फोड़ों से लद गए।
दुखिया मुमानी घी को सैंकड़ों बार पानी से धोतीं। उसमें गंधक और बहुत सी दवाएँ कूट छानकर मिलातीं। धड़ियों मरहम थोपा जाता, पतीलियों में नीम के पत्तों का पानी औटातीं और सुब्ह शाम पीप, ख़ून धोतीं, उनमें से चंद फोड़े मुस्तक़िल नासूर बन गए थे और मामूँ को निगल रहे थे।
फिर एक दिन तो अंधेर ही हो गई। मामूँ बहुत कमज़ोर हो गए थे। बहनें बैठी भावज का दुखड़ा रो रही थीं कि नज्जी बुढ़िया ख़ुदा जाने कहाँ से आन मरी। पहले तो वो शुजाअ’त मामूँ को नाना-जान समझ कर उनसे फ़्लर्ट करने लगी। किसी ज़माने में नाना-जान उस पर बहुत मेहरबान रह चुके थे।
बुढ़िया ना-मुराद की मत मारी गई थी। नाना-जान को मरे बीस बरस हो चुके थे। और वो अपनी चीपड़ भरी आँखों में पुराने ख़्वाब जगाने पर मुसिर थी, बड़ी ले दे के बा’द वो मामूँ का असली मुक़ाम समझी तो मरहूमा मुमानी का मातम ले बैठी।
“है है। क्या बुढ़ापे में दग़ा दे गईं।” अचानक उसकी नज़र मुमानी पर जा पड़ी। मुमानी सहन में कबूतरों को दाना डाल रही थीं। अजब प्यारे अंदाज़ में वो गर्दन नौढ़ाए बैठी थीं, जैसे तस्वीर खिंचवा रही हों। कबूतर उनकी बिल्लौरी दमकती हुई हथेली को गुदगुदा रहे थे। और वो बे-इख़्तियार हँस रही थीं।
“हाय मैं मर गई!” बुढ़िया ने अपना चपाती जैसा सीना कूट कर रुख़साना मुमानी की तरफ़ हवा में बलाएँ लेकर कनपटियों पर दसों उँगलियाँ चड़-चड़ चटख़ाईं, “अल्लाह पाक नज़र-ए-बद से बचाए। बिटिया तो चाँद का टुकड़ा है। मैं जानूँ मीठा बरस लगा है। ए मियाँ”, वो राज़दारी के अंदाज़ में मामूँ के क़रीब खिसकी, “सौदागरों का मँझला बेटा विलायत पास करके आया है। अल्लाह क़सम बस चाँद और सूरज की जोड़ी रहेगी।”
किसी ज़माने में बुढ़िया बड़ी मारके की मश्शाता थी, अब उसका बाज़ार बंद हो चुका था। चोंडा सफ़ेद हुआ, हाथ पैर से माज़ूर हुई तो टुकड़े माँग कर गुज़र-औक़ात करने लगी थी।
थोड़ी देर तक तो किसी की समझ ही में न आया कि बुढ़िया मुर्दार क्या बक रही है। सौदागरों का मँझला बेटा जो विलायत पास था, सबकी निगाहों में था। किसी को शुबह भी न हुआ कि नाशुदनी क़ुत्तामा रुख़साना मुमानी का रिश्ता लगाने की ताक़ में है।
“इमाम हुसैन की क़सम, मियाँ मैं तो कंगनों की जोड़ी लूँगी। बात छेड़ूँ?”
बात जो वाज़ेह हुई और पानी मरा तो भिड़ों का छत्ता छिड़ गया। चारों तरफ़ से तोपें दगने लगीं।
“है है, मुझ जनम पीटी को क्या ख़बर?” बुढ़िया स्लीपर पहनती रपटी, बाहर की तरफ़ चलते चलते उसने मामूँ की पिटी हुई सूरत पर एक मुश्तबा नज़र डाली, “मुँह पर तो साफ़ कुँवारपना बरस रहा है।”
उस दिन शुजाअ’त मामूँ ने क़ुरआन उठाकर सब के सामने कह दिया कि ये दोनों बच्चे उनके नहीं, अड़ोस-पड़ोस की मेहरबानियों का फल हैं जिनसे रुख़साना बेगम ताक-झाँक किया करती हैं।
उस रात वो रोते रहे, कराहते रहे, अंगारों पर लोटते रहे। उस रात उन्हें बड़ी मुमानी बहुत याद आईं, उनके बाल क़ब्ल-अज़-वक़्त पक गए थे, उनकी जवानी, उनका दुल्हनापा आँसुओं में बह गया। नेकी और पारसाई का मुजस्समा, वफ़ा की पुतली… उनके हिस्से का बुढ़ापा भी उन्होंने अपने वजूद में समेट लिया, और शरीफ़ बीवियों की तरह जन्नत को सिधारीं।
आज वो होतीं तो ये दर्द, ये सोज़िश, ये सफ़ेद जड़ों वाले मेहंदी लगे बाल, ये रिस्ते नासूर, ये तन्हाई बट जाती। फिर बुढ़ापा यूँ न दहलाता। दोनों साथ बूढ़े होते, एक दूसरे के दुःख को समझते, सहारा देते।
अमर-बेल दिन दूनी रात चौगुनी फैलती गई। बड़के पेड़ का तना खोखला हो गया, टहनियाँ झूल गईं, पत्ते झड़ गए… बेल पास के दूसरे हरे-भरे पेड़ पर रेंग गई।
कैसा जाँ-सोज़ समाँ था। शुजाअ’त मामूँ की मय्यत सेहन में बनी सँवरी रखी हुई थी, बहनें खड़ी खड़ी पछाड़ें खा रही थीं। मामूँ ने अपनी सारी जायदाद बहनों के नाम हेबा कर दी थी।
रुख़साना मुमानी सबसे अलग थलग दर से लगी बैठी थीं। कहने वाले कहते हैं कि इतनी हसीन और सोगवार बेवा ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। सफ़ेद कपड़ों में वो अ’जीब पुर-असरार ख़्वाब लग रही थीं। रो-रो कर आँखें मख़मूर और बोझल हो रही थीं। ज़र्द चेहरा पुखराज के नगीने की तरह दमक रहा था। पुरसे को आने वाले सब कुछ भूल कर बस उन्हें तकते रह जाते। उन्हें मरहूम की ख़ुश-नसीबी पर रश्क आ रहा था।
मुमानी पर बे-पनाह बेबसी और अफ़्सुर्दगी छाई हुई थी। ख़ौफ़ और सरा-सीमगी से उनका चेहरा और भी भोला लग रहा था। दोनों बच्चे उनके पहलू से लगे बैठे थे। वो उनकी बड़ी बहन लग रही थीं।
वो गुम-सुम बैठी थीं, जैसे क़ुदरत के सबसे मश्शाक़ फ़नकार ने अपनी बे-मिस्ल क़लम से कोई शाहकार बनाकर सजा दिया हो।


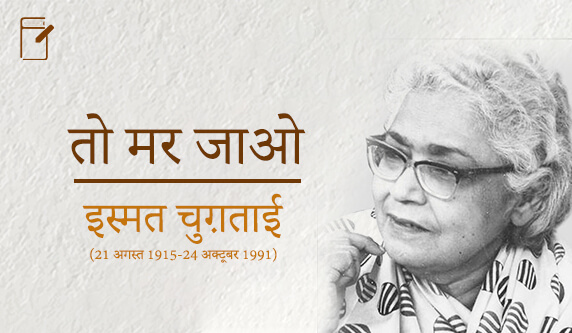


No Comments