- उन मैडम से आज भी माफ़ी मांगनी बाकी है।
- बी ए में एडमिशन
- जिस घटना ने जिंदगी के प्रति मेरा नज़रिया बदला
- बुद्धू होते हैं न प्यार में
- इस घटना ने मुझे लेखक बनाया
- हम दोनों ने प्यार के चक्कर में तमिल सीखी
- आई डोनेशन कार्ड
- वो होली
- वह जानलेवा हादसा
- नमक के बहाने
- पुणे में
- मेरी लेखन यात्रा
1. उन मैडम से आज भी माफ़ी मांगनी बाकी है।
सातवीं में था। देहरादून के गांधी स्कूल में। एक टीचर आयीं संतोष अरोड़ा। वे हिंदी और अंग्रेज़ी पढ़ाती थीं। काम दे देतीं और चुपचाप सोचती रहतीं। उनका एक ही नियम था कि कोई बोले नहीं। मेरे बगल में बैठा प्रदीप अरोड़ा मुझे तंग करने लगा। मैं मना करने लगा तो टीचर ने मुझे बोलते हुए देख लिया। टीचर ने इशारे से मना किया। दूसरी बार, तीसरी बात और चौथी बार। हर बार पिन प्रदीप चुभाता और मैडम की निगाह में मैं आ जाता। आखिर मैडम ने कह ही दिया – सूरज तुम मेरी नज़रों से गिरते जा रहे हो। बहुत शर्म आयी लेकिन कभी उनसे कह नहीं पाया कि गलती मेरी नहीं, प्रदीप की थी हर बार।
उन दिनों इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि स्टाफ रूम में जा कर माफ़ी ही मांग लूं। वे बाद में सेंट्रल स्कूल चली गयीं। संयोग से वहां मेरा छोटा भाई पढ़ता था। कई बार नज़र आयीं लेकिन बात करने की हिम्मत न जुटा पाया कि उस दिन मेरी गलती नहीं थी। वे अक्सर आते जाते नज़र आ जातीं, उनसे नज़रें भी मिलतीं, लेकिन कभी कह नहीं पाया।
इस बात को 49 बरस बीत चुके लेकिन आज भी मुझे ये मलाल है कि मैं उन्हें नहीं बता पाया कि मेरी गलती नहीं थी कि वे अपनी नज़रों से गिरातीं। टीचर्स डे पर आज वे ही याद आ रही हैं।
2. बी ए में एडमिशन
वह 25 नवम्बर 1971 की सुबह थी। दूसरे सेमिस्टर में एडमिशन की आखिरी तारीख थी और घर में सिर्फ 500 रुपये थे जिससे उसी दिन सीमेंट लाया जाना था। डैडी ने मेरा उदास चेहरा देखा और पूछा कि क्या बात है। पूरी बात जानने के बाद भरे मन से वे सारे रुपये मुझे थमा दिये – जा एडमिशन ले ले। घर बनता रहेगा। यह मेरे प्रति उनका पहला त्याग था। मैं आज तक उनकी वे नम आंखें नहीं भूल पाया हूं। भूल सकता भी नहीं। भूलना भी नहीं चाहिये।
3. जिस घटना ने जिंदगी के प्रति मेरा नज़रिया बदला
बात 1977 की है। तब मैं देहरादून में रहता था। पीएचडी करना चाहता था। मैंने विषय चुना था – हिंदी उपन्यासों में असामान्य मनोविज्ञान।
अब संकट यह हुआ कि कोई भी गाइड इस विषय के लिए तैयार नहीं हुआ। जो हिंदी के जानकार थे एवं मनोविज्ञान नहीं जानते थे और जो मनोविज्ञान के जानकार थे, उन्हें हिंदी साहित्य की जानकारी नहीं थी। बहुत मुश्किल से मसूरी कॉलेज के प्रिंसिपल श्री जोशी तैयार हुए। वे शर्त पर मेरे गाइड बनने के लिए तैयार हुए कि मैं खुद ही सारा काम करूंगा लेकिन उनसे कोई मार्गदर्शन नहीं मिल पाएगा। मैं तैयार था। आखिर गाइड मिले तो सही।
उन दिनों एक टुच्ची सी नौकरी कर रहा था।
हर हफ्ते मैटर तैयार करके उन्हें दिखाने के लिए बस से मसूरी जाता और शाम को लौट आता था।
एक बार रविवार के दिन जब मसूरी जाने के लिए बस अड्डे पर आया तो देखा, बहुत लंबी लाइन थी। चार बसें गुज़र जाने के बाद भी मैं लाइन में खड़ा था। बस इतना आगे आ पाया था कि रेलिंग के भीतर पहुंच जाऊं और अगली बस में मुझे सीट भी मिल जाए।
तभी एक सज्जन मेरे पास आए और कहने लगे – हम आज ही दिल्ली से आए हैं, मसूरी जाना है और शाम को लौटना भी है। अगर आप मेहरबानी करके हमारे लिए चार टिकट ले लेंगे तो हमारा काफी समय बच जाएगा।
मैं 2 घंटे से लाइन में झल्लाया खड़ा था और अब तक मेरा नंबर नहीं आया था। उन्हें विश्वास था कि मैं उनकी मदद कर दूंगा। मैंने उनके पीछे देखा, उनका परिवार बहुत हसरत भरी निगाहों से मेरी तरफ देख रहा था।
मैंने मना कर दिया – लाइन में आइए। मेरे मना करने के बाद आगे-पीछे वाले सभी लोगों ने उनकी मदद करने से मना कर दिया।
तभी एक कंडक्टर की आवाज़ आयी – एक स्पेशल बस मसूरी जा रही है। टिकट बस में ही मिलेंगे। वह परिवार स्पेशल बस के एकदम पास ही खड़ा था। सब लपक कर बस में चढ़ गये।
मैं रेलिंग के अंदर होने की वज़ह से बाहर जब तक बाहर निकलता बस भर चुकी थी।
खैर, मैं भी मसूरी गया और दिन भर जोशी साहब के साथ काम करके जब वापस मसूरी के बस अड्डे पर आया तो मेरी सांस अटक गई। 6:30 बज रहे थे और दो ही बसें देहरादून की तरफ जाने के लिए बाकी थीं। आखिरी बस सात बीस पर छूटती थी। किसी भी हालत में मेरा नंबर नहीं आ सकता था। न मेरे पास टैक्सी के लायक पैसे थे और न ही मसूरी में रुकने इंतज़ाम ही था। परेशान हाल मैं सोच रहा था कि क्या करूंगा और कैसे करूंगा तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैंने मुड़ कर देखा। सुबह वाले सज्जन थे। उन्होंने मेरी तरफ एक टिकट बढ़ाया और कहा – यह आपका टिकट है। हम लाइन में बहुत आगे खड़े थे और आपको देख लिया था। हमें पता था कि आपका नंबर नहीं आएगा इसलिए आपके लिए टिकट ले लिया है।
मुझे संकोच में देख कर वे बोले – चिंता ना करें, हम आपसे टिकट के पैसे लेंगे लेकिन एक बात याद रखना। आप मदद करें या ना करें, कभी भी किसी का काम रुकता नहीं है, लेकिन अगर आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा है और सामने वाले की मदद कर सकते हैं ज़रूर कर देनी चाहिए। मुझ पर घड़ों पानी पड़ गया था।
आप समझ सकते हैं मेरी क्या हालत हुई होगी।
वह दिन और आज का दिन।
ज़िंदगी के प्रति और दूसरों के काम आने के प्रति मेरा नज़रिया ही बदल गया था।
ये बात अलग है कि मेरी पीएचडी कभी पूरी नहीं हुई। बेशक मेरे लेखन पर ही कई शोध हो चुके।
4. बुद्धू होते हैं न प्यार में
जब वह अगली बार मिली तो बताया उसने – कल देर शाम हमारे घर टेलिफोन लग गया है।
मैंने बधाई दी और कहा कि ये तो बहुत ही अच्छी खबर है।
तभी उसने बताया कि जब कल शाम आठ बजे फोन चालू हुआ तो सबसे पहले मैंने ही उसका उद्घाटन किया और तुम्हारा नंबर डायल किया।
मैं हैरानी से बोला – अरे, तुम्हें पता तो है कि हमारा ऑफिस छह बजे बंद हो जाता है।
वह भड़की – तुम निरे बुद्धू हो। पता नहीं, तुम्हारे प्यार में कैसे पड़ गयी।
और वह उस दिन सचमुच नाराज़ हो कर चली गई थी।
कई दिन बाद मुझे समझ में आया था कि वह मुझसे कितना प्यार करती थी कि फोन पर सबसे पहले मेरा ही नंबर डायल करने का जो सुख उसने पाया था, मुझसे साझा करना करना चाहती थी। बेशक जानती थी कि बंद ऑफिस में देर तक घंटी बजती रहेगी।
हम कितने बुद्धू होते हैं न कि प्यार की अलग इबारतें समझ ही नहीं पाते।
5. इस घटना ने मुझे लेखक बनाया
कविता की तुकबन्दी बेशक मैंने तेरह बरस की उम्र में शुरू कर दी थी लेकिन अपनी पहली कहानी लिखने के लिए मुझे अगले बीस-बाइस बरस तक इंतज़ार करना पड़ा था। भीतर बहुत कुछ था जो लिखना चाहता था लेकिन शब्द नहीं सूझते थे कि क्या और कैसे लिखना है। कहानी बन ही नहीं पाती थी। तभी ये घटना हुई थी जिसने मुझे लेखक बनाया और बरसों से अटकी हुई अभिव्यक्ति को रास्ता मिला था।
1980 के आसपास की बात है। तब मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड में काम करता था। तभी वहां एक नए लड़के वोरा ने जूनियर असिस्टेंट के रूप में ज्वाइन किया। उससे पहले वह बिक्री कर विभाग में काम करता था। हम सब हैरान थे कि इतनी अच्छी ऊपर की कमाई वाली नौकरी छोड़कर वह क्लर्क बनने क्यों आया है।
उसने जो कुछ बताया था उसे सुनकर मैं दहल गया था। बेशक इसी घटना से ही मेरा लेखन शुरू हुआ था। यह घटना मुझे कई बरस तक मथती रही। तब तक मैं बंबई आ गया था।
तब मैंने इस घटना को एक लघुकथा के रूप में लिखा था। 1984 में यह लघुकथा सारिका की सर्व भाषा लघुकथा प्रतियोगिता में एक हजार लघु कथाओं में से पहले नंबर पर चुनी गई थी। इसी लघुकथा को पढ़कर विविध भारती से कवि अनूप सेठी ने मुझे कहानी रिकार्ड करने के लिए बुलाया था। उनके लिए मैंने अपनी पहली कहानी अल्बर्ट लिखी थी। यह कहानी अगले पच्चीस बरस तक मेरी फाइलों में रही और पहली बार 2009 में छपी थी।
घटना यूं थी कि वोरा को जब बिक्री कर विभाग में नौकरी मिली तो संयोग से उसे वह डेस्क मिली जहां ऊपर की कमाई होती थी। उसे पहले ही दिन बता दिया गया था कि किस दर से रिश्वत लेनी है, किस-किस से लेनी है, कहां और किस समय लेनी है और ली गई रिश्वत किस-किस के बीच बंटेगी। वह बेशक ईमानदार परिवार से आया था लेकिन ऊपर की कमाई का लालच बहुत बड़ा था और वह जल्दी ही इस दुष्चक्र में फंस गया। अपना और अपने सीनियर्स का भला करने लगा।
संयोग से उसके पिताजी की किराने की दुकान जिस बाजार में थी उस इलाके की फाइलें उसी की डेस्क से क्लियर होनी थीं। वरिष्ठ अधिकारी कहीं अन्यथा ना लें इसलिए उसने अपने साथी क्लर्क से कहा कि यह केस मेरे पिताजी की दुकान का है, जरा देख लेना।
साहब ने केस क्लियर तो कर दिया था लेकिन साथी क्लर्क से पूछ लिया था कि सच में ये दुकान वोरा के पिताजी की है या पूरा कमीशन अकेले खाने के लिए उन्हें बाप बना लिया है।
6. हम दोनों ने प्यार के चक्कर में तमिल सीखी
उन दिनों मैं दिल्ली में था। मंटो के शब्दों में कहें तो तब हम दोनों एक दूसरे के प्यार में घुटने-घुटने डूबे हुए थे। जब तक हम एक ही ऑफिस में थे तो चल जाता था। दिन में कई बार बात भी और मुलाकात भी हो जाती थी लेकिन जब मैं नौकरी बदल कर दूसरे ऑफिस में चला गया तो बात करने और मिलने के मौके दुर्लभ होते चले गए। वह जिस हॉल में बैठती थी वहां पर एक ही कॉमन फोन था और जब वह मुझसे बात करती थी तो पूरे ऑफिस को खबर हो जाती थी। यह बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी।
हमें मिले हुए बहुत दिन हो गए थे सो सोचा, लंच के बाद उसके घर के पास ही उससे मिला जाए। उसका घर और ऑफिस पास-पास ही थे और वह लंच के लिए घर जाया करती थी। आधे दिन की छुट्टी ले कर एक लंबी मुलाकात हो जाती।
उसका इंतज़ार करते समय तभी मैंने वहां दीवार पर एक पोस्टर देखा – छह महीने में तमिल सीखें। कक्षाएं मंगल और शुक्रवार, शाम छह से आठ बजे तक। पढ़ते ही दिल खुश हो गया।
वह आयी तो नाराज़ होने लगी – यहां क्यों खड़े हो। मैंने बताया – नाराज़ बाद में हो लेना, पहले इसे पढ़ो। दो-तीन बार पढ़ने के बाद उसे भी समझ में आ गया कि हमारी नियमित मुलाकातों के लिए कितना अच्छा मौका दिया जा रहा है। कक्षाएं आर के पुरम के सेक्टर छह में दिल्ली तमिल संगम में लगनी थी। यह जगह उसके घर से बहुत दूर नहीं थी।
हमने अगले ही दिन सबसे पहले जाकर एडमिशन ले लिया।
हमने अगले 6 महीने तक लगातार हफ्ते में दो बार, दो ढाई घंटे एक साथ क्लास में बैठकर खूब इश्क भी लड़ाया और तमिल भी सीखी। इन दो दिनों में कितने भी ज़रूरी काम हों, हम क्लास मिस नहीं करते थे।
आखिरी बात यह कि हम दोनों ने ही इस तमिल कोर्स में टॉप किया था। हमने तमिल में इतनी महारत हासिल कर ली थी कि कई बार फोन पर भी तमिल में बात करते थे, प्रेम पत्र भी तमिल में लिखते थे और अक्सर बात भी तमिल में करते। इस पूरे अरसे के दौरान मैंने मंगलवार और शुक्रवार को किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। ये दो दिन प्रेम के लिए समर्पित थे।
7. आई डोनेशन कार्ड
तारीख थी 27 फरवरी 1989 । सोमवार। बंबई में मेरा आखिरी दिन था और रात की ट्रेन से मुझे ट्रांसफर पर अहमदाबाद जाना था। मुझे अपनी बाइक साथ ले जानी थी इसलिए बाइक पर ही स्टेशन जा रहा था। घर से निकला तो पड़ोस की एक परिचित लड़की ने पूछा – अंकल कहां जा रहे हैं। जब मैंने बताया कि बंबई सेंट्रल तो उसने कहा कि अंकल मुझे रास्ते में षण्मुखानंद हॉल के पास छोड़ देंगे। मुझे क्या एतराज हो सकता था। मेरे रास्ते में ही पड़ता था।
जब उसकी मंज़िल के पास पहुंचे तो उसने सड़क के सिरे पर ही कहा – अंकल यहीं पर छोड़ दीजिए। आगे मैं पैदल चली जाऊंगी। उसे उतार कर ज्यों ही मैंने मोटरसाइकिल मोड़ी तो सामने पुलिस वाला खड़ा था। मुझे रोका और पूछा – ये वन वे है। आप वन वे से कैसे आ रहे हैं। मैंने बताया कि मैं वन वे से नहीं आ रहा हूं। यहीं यू टर्न लिया है। पुलिस वाला जिद पर अड़ गया कि मैंने आपको अंदर से आते हुए देखा है। मैं अपनी बात पर अड़ा रहा कि मैं यहीं पर मुड़ा हूं।
तब उस पुलिस वाले ने कहा कि मेरे बॉस से मिलिए। जब मैं उसके सीनियर पुलिस वाले के पास गया तो वह भी कहने लगा – मैंने भी आपको वन वे से आते हुए देखा है। चालान तो होगा। लाइसेंस दिखाइए। मैंने फिर कहा कि मैं रिज़र्व बैंक में ऑफिसर हूं और मैं झूठ नहीं बोलूंगा और वैसे भी आज बंबई में मेरा आखिरी दिन है। पहले ही परेशान हूं। स्टेशन ही जा रहा हूं। मिस्टर पठान नाम के उस पुलिस अधिकारी ने कुछ नहीं सुना और लाइसेंस मांगा। जब मैंने उन्हें लाइसेंस निकाल के दिया तो लाइसेंस उनके हाथ से नीचे गिर गया। जब उन्होंने उठाया तो प्लास्टिक जैकेट में लाइसेंस के दूसरी तरफ रखा आई डोनेशन कार्ड देखा।
पठान ने पूछा – यह कार्ड क्या है। मैंने बताया कि अगर किसी दुर्घटना में मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरी आंखें दान दी जा सकती हैं। सामने ही तिलक अस्पताल है यहां पर भी मेरी आंखें दान दी जा सकती हैं। तब पठान ने पूछा – यह कार्ड कैसे बनता है तो मैंने बताया कि टेलिफ़ोन डाइरेक्टरी में पहले पन्ने पर इसका विज्ञापन होता है, टाइम्स आइ फाउंडेशन में भी फॉर्म भर के आंखें दान की जा सकती हैं और किसी भी अस्पताल में फॉर्म भर कर ये काम किया जा सकता है।
तब पठान ने मुझे सैल्यूट किया और मुझसे हाथ मिलाते हुए लाइसेंस और कार्ड वापिस करते हुए कहा – जो व्यक्ति अपनी आंखें दान कर सकता है, वह एक मामूली चालान के लिए झूठ नहीं बोलेगा। जाइये सर। हमसे गलती हुई।
8. वो होली
कई होलियाँ याद आती हैं। बचपन के शहर देहरादून की होलियाँ जहाँ बड़े लोग झांझ मझीरे ले कर फ़िल्मी गानों की अश्लील पैरोडियाँ गाते हुए गली मोहल्लों में निकलते थे। हमें सहसा यकीन नहीं होता था कि ये बड़े भाइयों सरीखे युवा लोग, जिनकी हम इतनी इज़्ज़त करते हैं और उनसे इतना डरते हैं, इस तरह से सरेआम अश्लील गाने भी गा सकते हैं।
बाद में जब हैदराबाद गया तो वहाँ की होलियाँ याद आती हैं। लोग अपने चेहरे पर पहले ही सफ़ेद रंग का कोई पेंट पोत कर निकलते थे ताकि उस पर कोई दूजा रंग चढ़े ही नहीं। फिर बाद में मुंबई की होलियाँ। रंग खेलने के बाद जुहू तट पर जाना याद आता है जहाँ हज़ारों लोग रंग खेलने के बाद हरहराते समंदर के साथ होली खेलने आते हैं और समंदर सबसे थोड़ा थोड़ा रंग ले कर बहुत रंगीन हो जाता है और जब ठाठें मारता हुआ सबसे होली खेलने के लिए हर ऊंची लहर के साथ सबको गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है तो बहुत ही रमणीय नज़ारा होता है।
वैसे मुंबईवासी अपनी ही सोसाइटियों में होली खेलते हैं। बहुत ऊंची आवाज़ में संगीत, एक दूजे की बीवियों पर बाल्टी भर-भर कर या माली वाले पाइप से पानी डालना, बस यही होली होती है, आम मुंबइया बाबुओं की। सड़कों पर टोलियाँ कम ही निकलती हैं। हाँ, कुछ लोग पी-पा कर सड़क पर शाम तक बेसुध पड़े रहते हैं। कुछेक युवा हा हा हू हू करते हुए तेज़ रफ़्तार गाड़ियाँ चलाते भी नज़र आ जाते हैं।
अब तो कई बरसों से होली खेलना ही छोड़ दिया है। बहुत हो ली होली। अगर कपड़े गीले करवाना ही होली है तो नहीं खेलनी मुझे। पहले से तय नहीं रहता कि होली खेलने नीचे उतरना है या नहीं। मूड बना तो ठीक वरना घर पर ही भले।
मैं यहाँ अहमबाद की जिस होली का ज़िक्र कर रहा हूँ, दरअसल ये घटना होली के दिन की नहीं, शाम की है। स्थानीय अख़बार गुजरात वैभव ने किसी पार्टी प्लॉट पर रात्रि भोज का निमंत्रण दिया था। मैं और मेरे कवि मित्र श्री प्रकाश मिश्र भी आमंत्रित थे। वैसे हम दोनों कहीं भी एक साथ जाते थे तो मेरी मोटर साइकिल पर ही चलते थे, लेकिन उस दिन पता नहीं कैसे हुआ कि उनके स्कूटर पर ही चलने की बात तय हुई। शायद सात आठ कि.मी. जाना था।
जब वहाँ पहुँचे तो कई परिचित लोग मिले। बातचीत होती रही। खाने से पहले भांग मली ठंडाई का आयोजन था। मैंने भी लोगों की देखा देखी दो एक गिलास ठंडाई ले ली लेकिन कुछ ख़ास मज़ा नहीं आया। तभी आयोजक शर्मा परिवार के सबसे युवा मनीष शर्मा जो मेरे अच्छे परिचित थे, मेरे पास आए और बात करते हुए अचानक उन्होंने पूछा कि मैंने ठंडाई ली है या नहीं। जब मैंने बताया कि हाँ, ली तो है लेकिन मुझे तो इसमें कोई ख़ास बात नज़र नहीं आई। वे मुस्कुराए और मेरी बाँह पकड़ कर मुझे एक तरफ़ ले जाते हुए बोले, अरे, इस चालू ठंडाई में थोड़े ही मज़ा है, आइए मैं आपको ख़ास तौर पर ख़ास मेहमानों के लिए बनाई गई ठंडाई पिलाता हूँ।
वे मुझे एक कमरे में ले गए जहाँ ख़ास लोगों के लिए ख़ास ठंडई का इंतज़ाम था। एक बड़ा गिलास मुझे पेश किया गया और तब मुझे लगा, हाँ इस गिलास में कुछ था। एक गिलास हलक से नीचे उतारा ही था कि उनके बड़े भाई ने एक और गिलास ज़बरदस्ती पिला दिया।
साढ़े नौ बजने को आए थे। मेहमानों ने भोजन करना शुरू कर दिया था। ज़मीन पर बिछी जाजमों पर बैठ कर भोजन करना था। स्वादिष्ट भोजन था। पूरी कचौरी, हलवा वगैरह और गुजरात के स्थानीय और होली के व्यंजन।
अब तक भांग ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। मैं खाना तो खा रहा था लेकिन धीरे-धीरे मुझे महसूस होना शुरू हुआ कि मुझे खाने के हर निवाले के लिए अपना हाथ धरती में बहुत नीचे तक ले जाना पड़ रहा है और मेरा हाथ वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। पानी पीना चाहा तो गिलास तक हाथ ही न पहुँचे। मेरी हालत ख़राब हो रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा भूख और प्यास लगी थी लेकिन किसी भी चीज़ तक मेरा हाथ ही नहीं पहुँच पा रहा था। मैं ऊँचाई और गहराई का अहसास खो चुका था। मैं भुनभुना रहा था, बड़बड़ा रहा था लेकिन किसी तक भी अपनी आवाज़ नहीं पहुँचा पा रहा था कि कोई मुझे बताए कि मैं क्या करूँ। पंगत में साथ बैठे खाने वाले कब के खा कर जा चुके थे और मेरी पत्तल में अभी भी खाने की चीज़ें जस की तस पड़ी हुई थीं और मैं बेहद भूखा था।
शायद मैं आधा घंटा तो इसी हालत में बैठा ही रहा होऊँगा। तभी श्री प्रकाश मिश्रा जी मुझे ढूँढते हुए आए और बोले चलो भई, बहुत खा लिया तुमने। और कितना खाओगे। साढ़े ग्यारह बज रहे हैं। चलना नहीं है क्या।
मैं आधे अधूरे पेट उठा तो दूसरी समस्या शुरू। उनके स्कूटर की सीट मुझे इतनी ऊँची लग रही थी कि मैं किसी तरह भी उस पर चढ़ नहीं पा रहा था। आस पास तमाशबीन जुट आए थे। मैं लगातार इस बात का रोना रो रहा था कि मैं आख़िर इतनी ऊँची सीट पर चढूँ कैसे? तभी मैंने देखा कि चार पाँच आदमियों ने मुझे किसी तरह से गोद में उठा कर स्कूटर पर बैठा ही दिया है। श्री प्रकाश जी ने स्कूटर स्टार्ट कया और मैंने उन्हें पीछे से कस कर पकड़ लिया।
अब एक और मुसीबत शुरू हो गई मेरे साथ। मुझे लगा कि ये स्कूटर अनंत काल से चल ही रहा है और हम कहीं नहीं पहुँच रहे। मैंने कम से कम बीस बार तो मिश्रा जी से पूछा ही होगा कि हम पहुँच क्यों नहीं रहे हैं।
आख़िर जब मुझे अपना घर नज़र आया तो मैं छोटे बच्चे की तरह् खुशी से चल्लाने लगा क मेरा घर आ गया। म जी ने मुझे किसी तरह से स्कूटर से उतारा, मेरी जेब से चाबी निकाली और दरवाज़ा खोला। मिश्रा जी कब वापस गए और मैं कब सोया, मुझे कोई ख़बर नहीं। अलबत्ता सुबह जब उठा तो पिछली रात की अपनी सारी बेवकूफ़ियाँ मुझे याद थीं। हँसी भी आ रही थी कि भांग भी क्या चीज़ है कि अच्छे भले आदमी का कार्टून बना देती है।
9. वह जानलेवा हादसा
10 दिसम्बर 2007 की सर्द सुबह थी वह। सवेरे साढ़े पांच बजे का वक्त। मुझे फरीदाबाद से नोयडा जाना था राष्ट्रीय स्तर के एक सेमिनार के सिलसिले में। सेमिनार के आयोजन का सारा काम मेरे ही जिम्मे था। पिछली रात मैं मेजबान संस्थान के जिस साथी के साथ नोयडा से फरीदाबाद अपने माता पिता से मिलने आया था, अचानक उसका फोन आया कि वह बाथरूम में गिर गया है और उसकी हालत खराब है। बताया उसने कि डॉक्टर ने उसे कुछ देर आराम करने के लिए कहा है। जब आधे घंटे तक उसका दोबारा फोन नहीं आया तो मैंने ही उससे पूछा कि अब तबीयत कैसी है। उसने बताया कि वह नोयडा तक कार चलाने की हालत में नहीं है। हां, जाना तो ज़रूर है। मैंने प्रस्ताव रखा कि वह घबराये नहीं, मैं ही कार चला लूंगा। उसका घर मेरे पिता जी के घर से 12 किमी दूर था। पहले तय कार्यक्रम के अनुसार वही मुझे लेने आने वाला था लेकिन अब नये हालात में मुझे ही उसके घर या उसके आस पास तक जाना था। हमने मिलने की जगह तय की और मैं अपने पिताजी के साथ उनके स्कूटर पर चल पड़ा ताकि कोई ऑटो लिया जा सके। मेरे 82 वर्षीय पिता बहुत जीवट वाले व्यक्ति हैं और इस उम्र में भी अने सारे काम अपने स्कूटर पर ही यात्रा करते हुए करते हैं। पता नहीं ज़िंदगी में पहली बार ऐसा क्यों हुआ कि जब मैं उनके पीछे स्कूटर पर बैठा तो मुझे लगा कि आज कुछ न कुछ होने वाला है। हमें मथुरा रोड हाइवे तक कम से कम तीन किलोमीटर जाना था। अब तक कोई आटो नहीं मिला था। रास्ते पर कोहरा और अंधेरा थे जिसकी वज़ह से वे बहुत धीमे धीमे स्कूटर चला रहे थे। मथुरा रोड हाइवे अभी सौ गज दूर ही रहा होगा कि सड़क पर चलते तेज यातायात को देखते ही कुछ देर पहले अनिष्ट का आया ख्याल एक बार दोबारा मेरे दिमाग में कौंधा। लगा वह घड़ी अब आ गयी है। मैंने पिताजी को सावधान करने की नीयत से कुछ कहना चाहा और उनके कंधे दबाये।
उसके बाद न तो मुझे होश रहा न उन्हें। हम शायद पन्द्रह मिनट तक वहीं चौराहे पर बेहोश पड़े रहे होंगे। अचानक पसलियों में तेज, जान लेवा दर्द उठा और मुझे होश आया। मैं सड़क पर औंधा पड़ा हुआ था और दर्द से छटपटा रहा था। मैं समझ गया वो कुघड़ी आ कर अपना काम कर गयी है। मुझे तुरंत पिताजी का ख्याल आया लेकिन कोहरे, अंधेरे और अपनी हालत के कारण उनके बारे में पता करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। जब मेरी आंखें खुलीं तो मैंने कई चेहरे अपने ऊपर झुके देखे। मैं कराह रहा था। दर्द असहनीय था, इसके बावजूद मैंने अपनी जैकेट की जेब से अपना मोबाइल निकाल कर लोगों के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया कि कोई मेरे पिताजी के घर पर फोन कर दे। मैं ज़ोर ज़ोर से उनके घर का नम्बर बोले जा रहा था। लेकिन शायद वे रात की या सुबह की पाली वाले मजदूर थे। मोबाइल उनके लिए अभी भी अनजानी चीज़ रही होगी। अंधेरा और कोहरा भी शायद अपनी भूमिका अदा कर रहे थे। कोई भी तो आगे नहीं आ रहा था।
मेरा दर्द असहनीय हो चला था। तभी मेरे मोबाइल की घंटी बजी। और देवदूत की तरह कोई युवक वहां आया। उसने मेरे हाथ से फोन ले कर अटैंड किया। दूसरी तरफ वही साथी थे जो मेरा इंतज़ार कर रहे थे और देरी होने के कारण चिंता में पड़ गये थे। उसी युवक ने उन्हें बताया कि आप जिनका इंतज़ार कर रहे हैं, वे तो सड़क पर जख्मी पड़े हैं। तब उसी युवक ने उनके और मेरे अनुरोध पर पिताजी के घर पर फोन किया। उस फैकल्टी ने एक अच्छा काम और किया कि तुरंत मेरे बड़े भाई के घर पर जा कर इस हादसे की खबर दी और उन्हें साथ ले कर घटना स्थल तक आया। वह खुद बुरी तरह से घबरा गया था। शायद दस मिनट लगे होंगे कि दोनों तरफ से भाई आ पहुंचे। जब तक हम एस्कार्ट अस्पताल तक ले जाये जाते, वे आस पास रह रहे सभी नातेदारों को खबर कर चुके थे।
हमें अब तक नहीं पता कि किस वाहन ने हमें किस कोण से टक्कर मारी थी। स्कूटर हमसे कई गज दूर तीन हिस्सों में टूटा पड़ा था। तमाशबीनों ने हमारे ओढ़े हुए शाल ही हमारे बदन पर डाल दिये थे और शायद हमें सड़क पर किनारे भी कर दिया था।
मेजबान संस्थान के साथी की तबीयत ज्यादा खराब हो गयी थी लेकिन खुद अस्पताल भरती होने से पहले नोयडा में अपने संस्थान में हादसे की खबर कर दी थी। मुझे तीसरे दिन होश आया, पांच दिन आइसीयू में रहा और पन्द्रह दिन अस्पताल में। दायें पैर में मल्टीपल फ्रैक्चर। कुचली हुई पांच पसलियां और दायें कंधे पर भी फ्रैक्चर। पिता जी की दोनों टांगों में फ्रैक्चर और ब्लड क्लाटिंग। वे हाल ही की सारी बातें भूल चुके हैं। हादसे के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं। अभी मुझे खुद दो महीने और स्तर पर रहना है लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ हम दोनों ठीक हो जायेंगे। ज़ोर का झटका बेशक ज़ोर से ही लगा है लेकिन हम दोनों बच गये हैं।
इस पोस्ट के जरिये मैं उन सभी मित्रों, शुभचिंतकों, ब्लाग मित्रों के प्रति आभार शब्द प्रयोग कर उनके और अपने बीच संबंधों की गरिमा को कम नहीं करना चाहता। सभी ब्लागों पर मेरे परिचित और अपरिचित मित्रों की ओर से मेरे शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की खबर मुझे मिलती रही। हिंदयुग्म ब्लाग के मित्रों ने तो ज़रूरत पड़ने पर रक्त दान के लिए इच्छुक रक्त दाताओं की सूची भी तैयार कर ली थी। मैं जानता हूं कि आप सब की प्रार्थनाओं, दुआओं और शुभेच्छाओं से हम दोनों जल्द ही चंगे हो जायेंगे लेकिन आप सब का प्यार मेरे पास आपकी अमानत रहेगा।
हमेशा।
हमेशा।
मुझे अभी दो महीने और बिस्तर पर गुज़ारने हैं। ज्यादा देर तक पीसी पर बैठना मना है। एक हाथ से ये पोस्ट टाइप की है। पिता जी भी स्वस्थ हो रहे हैं। बस, इस बात का मलाल रहेगा कि हम उस अनजान युवक को धन्यवाद नहीं कह पा रहे जिसने मेरे हाथ से फोन ले कर हमारे घर तक हादसे की खबर पहुंचायी थी और हम बच पाये।
प्रसंगवश, उस वक्त पिताजी के पास मोबाइल नहीं था और मेरे पुणे के मोबाइल में दर्ज नम्बरों से उस अंधेरे और कोहरे में फरीदाबाद का काम का नम्बर खोजना इतना आसान नहीं होता।
मार्च 2008
10. नमक के बहाने
पुणे में वह मेरा आखिरी दिन था। लगभग पचास महीने वहां बिताने के बाद मैं मुंबई वापिस जा रहा था। जो दो-एक दावतनामे थे, वे निपट चुके थे। मैं वहां अपने आखिरी दिनों में होटलों में ही खाना खा रहा था। बेशक सामान बाद में ले जाता, मैं अगली सुबह वापिस जा रहा था। धीरे-धीरे ही सही सारी किताबों की पैकिंग मैंने खुद की थी और बाकी सामान मेरा नौकर मोहिते पैक करता रहा था। रसोई समेटने का काम वही कर रहा था। डिब्बे वगैरह खाली करके मसाले, दालें और दूसरी चीज़ें उसे ले जाने के लिए मैंने कह दिया था। उसे ये ज़रूर कह दिया था कि थोड़ा-सा नमक, काली मिर्च और मक्खन का एक पैकेट वह आखिरी दिन तक खुले रखे रहे। रसोई का बाकी सामान या तो पैक कर दे या अपने घर ले जाये।
तो जिस दिन का किस्सा है ये, अचानक झमाझम बरसात शुरू हो गयी। तीन चार घंटे लगातार पानी बरसता ही रहा। कार शाम को ही मुंबई भिजवा चुका था। अब कैसे भी करके होटल खाना खाने नहीं जाया जा सकता था। पैर के दूसरे ऑपरेशन के बाद बैकम शू पहन कर चलता था। बहुत ज्यादा चलना मना था और इस बरसात में इतना महंगा जूता बरबाद तो नहीं ही किया जा सकता था। साढ़े नौ बजने को आये थे। बरसात जैसे रात भर होने का परमिट ले कर आयी थी। मैं बार-बार बाल्कनी में आता और बरसात का जायज़ा लेता। ऑटो वैसे भी दिन में नहीं मिलता, रात के वक्त मिलने के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता था।
जब ये तय हो गया कि बरसात तो नहीं ही रुकने वाली, मैंने घर पर ही कुछ बनाना तय किया। अब मुझे ये नहीं पता था कि मोहिते ने किस कार्टन में क्या पैक किया है या खाने का सामान कुछ छोड़ा भी है या नहीं। संयोग से तीन चार कार्टन खंगालने के बाद प्रेशर कुकर, चावल और मूंग मिल गये। सोचा मैंने, पहले दाल-चावल ही भिगो लिये जायें फिर मसाले तलाश किये जायें।
मैंने आधे घंटे की मेहनत के बाद लगभग सारे कार्टन खोल डाले लेकिन नमक कहीं नहीं था। फ्रिज में रखा थोड़ा-सा मक्खन ज़रूर मिल गया। नमक सहित सारे मसाले ले जाये जा चुके थे। अब क्या हो। भूख अपनी जगह कायम थी और बरसात अपनी जगह। नमक लाने के लिए बाज़ार तक जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मैं जिस इमारत में रहता था उसके आठ फ्लैट्स में मेरे अलावा चार और ऑफिसर्स रहते थे। बाकी फ्लैट्स खाली थे। एक ही संस्थान में होने और एक ही इमारत में रहने के बावजूद उनसे संबंध ऐसे नहीं थे कि पहली बार उनके घर जा कर नमक मांग सकूं। सामने वाली बिल्डिंग में गेस्ट हाउस था और उसके पीछे वाली इमारत तक कभी गया ही नहीं था। बेशक वहां भी हमारे ही संस्थान के ही लोग रहते थे।
अब फीकी खिचड़ी तो नहीं ही खायी जा सकती थी। चम्मच भर नमक का सवाल था जो मैं हल
नहीं कर पा रहा था। काफी देर तक अंदऱ-बाहर होता रहा कि क्या करूं। अपने आप पर, अपने वक्त पर और अपनी जीवन शैली पर अफ़सोस होता रहा कि चम्मच भर नमक लायक संबंध भी नहीं रहे हैं हमारे। बार-बार संकोच आड़े आता रहा और मैं नमक नमक जपता रहा।
इसी अंदर-बाहर की चहलकदमी में अपने बचपन के कितने ही ऐसे प्रसंग याद आते रहे जब मां
ने हमारी पसंद का कुछ नहीं बनाया होता था तो पूरे मोहल्ले की रसोई हमारे लिए अपनी होती थी और हम किसी भी पड़ोसी के घर में जा कर खाना खा सकते थे। पूरे मोहल्ले की रसोई हमारे लिए सांझी होती थी। मज़ाल है किसी घर में कोई ख़ास पकवान बना हो और वह दस घरों में सबके हिस्से में न आये। बिना नमक वाली इस झमाझम बरसात में ये भी शिद्दत से याद आया कि छोटा-सा एक तंदूर पूरे मोहल्ले में सिर्फ हमारे घर में था और जिस दिन हमारी मां दोपहर के वक्त तंदूर तपाने का फैसला करती, आस पास के दस घरों में पहले खबर कर दी जाती और मोहल्ले की सारी चाचियां-मासियां तंदूर को गरम बनाये रखने के वास्ते अपने हिस्से की दो-चार लकडि़यां और गूंथे आटे की परात ले कर आ जातीं। हम बच्चों की मौज हो जाती। उसी छोटे से तंदूर में से बारी-बारी से सोंधी-सोंधी गंध लिये कभी मिस्सी रोटी निकल रही है, तो कभी प्याज के
पराठे निकल रहे हैं। मक्की की रोटी निकल रही है और रात की बची दाल डाल कर बनाये गये पराठे भी। अगर किसी बच्चे को अपनी मां के हाथ की सादी रोटी पसंद नहीं है तो किसी भी चाची की परात में से अपनी मन पसंद रोटी ले लो। खुशी-खुशी मिलेगी।
खाना बनाना निपट जाने के बाद तंदूर की बाकी बची आंच का इस्तेमाल मिट्टी की हांडी में उड़द
और चने की दाल बनाने के लिए किया जाता था और ज़रूरी नहीं कि ये दाल हमारी ही बन रही हो। जिसका मन आये, दाल की हांड़ी चढ़ा सकती थी। आखिर ये दाल भी तो चार घरों में पहुंचती ही थी।
सब दिन हवा हुए। मैं अपने बचपन के यानी चालीस-पैंतालीस साल पहले के दिन याद कर रहा था
और सोच रहा था कि या तो भूखा सोऊं या फीकी खिचड़ी खाऊं। नमक मांग कर लाने की हिम्मत नहीं ही हुई।
तभी एक चमत्कार हुआ। रात दस बजे की पाली वाला सिक्युरिटी गार्ड आ चुका था और जाने
वाले गार्ड से चार्ज ले रहा था। उसने मेरी बाल्कनी की तरफ देखा और आदतन मुझे सलाम किया। सलाम के जवाब में मैंने उसे ऊपर आने का इशारा किया। जब वह ऊपर आया तो मैंने उसे अपनी समस्या बतायी। हैरानी की बात, गार्ड को मालूम था कि मोहिते नमक सहित सारे मसाले और दूसरा सामान कल ही अपने घर ले गया है। गार्ड ने खुशी-खुशी मेरे लिए बाज़ार से नमक लाना मंज़ूर किया और मैंने पुणे में बितायी अपनी आखिरी रात को नमक वाली खिचड़ी खायी।
गार्ड बेशक भरी बरसात में भीगते हुए मेरे लिए नमक ले कर आया था, उस नमक की अपनी सीमा थी। उस नमक में सिर्फ खिचड़ी को नमकीन कर सकने का गुण था। जीवन को लवणयुक्त बनाने का गुण उसमें नहीं था। मिल-बांट कर जीवन जीने से जो लवण आता है हमारे हिस्से में, सारे मतभेदों के बावजूद जो नमक हमारी मर्यादा को ढंके रहता है, हमारी चार कमज़ोरियों पर पर्दा किये रहता है जो साझा नमक, ये वो नमक नहीं था।
क्या अब भी कहीं मिलता है वो नमक। मिले तो बताना।
03 जुलाई 2009__
11. पुणे में
लगभग चार बरस और दो महीने बिताने के बाद आज अपनी 29 बरस पुरानी कर्मस्थली मुंबई लौट रहा हूं। मुंबई आना जाना पहले भी होता रहा है। 1989 से 1995 तक मैं अहमदाबाद में रहा था और तब मैं वहां से बहुत अमीर हो कर लौटा था। ज़िंदगी के सही मायनों में अमीर। वहां ढेरों मित्र बने, खूब घुमक्कड़ी की, ट्रैकिंग की, गुजराती भाषा सीखी और कई किताबों के अनुवाद किये थे। खूब मस्ती की थी और गम्भीर साहित्य पढ़ा था। शास्त्रीय संगीत सुनने और गुनने की तमीज वहीं आयी थी। वहीं रहते हुए सीखा था कि शनिवार की दोपहर से ले कर सोमवार की सुबह तक मौन कैसे रहा जा सकता है। एक बार नहीं, कई बार।
एक तरह से वहीं रहते हुए लिखना शुरू हुआ था और पहला कहानी संग्रह वहीं रहते हुए आया था। तभी गुजरात साहित्य अकादमी बनी थी और आस पास और कोई कहानीकार न पा कर उन्होंने पहला साहित्य अकादमी सम्मान मुझे ही थमा दिया था। तब शहर में आने वाले अमूमन सभी साहित्यकारों के सम्मान में साहित्यिक जमावड़े मुझ छड़े के घर पर ही होते थे। हम यार दोस्त तो आपस में मिल कर धमाल मचाते ही थे।
शायद तब दो एक बातें मेरे पक्ष में थीं। एक तो उम्र तब चालीस से कम थी और मैं साहित्य का ककहरा सीख रहा था। अहमदाबाद जाते समय मेरे पास कुल जमा तीन कहानियों की जमा पूंजी थी। हंस में यह जादू नहीं टूटना चाहिये और धर्मयुग में अधूरी तस्वीर तब छपी ही थीं। वर्तमान साहित्य में उर्फ चंदरकला अहमदाबाद में रहते हुए ही आयी थी और मैं रातों रात उस वक्त का सबसे विवादास्पद लेखक बन चुका था। इस तरह से गुजरात ने मुझे बहुत कुछ दिया था और जब मैं वहां से लौटा था तो बेशक कहानियां ज्यादा नहीं थीं मेरे पास लेकिन अगले दस बरस के लेखन के लायक कच्चा माल मेरे पास था और मैं उसी की पुडि़या बना बना कर लिखता छपता रहा।
मैं दूसरी बार मुंबई में 1995 से 2005 तक रहा और नौकरी के चक्कर में बेहद व्यस्त रहने के बावजूद मेरी मूल, अनूदित और संपादित 17 किताबें आयीं।
लेकिन सच कहूं तो पुणे यानी पुण्य नगरी में पचास महीने बिता कर जाने के बाद भी मैं लगभग खाली हाथ ही वापिस जा रहा हूं। एक भी कहानी नहीं लिखी। बस, चार्ली चैप्लिन और चार्ल्स डार्विन के अनुवाद ही हो पाये। बेशक पढ़ा खूब और फिल्में भी खूब देखीं लेकिन मैं पुणे में कुछ नया लिखने, दोस्त बनाने, पुणे के भीतर उतरने और बहुत कुछ जानने आया था। हो ही नहीं पाया। मेरी झोली ही फटी निकली। अगर बाद में मेल मुलाकात के न्यौते आये भी तो मेरा अहं आड़े आ गया और नुक्सान में मैं ही रहा। मेरी बहुत अच्छी दोस्त सुनीता इस बात को ले कर आज तक मुझसे नाराज़ है कि मैं खुद आगे बढ़ कर मौके के अनुरूप अपने आपको प्रस्तुत क्यों नहीं कर पाता। ये अलग बहस का मुद्दा है।
12. मेरी लेखन यात्रा
मुझे कहानियां और उपन्यास लिखते हुए लगभग तैंतीस-चौंतीस बरस हो गए हैं। इस बीच मैंने चार उपन्यास और पचास के करीब कहानियां और तीस के करीब लघुकथाएं लिखी हैं। सौ के करीब व्यंग्य लिखे होंगे और इतने ही लेख भी। अगर मोटे तौर पर गिना जाए तो इस अवधि में और इन रचनाओं के जरिये मैंने कम से कम 300 पात्रों की रचना तो की ही होगी। इनमें से कुछ पात्र मुझे बहुत प्रिय हैं और कुछ पात्र पाठकों के दिल में जगह बना कर बैठ गये हैं और कुछ ऐसे पात्र भी हैं जो मुझे और पाठकों, दोनों के लिए बहुत ही प्रिय बन पड़े हैं।
पाठक अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि हम लेखक लोग इतने सारे पात्र कहां से लाते हैं, उन्हें कैसे रचते हैं और उनमें प्राण कैसे फूंकते हैं कि वे न केवल हमारे लेखन में सजीव, विश्वसनीय और अपने से लगें बल्कि जिस समाज से हम उन पात्रों को उठाते हैं जिस समाज के लिए लिखते हैं वहां के पाठकों को भी वे अपने से लगें। तभी तो अक्सर ऐसा होता है कि पाठक हमें बताते हैं और उन्हें कई बार ऐसा लगता भी है कि कही गयी कहानी दरअसल उन्हीं की कहानी है या कहानी में दर्शायी गयी कुछ या अधिकांश घटनाएं उनके जीवन में हू ब हू घट चुकी हैं।
अपनी बात कहूं तो यह बात मैंने पहले भी कही है कि हम कहीं से पात्र तय करके नहीं लाते और ना ही किसी व्यक्ति को देख कर बता सकते हैं कि यह हमारी रचना का पात्र बनने वाला है। कई लोग हमसे अक्सर कहते भी रहते हैं कि हम पर कहानी लिखो या हमारा जीवन किसी उपन्यास से कम नहीं है, आप एक बार लिखना शुरू तो करो लेकिन हम पूरी संभावनाओं के बावजूद और चाह कर भी उस व्यक्ति पर कहानी किस्सा तो दूर एक लतीफा तक नहीं लिख पाते और ऐसा भी होता है कि कोई मामूली सा व्यक्ति या घटना हमें किसी बड़ी रचना के लिए प्रेरित करती है और इस तरह वे हमारी रचना के यादगार पात्र बनते चलते हैं। कितनी बार होता है कि हम एक व्यक्ति के जीवन की घटना उठा कर उस पर कहानी लिखते हैं लेकिन कहानी में चेहरा किसी और शख्स का होता है।
यह अपने आप होता चलता है कि परिचित या अपरिचित लोग हमारी रचनाओं के पात्र बनते चलते हैं और वक्त बीतने के साथ-साथ अमर भी हो जाते हैं। कई बार तो हम ऐसे पात्र भी रचते हैं जिनसे हम कभी मिले ही नहीं होते या वे जिस तरह का जीवन वे जी रहे होते हैं उससे बिल्कुल अलग और कई बार उसके विपरीत रूप में हमारी रचनाओं में आ विराजते हैं। मैंने यह भी कहा था कहीं कि हम लेखक समाज से सोना लेते हैं और समाज को अच्छे-अच्छे और खूबसूरत गहने बना कर लौटा देते हैं।
अपनी बात कहूं तो लेखन की पूरी अवधि के दौरान मैंने जितने भी पात्रों की रचना की है, लगभग तीन सौ के आसपास, सबके नाम, स्वभाव, किरदार, हैसियत और भूमिकाएं एक दूसरे से अलग हैं।
मैं लगभग इकतीस बरस तक बैंक में रहा और उससे पहले भी अलग-अलग नौकरियां दस बरस तक करता रहा। बेशक मेरा पहला उपन्यास हादसों के बीच बैंक की यूनियनबाजी की गतिविधियों के बारे में है और उसमें 25 के करीब किरदार हैं, मैंने अपनी कहानियों में से पांच सात कहानियां ही बैंक कर्मियों पर लिखी हैं। उससे पहले की नौकरियों में से भी कुछ ही पात्र मेरी कहानियों में आये हैं।
संयोग से मैंने अपनी रचनाओं में महिला पात्र ज्यादा रचे हैं। इनमें घरेलू, कामकाज करने वाली औरतें, नौकरानियां, अमीर औरतें, संघर्ष करती लड़कियां, भिखारिनें और वेश्याएं भी शामिल हैं। मेरी कहानियों में आये किसी नायक या नायिका किसी और कहानी में रिपीट नहीं हुए हैं। कुछ पात्र ऐसे हैं जो अपने जीवन में से जस के तस मेरी कहानियों में चले आये हैं और कुछ पात्र ऐसे हैं जिन्हें रचने के लिए मुझे कई-कई परिचितों के चेहरों, आदतों और स्वभाव आदि को शामिल करना पड़ा है और कई बार ऐसा भी हुआ है कि उन्हें रचने के लिए, रोचक और यादगार बनाने के लिए मुझे काफी हद तक कल्पना का सहारा लेना पड़ा है।
मेरे कुछ पात्रों ने मुझे बहुत रुलाया है और कागज पर उतरने से पहले मुझे बहुत तंग किया है और मेरी अच्छी खासी परीक्षा ली है। बहुत से ऐसे पात्र भी रहे जिन्हें रचते समय असीम सुख मिला। कुछ पात्र पूरी तरह से काल्पनिक हैं लेकिन बहुत अच्छे बन पड़े हैं और कुछ पात्र थोड़ा बहुत कल्पना का सहारा लेकर रचे गए हैं और शानदार बन गये हैं।
मेरी कई कहानियों में नायक या नायिका का नाम या तो सिर्फ एक ही बार आता है या नहीं आता। हमें आखिर तक पता नहीं चलता कि उस नायक या नायिका का नाम क्या है। मेरी लंबी कहानी देश, आज़ादी की पचासवीं वर्षगांठ और एक मामूली सी प्रेम कहानी, एक कमज़ोर लड़की कही कहानी, दो जीवन समांतर और दूसरी कई कहानियों में नायक का नाम एक बार भी नहीं आता। बस ऐसा होता चला गया। कई कहानियां सूत्रधार के माध्यम से कही गयी हैं और कुछ कहानियों में तो सूत्रधार पाठकों को संबोधित करता चलता है।
एक और बात, मेरी लगभग सभी रचनाओं में होती चली गयी है कि चाहे वह उपन्यास हो या कहानी, रचना के अंत में नायक और नायिका नहीं मिलते हैं। मेरी अधिकतर रचनाओं के पात्र ऐसे ही होते चले गए हैं कि वे नहीं मिलते तो नहीं ही मिलते। कोई न कोई ऐसा प्रसंग आ जाता है कि उनका मिलना नहीं हो पाता। मेरे पाठक हमेशा मुझसे इस बात के लिए नाराज़ होते रहे हैं कि मैं अपने पात्रों को क्यों नहीं मिलवाता। मैं इसका क्या जवाब दूं। हँस कर टाल देता हूं। मैं यह काम पाठक पर छोड़ देता हूं कि वह अपनी पसंद के नायक या नायिका से मिले। वही ज्यादा अच्छा होगा। बजाय इसके कि वह मेरी पसंद के नायक या नायिका से मिले और निराश हो। मेरी नायिका तो वक्त के साथ बूढ़ी हो जायेगी लेकिन पाठक की कल्पना की नायिका हमेशा युवा रहेगी।
यह बात भी है कि मैं अपनी रचनाओं में पाठकीय सहभागिता की गुंजाइश छोड़ता हूं। मैं कहानी को एक ऐसे बिंदु पर छोड़ देता हूं जहां से पाठक उसे आगे बढ़ा सके। ऐसा कितनी बार हुआ है कि पाठकों ने मुझे मेरी कहानी से आगे की कहानी लिख भेजी है। इसका अर्थ यही हुआ न कि कहानी खत्म होने के बाद भी पाठक के मन में चलती रहती है और वह उससे जुड़ा रहता है।
मेरी कई ऐसी कहानियां हैं जिनके पात्रों से मैं आज तक नहीं मिला और कहानी के सूत्र मुझे दूसरों से सुनकर या जानकर मिले हैं।
यह भी मेरे साथ ही हुआ है मेरी कहानी की नायिका की ज़िंदगी उस पर लिखी गई कहानी की वज़ह से ही बदल गयी। मेरी एक कहानी है एक कमज़ोर लड़की की कहानी। कहानी के अंत में यह दिखाया गया था कि नायिका को कैंसर है और नायक से उसका संपर्क खत्म हो जाता है। वह फोन, फेसबुक, व्हाट्सएप या संपर्क के किसी भी साधन से दूर हो चुकी है।
इस बीच कहानी की नायिका ठीक हो चुकी थी और फेसबुक के जरिए कहानी की खबर उस तक पहुंची थी। उसने कहानी पढ़ी। एक बार, दो बार और कई बार कहानी पढ़ने के बाद उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था और पति से कहा था कि घर चलाना उसका काम नहीं है। अब तक वह नौकरी करके घर चला रही थी और उसका पति बेबी सिटिंग करता रहा था। काम छोड़ देने के बाद उनके लिए संभव नहीं था कि वे दिल्ली जैसे शहर में रह पाएं। वे अपने शहर लौट गए थे। नायिका ने पहले एमए में किया फिर एमबीए किया और इस समय एक शानदार नौकरी कर रही है। अपने इस बदले हुए जीवन के लिए वह इस कहानी को टर्निंग प्वाइंट मानती है बेशक वह किसी को बता नहीं सकती कि यह कहानी उसके जीवन पर लिखी गयी है।
दो बार ऐसा हुआ कि मुझे अपनी ही कहानियों के सीक्वल यानी आगे के भाग लिखने पड़े। 1992 में लिखी गई कहानी फैसले मेरे बॉस के जीवन पर लिखी गई थी जो मुंबई में अकेले रहकर संघर्ष कर रहे थे और उनके परिवार ने उनके साथ आकर रहने से मना कर दिया था। वक्त ने करवट ली और वे पूरी ज़िंदगी लगभग 36 बरस तक परिवार से अलग मुंबई में अकेले रहते रहे। जब वे रिटायर हुए तो कई रोग पाल चुके थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे रिटायरमेंट के बाद कहां जायें। गांव गए लेकिन वहां पर रह नहीं पाए। मजबूरन पत्नी के शहर पत्नी और बच्चों के पास गए लेकिन वहां पर भी एडजस्ट नहीं कर पाए। पहले ब्रेन हेमरेज, फिर पैरालिसिस और उसके बाद कोमा में चले गए। 2010 में जब मैं उनसे मिला था तो पिछले चार साल से कोमा में पड़े हुए थे। उनकी यह हालत देखकर मैंने 7 बरस के राइटर्स ब्लॉक के बाद डरा हुआ आदमी कहानी लिखी थी। पिछले वर्ष ही तेरह बरस तक अपने घर में कौमा में रहने के बाद उनकी मृत्यु हो गई है।
मेरी एक और कहानी है छोटे नवाब बड़े नवाब जो 1991 में लिखी गई थी। यह दो भाइयों की कहानी है जो प्रॉपर्टी के बंटवारे के साथ-साथ अपने मां-बाप का भी बंटवारा कर देते हैं। कैंसर से पीड़ित मां छोटे भाई के हिस्से में आती है। मां के मरने पर वह आधी रात को फोन करके बड़े भाई से सौदेबाजी करता है कि अगर मां के अंतिम दर्शन करने हैं तो मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी की पेपर्स लेकर आए। यह घटना मेरे पिताजी ने सुनाई थी। वे उन दिनों उन्हीं भाइयों के साथ प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहे थे। छोटे नवाब बड़े नवाब कहानी दूरदर्शन पर दिखायी गयी थी। तब कहानी में उनके पिता की बात कहनी रह गयी थी जो अपनी पत्नी की लाश पर बेटों को सौदेबाजी करते हुए देख रहा था और जो अंतिम संस्कार 11:00 बजे होना था वह शाम के 4:00 बजे हो पाया था।
इस कहानी के लगभग 12 बरस बाद मैंने पिता को लेकर आगे की कहानी लिखी थी – मर्द नहीं रोते। तभी मुझे लगा था कि मैं कम से कम अपने पात्रों के साथ न्याय कर पाया हूं। दोनों कहानियां बहुत पसंद की जाती हैं।
पिछले बरसों की लगभग सभी कहानियों में और दोनों उपन्यासों में भी महिला पात्र अधिक हैं और वे फेसबुक से आए हैं। मैं मानता हूं कि फेसबुक बेशक आभासी है लेकिन उसके पीछे के चेहरे असली हैं और इसी जगत से आते हैं। एक बात और भी है कि फेसबुक पर अधिकतर महिला मित्र ऐसी मिली हैं जिन्हें कुछ ना कुछ शेयर करना था और उन्हें मुझ पर विश्वास करके अपनी तकलीफें, अपनी महत्वाकांक्षाएं और अपनी हसरतें शेयर की हैं और उनमें मुझे कहानी के लायक सामग्री मिली है। मैंने उनकी पूरी निजता का सम्मान करते हुए उन पर कहानियां लिखी हैं। कुछ कहानियां तो मैंने अपने पात्रों के साथ शेयर भी की है और कुछ कहानियां ऐसी भी है कि उन तक नहीं पहुंची है या मैंने इसकी ज़रूरत नहीं समझी है।
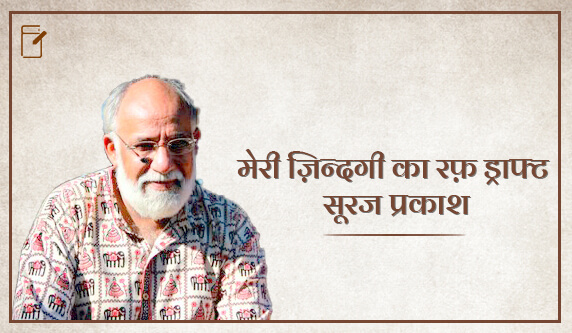
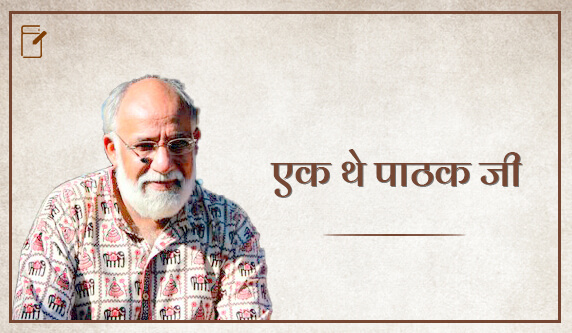

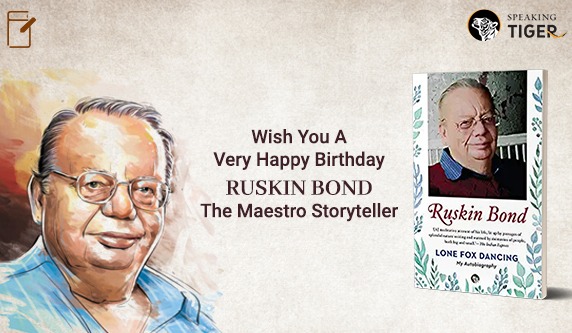

No Comments